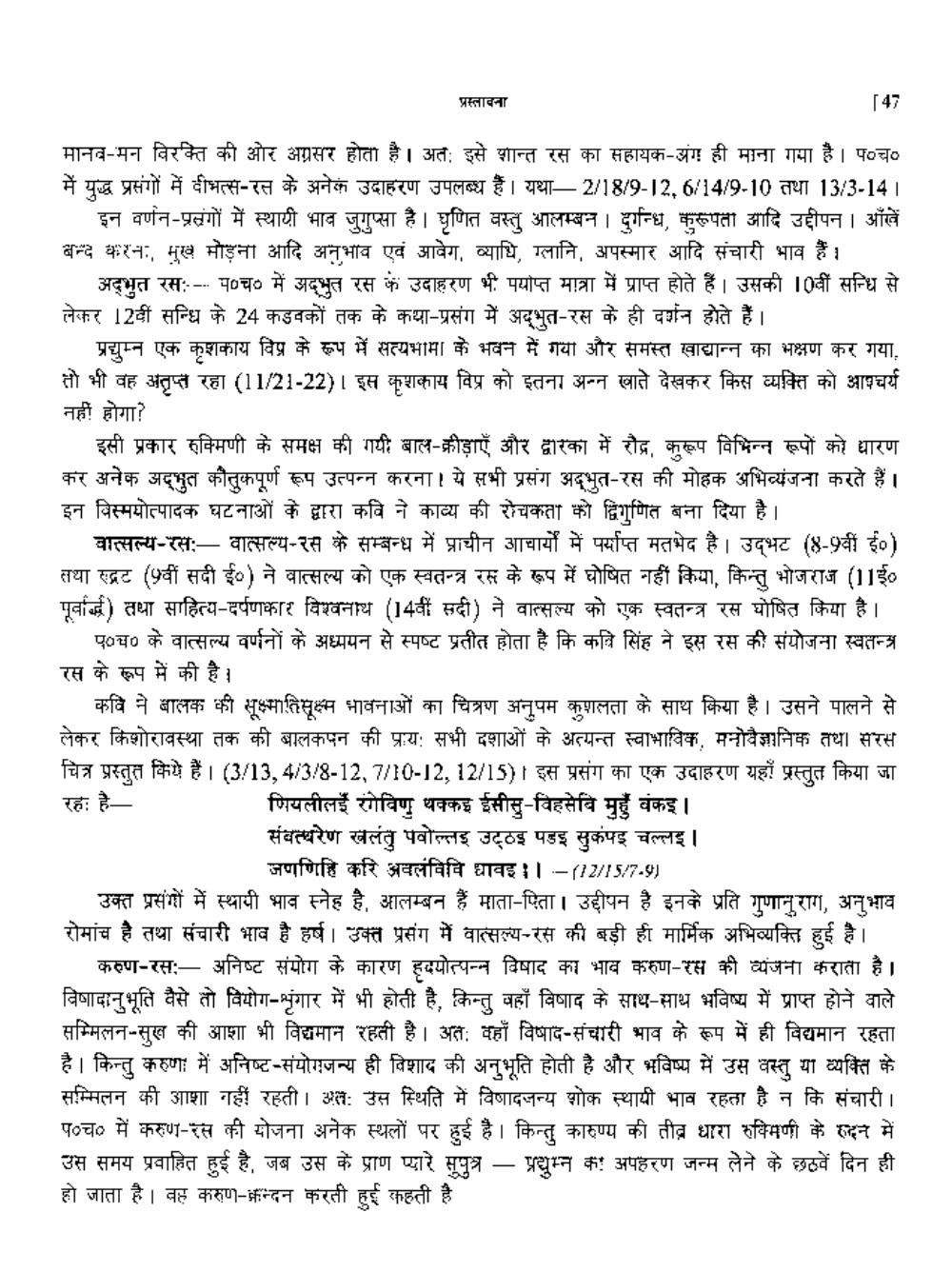________________
प्रस्तावना
147
मानव-मन विरक्ति की ओर अग्रसर होता है। अत: इसे शान्त रस का सहायक-अंग ही माना गया है। प०च० में युद्ध प्रसंगों में वीभत्स-रस के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। यथा- 2/18/9-12, 6/14/9-10 तथा 13/3-14 ।
इन वर्णन-प्रसंगों में स्थायी भाव जुगुप्सा है। घृणित वस्तु आलम्बन । दुर्गन्ध, कुरूपता आदि उद्दीपन । आँखें बन्द करनः, मुख मोड़ना आदि अनुभाव एवं आवेग, व्याधि, ग्लानि, अपस्मार आदि संचारी भाव हैं। ___अद्भुत रस:--- म०च० में अद्भुत रस के उदाहरण भ. पयोप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। उसकी 10वीं सन्धि से लेकर 12वीं सन्धि के 24 कड़वकों तक के कथा-प्रसंग में अद्भुत-रस के ही दर्शन होते हैं।
प्रद्युम्न एक कृशकाय विप्र के रूप में सत्यभामा के भवन में गया और समस्त खाद्यान्न का भक्षण कर गया, तो भी वह अतृप्त रहा (11/21-22)। इस कृशकाय विप्र को इतना अन्न खाते देखकर किस व्यक्ति को आश्चर्य नहीं होगा?
इसी प्रकार रुक्मिणी के समक्ष की गयी बाल-क्रीड़ाएँ और द्वारका में रौद्र, कुरूप विभिन्न रूपों को धारण कर अनेक अद्भुत कौतुकपूर्ण रूप उत्पन्न करना। ये सभी प्रसंग अद्भुत-रस की मोहक अभिव्यंजना करते हैं। इन विस्मयोत्पादक घटनाओं के द्वारा कवि ने काव्य की रोचकता को विगणित बना दिया
वात्सल्य-रस:- वात्सल्य-रस के सम्बन्ध में प्राचीन आचार्यों में पर्याप्त मतभेद है। उद्भट (8-9वीं ई०) तथा रुद्रट (५वीं सदी ई.) ने वात्सल्य को एक स्वतन्त्र रस के रूप में घोषित नहीं किया, किन्तु भोजराज (11ई० पूर्वार्द्ध) तथा साहित्य-दर्पणकार विश्वनाथ (14वीं सदी) ने वात्सल्य को एक स्वतन्त्र रस घोषित किया है।
प०च० के वात्सल्य वर्णनों के अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि कवि सिंह ने इस रस की संयोजना स्वतन्त्र रस के रूप में की है।
कवि ने बालक की सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावनाओं का चित्रण अनुपम कुशलता के साथ किया है। उसने पालने से लेकर किशोरावस्था तक की बालकपन की प्राय: सभी दशाओं के अत्यन्त स्वाभाविक, मनोवैज्ञानिक तथा सरस चित्र प्रस्तुत किये हैं। (3/13,473/8-12, 7/10-12, 12/15)। इस प्रसंग का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जा
णियलीलइँ रंगेविण थक्कइ ईसीसु-विहसेबि मुहुँ वंकइ । संवत्थरेण खलंतु पवोल्लइ उट्ठइ पडइ सुकंपइ चल्लइ ।
जणणिहि करि अवलंविवि धावइ ।। -(12/15/7-9) उक्त प्रसंगों में स्थायी भाव स्नेह है, आलम्बन हैं माता-पिता। उद्दीपन है इनके प्रति गुणानुराग, अनुभाव रोमांच है तथा संचारी भाव है हर्ष। उक्त प्रसंग में वात्सल्य रस की बड़ी ही मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है।
करुण-रस:- अनिष्ट संयोग के कारण हृदयोत्पन्न विषाद का भाव करुण-रस की व्यंजना कराता है। विषादानुभूति वैसे तो वियोग-शृंगार में भी होती है, किन्तु वहाँ विषाद के साथ-साथ भविष्य में प्राप्त होने वाले सम्मिलन-सुख की आशा भी विद्यमान रहती है। अत: वहाँ विषाद-संचारी भाव के रूप में ही विद्यमान रहता है। किन्तु करुणा में अनिष्ट-संयोग्गजन्य ही विशाद की अनुभूति होती है और भविष्य में उस वस्तु या व्यक्ति के सम्मिलन की आशा नहीं रहती। अत: उस स्थिति में विषादजन्य शोक स्थायी भाव रहता है न कि संचारी। प०च० में करुण-रस की योजना अनेक स्थलों पर हुई है। किन्तु कारुण्य की तीव्र धारा रुक्मिणी के रुदन में उस समय प्रवाहित हुई है, जब उस के प्राण प्यारे सुपुत्र – प्रद्युम्न का अपहरण जन्म लेने के छठवें दिन ही हो जाता है। वह करुण-अन्दन करती हुई कहती है