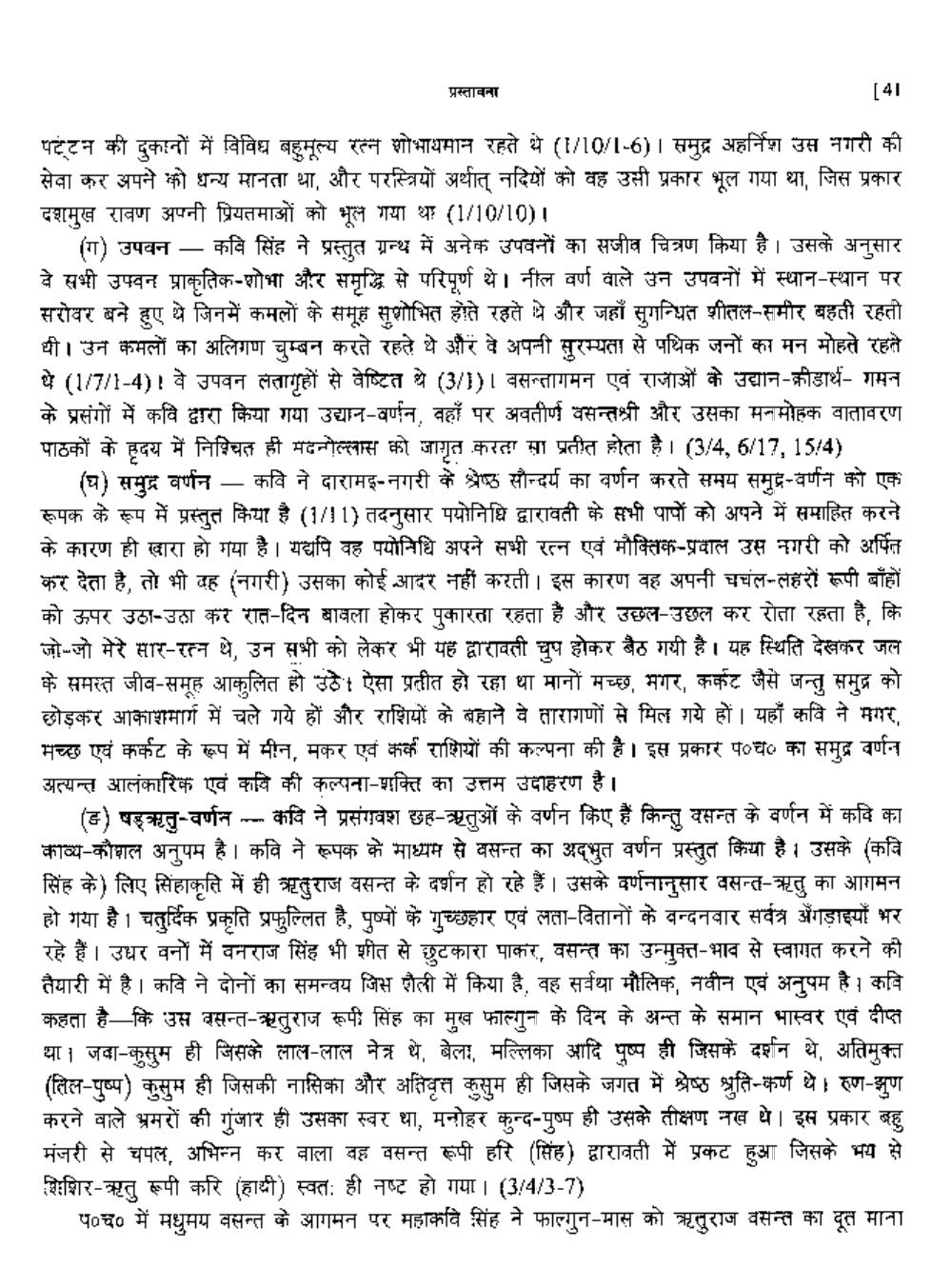________________
प्रस्तावना
[41
पट्टन की दुकानों में विविध बहुमूल्य रत्न शोभाधमान रहते थे (1/10/1-6)। समुद्र अहर्निश उस नगरी की सेवा कर अपने को धन्य मानता था, और परस्त्रियों अर्थात् नदियों को वह उसी प्रकार भूल गया था, जिस प्रकार दशमुख रावण अपनी प्रियतमाओं को भूल गया था (1/10/10)।
(ग) उपवन - कवि सिंह ने प्रस्तुत ग्रन्थ में अनेक उपवनों का सजीव चित्रण किया है। उसके अनुसार वे सभी उपवन प्राकृतिक-शोभा और समृद्धि से परिपूर्ण थे। नील वर्ण वाले उन उपवनों में स्थान-स्थान पर सरोवर बने हुए थे जिनमें कमलों के समूह सुशोभित होते रहते थे और जहाँ सुगन्धित शीतल-समीर बहती रहती थी। उन कमलों का अलिगण चुम्बन करते रहते थे और वे अपनी सुरम्यता से पथिक जनों का मन मोहते रहते थे (1/7/1-4)! वे उपवन लतागृहों से वेष्टित थे (373)। वसन्तागमन एवं राजाओं के उद्यान-क्रीडार्थ- गमन के प्रसंगों में कवि द्वारा किया गया उद्यान-वर्णन, वहाँ पर अवतीर्ण वसन्तश्री और उसका मनमोहक वातावरण पाठकों के हृदय में निश्चित ही मदनोल्लास को जागृत करता सा प्रतीत होता है। (3/4,6/17, 15/4)
(घ) समुद्र वर्णन – कवि ने दारामइ-नगरी के श्रेष्ठ सौन्दर्य का वर्णन करते समय समुद्र-वर्णन को एक रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है (1/11) तदनुसार पयोनिधि द्वारावती के सभी पापों को अपने में समाहित करने के कारण ही खारा हो गया है। यद्यपि वह पयोनिधि अपने सभी रत्न एवं मौक्तिक-प्रवाल उस नगरी को अर्पित कर देता है, तो भी वह (नगरी) उसका कोई आदर नहीं करती। इस कारण वह अपनी चचल-लहरों रूपी बाँहों को ऊपर उठा-उठा कर रात-दिन बावला होकर पुकारता रहता है और उछल-उछल कर रोता रहता है, कि जो-जो मेरे सार-रत्न थे, उन सभी को लेकर भी यह द्वारावती चुप होकर बैठ गयी है। यह स्थिति देखकर जल के समस्त जीव-समूह आकुलित हो उठे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानों मच्छ, मगर, कर्कट जैसे जन्तु समुद्र को छोड़कर आकाशमार्ग में चले गये हों और राशियों के बहाने वे तारागणों से मिल गये हों। यहाँ कवि ने मगर, मच्छ एवं कर्कट के रूप में मीन, मकर एवं कर्क राशियों की कल्पना की है। इस प्रकार प०च० का समुद्र वर्णन अत्यन्त आलंकारिक एवं कवि की कल्पना-शक्ति का उत्तम उदाहरण है।
(ड) षड्ऋतु-वर्णन --- कवि ने प्रसंगवश छह-ऋतुओं के वर्णन किए हैं किन्तु वसन्त के वर्णन में कवि का काव्य-कौशाल अनुपम है। कवि ने रूपक के माध्यम से वसन्त का अद्भुत वर्णन प्रस्तुत किया है। उसके (कवि सिंह के लिए सिंहाकृति में ही ऋतुराज वसन्त के दर्शन हो रहे हैं। उसके वर्णनानुसार वसन्त-ऋतु का आगमन हो गया है। चतुर्दिक प्रकृति प्रफुल्लित है, पुष्पों के गुच्छहार एवं लता-वितानों के वन्दनवार सर्वत्र अँगड़ाइयाँ भर रहे हैं। उधर वनों में वनराज सिंह भी शीत से छुटकारा पाकर, वसन्त का उन्मुक्त-भाव से स्वागत करने की तैयारी में है। कवि ने दोनों का समन्वय जिस शैली में किया है. वह सर्वथा मौलिक, नवीन एवं अनुपम है। कवि कहता है कि उस वसन्त-ऋतुराज रूपी सिंह का मुख फाल्गुन के दिन के अन्त के समान भास्वर एवं दीप्त था। जदा-कुसुम ही जिसके लाल-लाल नेत्र थे, बेला, मल्लिका आदि पुष्प ही जिसके दर्शन थे, अतिमुक्त (तिल-पुष्प) कुसुम ही जिसकी नासिका और अतिवृत्त कुसुम ही जिसके जगत में श्रेष्ठ श्रुति-कर्ण थे। रुण-झुण करने वाले भ्रमरों की गुंजार ही उसका स्वर था, मनोहर कुन्द-पुष्प ही उसके तीक्षण नख थे। इस प्रकार बहु मंजरी से चपल, अभिन्न कर वाला वह वसन्त रूपी हरि (सिंह) द्वारावती में प्रकट हुआ जिसके भय से शिशिर-ऋतु रूपी करि (हादी) स्वत: ही नष्ट हो गया। (314/3-7)
प०५० में मधुमय वसन्त के आगमन पर महाकवि सिंह ने फाल्गुन-मास को ऋतुराज वसन्त का दूत माना