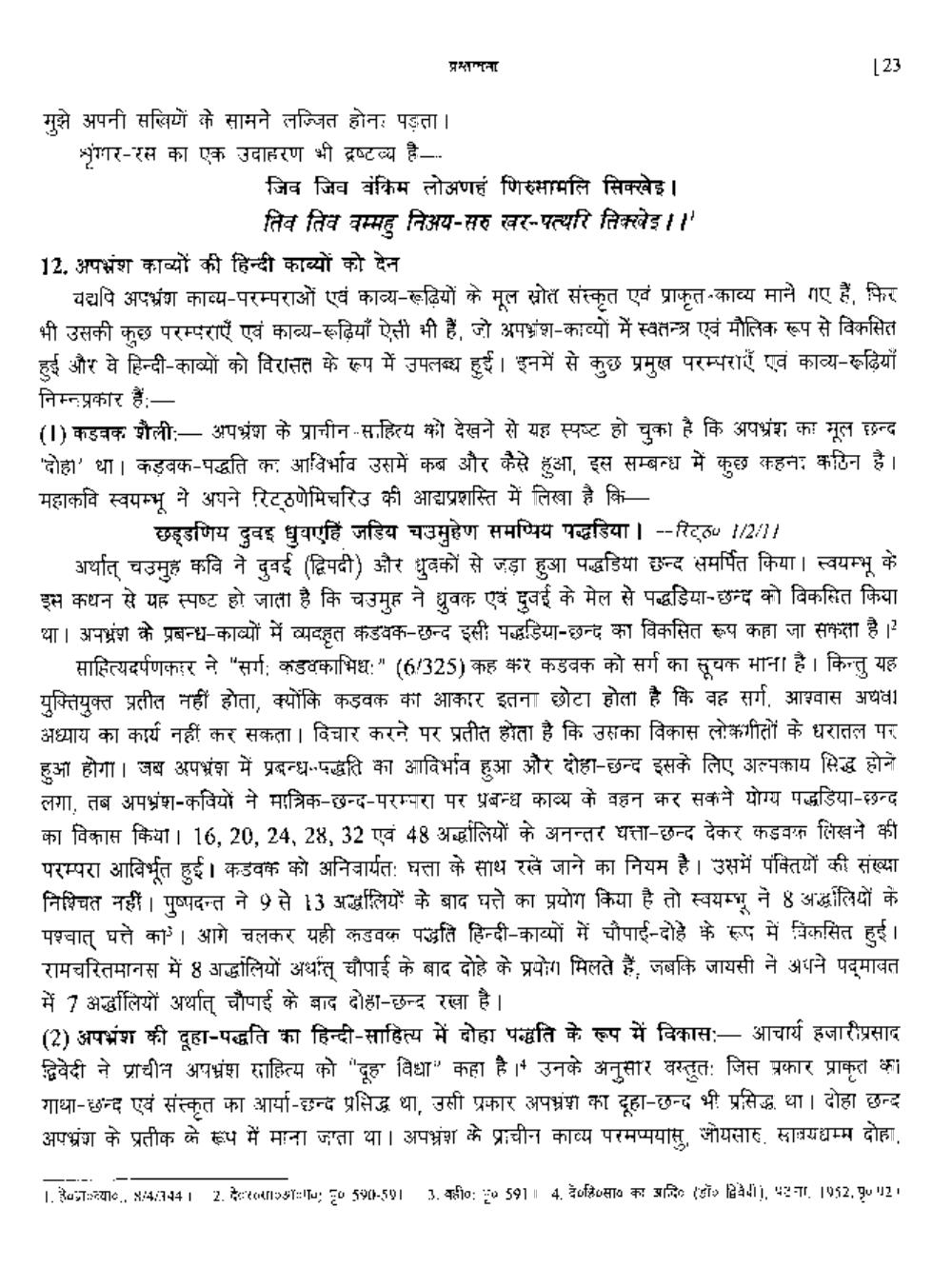________________
प्रशमना
मुझे अपनी सखिों के सामने लज्जित होना पड़ता। श्रृंगार-रस का एक उदाहरण भी द्रष्टव्य है...
जिव जिव बंकिम लोअणहं णिरुसामलि सिक्खेइ।
तिव तिव वम्महु निअय-सरु खर-पत्थरि तिक्खेइ।। 12. अपभंश काव्यों की हिन्दी काव्यों को देन __वद्यपि अपभ्रंश काव्य-परम्पराओं एवं काव्य-रूढ़ियों के मूल स्रोत संस्कृत एवं प्राकृत काव्य माने गए हैं, फिर भी उसकी कुछ परम्पराएँ एवं काव्य-रूढ़ियाँ ऐसी भी हैं, जो अपभ्रंश-काव्यों में स्वतन्त्र एवं मौलिक रूप से विकसित हुई और वे हिन्दी-काव्यों को विरासत के रूप में उपलब्ध हुई। इनमें से कुछ प्रमुख परम्पराएँ एवं काव्य-रूढ़ियों निम्न प्रकार हैं:(I) कडवक शैली:- अपभ्रंश के प्राचीन साहित्य को देखने से यह स्पष्ट हो चुका है कि अपभ्रंश का मूल छन्द "दोहा' था। कड़वक-पद्धति कः आविर्भाव उसमें कब और कैसे हुआ, इस सम्बन्ध में कुछ कहना कठिन है। महाकवि स्वयम्भू ने अपने रिट्ठणेमिचरिउ की आद्यप्रशस्ति में लिखा है कि
छड्डणिय दुवइ धुवाएहिं जडिय चउमुहेण समप्पिय पद्धडिया। --रिट्ठः ।।27। अर्थात् चउमुह कवि ने दुबई (द्विपदी) और धुवकों से जुड़ा हुआ पद्धडिया छन्द समर्पित किया। स्वयम्भू के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि चउमुह ने धुवक एवं दुबई के मेल से पद्धड़िया-छन्द को विकसित किया था। अपभ्रंश के प्रबन्ध-काव्यों में व्यवहृत कडवक-छन्द इसी पद्धडिया-छन्द का विकसित रूप कहा जा सकता है।
साहित्यदर्पणकार ने "सर्ग: कडवकाभिध:" (6/325) कह कर कडवक को सर्ग का सूचक माना है। किन्तु यह युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कड़वक का आकार इतना छोटा होता है कि वह सर्ग. आश्वास अथवा अध्याय का कार्य नहीं कर सकता। विचार करने पर प्रतीत होता है कि उसका विकास लोकगीतों के धरातल पर हुआ होगा। जब अपभ्रंश में प्रबन्ध-पद्धति का आविर्भाव हुआ और दोहा-छन्द इसके लिए अल्पकाय सिद्ध होने लगा, तब अपभ्रंश-कवियों ने मात्रिक-छन्द-परम्परा पर प्रबन्ध काव्य के वहन कर सकने योग्य पद्धडिया-छन्द का विकास किया। 16, 20, 24, 28, 32 एवं 48 अद्धालियों के अनन्तर धत्ता-छन्द देकर कड़वास लिखने की परम्परा आविर्भूत हुई। कडवक को अनिवार्यत: घत्ता के साथ रखे जाने का नियम है। उसमें पंक्तियों की संख्या निश्चित नहीं। पुष्पदन्त ने 9 से 13 अलियों के बाद घत्ते का प्रयोग किया है तो स्वयम्भू ने 8 अर्ड्सलियों के पश्चात् घत्ते का। आगे चलकर यही लडवक पद्धति हिन्दी-काव्यों में चौपाई-दोहे के रूप में विकसित हुई। रामचरितमानस में 8 गोलियों अर्थात् चौपाई के बाद दोहे के प्रयोग मिलते हैं, जबकि जायसी ने अपने पद्मावत में 7 अर्धालियों अर्थात् चौपाई के बाद दोहा-छन्द रखा है। (2) अपभ्रंश की दूहा-पद्धति का हिन्दी-साहित्य में दोहा पद्धति के रूप में विकास:- आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन अपभ्रंश साहित्य को "दूह' विधा" कहा है। उनके अनुसार वस्तुतः जिस प्रकार प्राकृत का गाथा-छन्द एवं संस्कृत का आर्या-छन्द प्रसिद्ध था, उसी प्रकार अपभ्रंश का दूहा-छन्द भी प्रसिद्ध था। दोहा छन्द अपभ्रंश के प्रतीक के रूप में माना जाता था। अपभ्रंश के प्राचीन काव्य परमप्पयासु, जोयसारू. सायधम्म दोहा.
I. ३ःच्या..843441 2.दे:१०NISTITUT0500-50
3. वहीं:0591॥ 4. दैहिसा० का अन्दिक डॉ
बी, पटना. 1952.
21