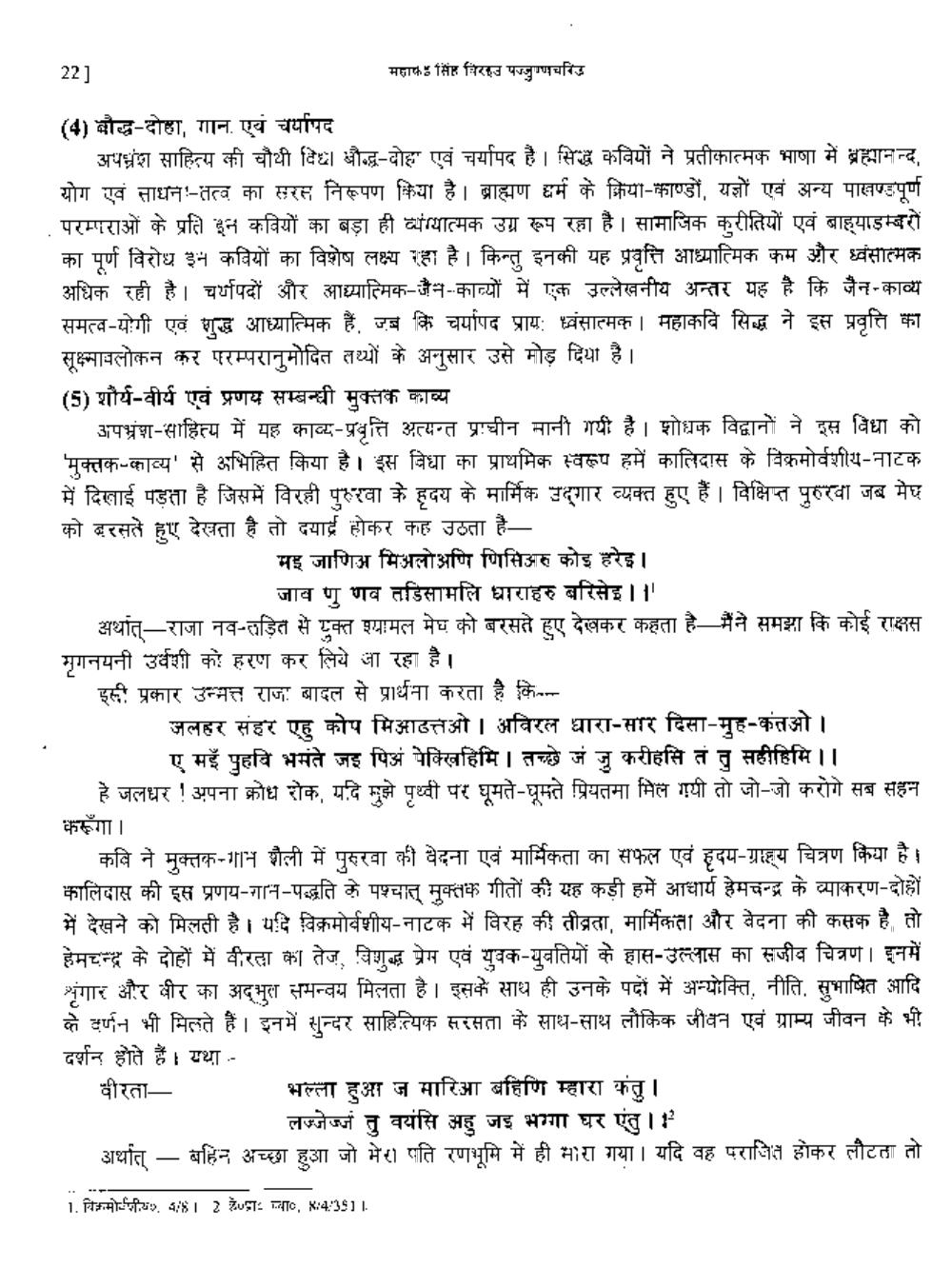________________
22]
महाफ ४ सिंह विरउ पज्जुग्णचरित
(4) बौद्ध-दोहा, गान. एवं चर्यापद ___ अपभ्रंश साहित्य की चौथी विधा बौद्ध-वोह एवं चर्यापद है। सिद्ध कवियों ने प्रतीकात्मक भाषा में ब्रह्मानन्द, योग एवं साधन-तत्व का सरस निरूपण किया है। ब्राह्मण धर्म के क्रिया-काण्डों, यज्ञों एवं अन्य पाखण्डपूर्ण परम्पराओं के प्रति इन कवियों का बड़ा ही व्यंग्यात्मक उग्र रूप रहा है। सामाजिक कुरीतियों एवं बाह्याइम्बरों का पूर्ण विरोध इन कवियों का विशेष लक्ष्य रहा है। किन्तु इनकी यह प्रवृत्ति आध्यात्मिक कम और ध्वंसात्मक अधिक रही है। चपदों और आध्यात्मिक-जैन-काच्यों में एक उल्लेखनीय अन्तर यह है कि जैन-काव्य समत्व-योगी एवं शुद्ध आध्यात्मिक हैं. उब कि चर्यापद प्राय: ध्वंसात्मक । महाकवि सिद्ध ने इस प्रवृत्ति का सूक्ष्मावलोकन कर परम्परानुमोदित तथ्यों के अनुसार उसे मोड़ दिया है। (5) शौर्य-वीर्य एवं प्रणय सम्बन्धी मुक्तक काव्य
अपभ्रंश-साहित्य में यह काव्य-प्रवृत्ति अत्यन्त प्राचीन नानी गयी है। शोधक विद्वानों ने इस विधा को 'मुक्तक-काव्य' से अभिहित किया है। इस विधा का प्राथमिक स्वरूप हमें कालिदास के विक्रमोर्वशीय-नाटक में दिखाई पड़ता है जिसमें विरही पुरुरवा के हृदय के मार्मिक उद्गार व्यक्त हुए हैं। विक्षिप्त पुरुरवा जब मेछ को बरसते हुए देखता है तो दयार्द्र होकर कह उठता है
मइ जाणिअ मिअलोअणि णिसिअरु कोइ हरेइ ।
जाव णु णव तडिसामलि धाराहरु बरिसेइ।।। अर्थात् राजा नव-तड़ित से युक्त श्यामल मेघ को बरसते हुए देखकर कहता है—मैंने समझा कि कोई राक्षस मृगनयनी उर्वशी को हरण कर लिये जा रहा है। इसी प्रकार उन्मत्त राजा बादल से प्रार्थना करता है कि...
जलहर संहर एहु कोप मिआढत्तओ । अविरल धारा-सार दिसा-मुह-कत्तओ।
ए मइँ पुहवि भमंते जइ पिझं पेक्खिहिमि । तच्छे जं जु करीहसि तं तु सहीहिमि ।। है जलधर ! अपना क्रोध रोक, यदि मुझे पृथ्वी पर घूमते-घूमते प्रियतमा मिल गयी तो जो-जो करोगे सब सहन करूँगा।
कवि ने मुक्तक-गान शैली में पुरुरवा की वेदना एवं मार्मिकता का सफल एवं हृदय-ग्राह्य चित्रण किया है। कालिदास की इस प्रणय-गान-पद्धति के पश्चात् मुक्तक गीतों की यह कड़ी हमें आधार्य हेमचन्द्र के व्याकरण-दोहों में देखने को मिलती है। यदि विक्रमोर्वशीय-नाटक में विरह की तीव्रता, मार्मिकता और वेदना की कसक है, तो हेमचन्द्र के दोहों में वीरता का तेज, विशुद्ध प्रेम एवं युवक-युवतियों के हास-उल्लास का सजीव चित्रण। इनमें शृंगार और वीर का अद्भुत समन्वय मिलता है। इसके साथ ही उनके पदों में अन्योक्ति, नीति. सुभाषित आदि के वर्णन भी मिलते हैं। इनमें सुन्दर साहित्यिक सरसता के साथ-साथ लौकिक जीवन एवं ग्राम्य जीवन के भी दर्शन होते हैं। यथा - वीरता
भल्ला हुआ ज मारिआ बहिणि म्हारा कंत् ।
लज्जेज तु वयंसि अहु जइ भग्गा घर एंतु ।' अर्थात् – बहिन अच्छा हुआ जो मेरा पति रणभूमि में ही मारा गया। यदि वह पराजित होकर लौटता तो
1. विक्रमोशीय 48। 2 प्राः ज्या०. :43911