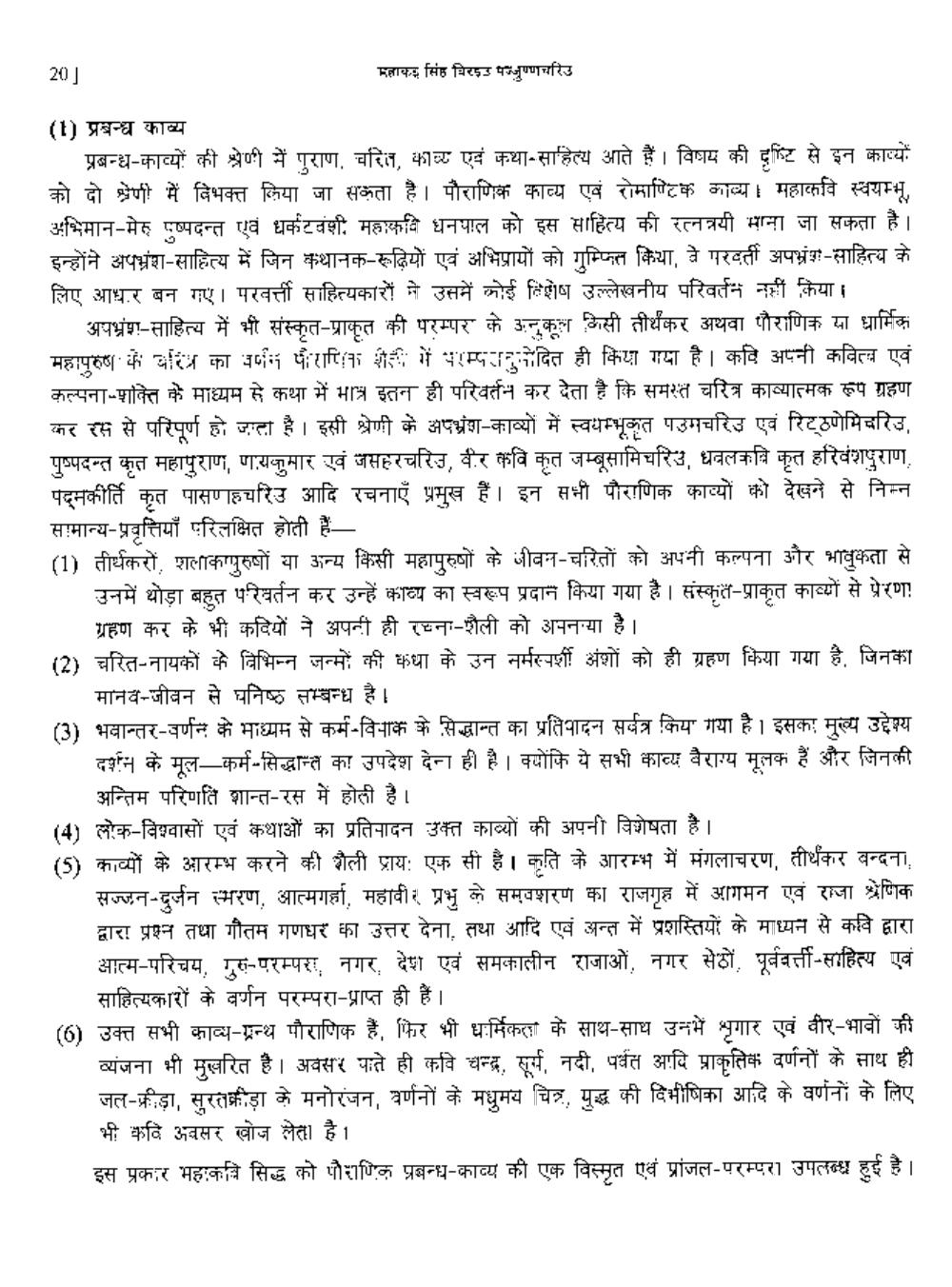________________
20]
महाकर सिंह चिरकर पन्जुण्णचरिउ
(1) प्रबन्ध काव्य
प्रबन्ध-काव्यों की श्रेणी में पुराण. चरित, काय एवं कथा-साहित्य आते हैं। विषय की दृष्टि से इन काव्ये को दो श्रेणी में विभक्त किया जा सकता है। पौराणिक काच्य एवं रोमाण्टिक काव्य। महाकवि स्वयम्भू, अभिमान-मेरु पुष्पदन्त एवं धर्कटवंश. महाकवि धनपाल को इस साहित्य की रत्नत्रयी माना जा सकता है। इन्होंने अपभ्रंश-साहित्य में जिन कथानक-रूढ़ियों एवं अभिप्रायों को गुम्प्ति किया, वे परवर्ती अपभ्रंशा-साहित्य के लिए आधार बन गए। परवर्ती साहित्यकारों से उसमें कोई विशेष उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं किया। ___ अपभ्रंशा-साहित्य में भी संस्कृत-प्राकृत की परम्पर के अनुकूल किसी तीर्थंकर अथवा पौराणिक या धार्मिक महापुरुष के यरित्र का वर्णन पौरारित शैली में पाम्पसनुमोदित ही किया गया है। कवि अपनी कवित्व एवं कल्पना-शक्ति के माध्यम से कथा में मात्र इतन ही परिवर्तन कर देता है कि समस्त चरित्र काव्यात्मक रूप ग्रहण कर रस से परिपूर्ण हो जाता है। इसी श्रेणी के अपभ्रंश-काव्यों में स्वयम्भूकत पउमरिउ एवं रिठणेमिचरिउ, पुष्पदन्त कृत महापुराण, णायकुमार एवं जसहरचरिज, वर कवि कृत जम्बूसामिचरिउ, धवलकवि कृत हरिवंशपुराण पद्मकीर्ति कृत पासणहचरिउ आदि रचनाएँ प्रमुख हैं। इन सभी पौराणिक काव्यों को देखने से निन्न सामान्य-प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं(1) तीर्थकरों, शलाकापुरुषों या अन्य किसी महापुरुषों के जीवन-चरितों को अपनी कल्पना और भावुकता से
उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर उन्हें काव्य का स्वरूप प्रदान किया गया है। संस्कृत-प्राकृत काव्यों से प्रेरणा
ग्रहण कर के भी कदियों ने अपनी ही रचना-शैली को अपनाया है। (2) चरित-नायकों के विभिन्न जन्मों की कंधा के उन नर्मस्पर्शी अंशों को ही ग्रहण किया गया है. जिनका
मानव-जीवन ले घनिष्ठ सम्बन्ध है। (3) भवान्तर-वर्णन के माध्यम से कर्म-विनाक के सिद्धान्त का प्रतिपादन सर्वत्र किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य
दर्शन के मूल-कर्म-सिद्धान्त का उपदेश देना ही है। क्योंकि ये सभी काय वैराग्य मूलक हैं और जिनकी
अन्तिम परिणति शान्त-रस में होती है। (4) लोक-विश्वासों एवं कथाओं का प्रतिपादन उक्त काव्यों की अपनी विशेषता है। (5) काव्यों के आरम्भ करने की शैली प्राय: एक सी है। कृति के आरम्भ में मंगलाचरण, तीर्थंकर बन्दना,
सज्जन-दुर्जन स्मरण, आत्मगर्हा, महावीर प्रभु के समवशरण का राजगृह में आगमन एवं राजा श्रेणिक द्वारा प्रश्न तथा गौतम गणधर का उत्तर देना, तथा आदि एवं अन्त में प्रशस्तियों के माध्यन से कवि द्वारा आत्म-परिचय, गुरु-परम्परा, नगर, देश एवं समकालीन राजाओं, नगर सेठों, पूर्ववर्ती-साहित्य एवं
साहित्यकारों के वर्णन परम्परा-प्राप्त ही हैं। (6) उक्त सभी काव्य-ग्रन्थ पौराणिक हैं, फिर भी धार्मिकता के साथ-साथ उनमें शृगार एवं वीर-भावों की
व्यंजना भी मुखरित है। अवसर पाते ही कवि चन्द्र, सूर्य, नदी, पर्वत आदि प्राकृतिक वर्णनों के साथ ही जल-फ्रीड़ा, सुरतक्रीड़ा के मनोरंजन, वर्णनों के मधुमय चित्र. युद्ध की विभीषिका आदि के वर्णनों के लिए भी कवि अवसर खोज लेता है। इस प्रकार महाकवि सिद्ध को पौराणिक प्रबन्ध-काव्य की एक विस्मृत एवं प्रांजल-परम्परा उपलब्ध हुई है।