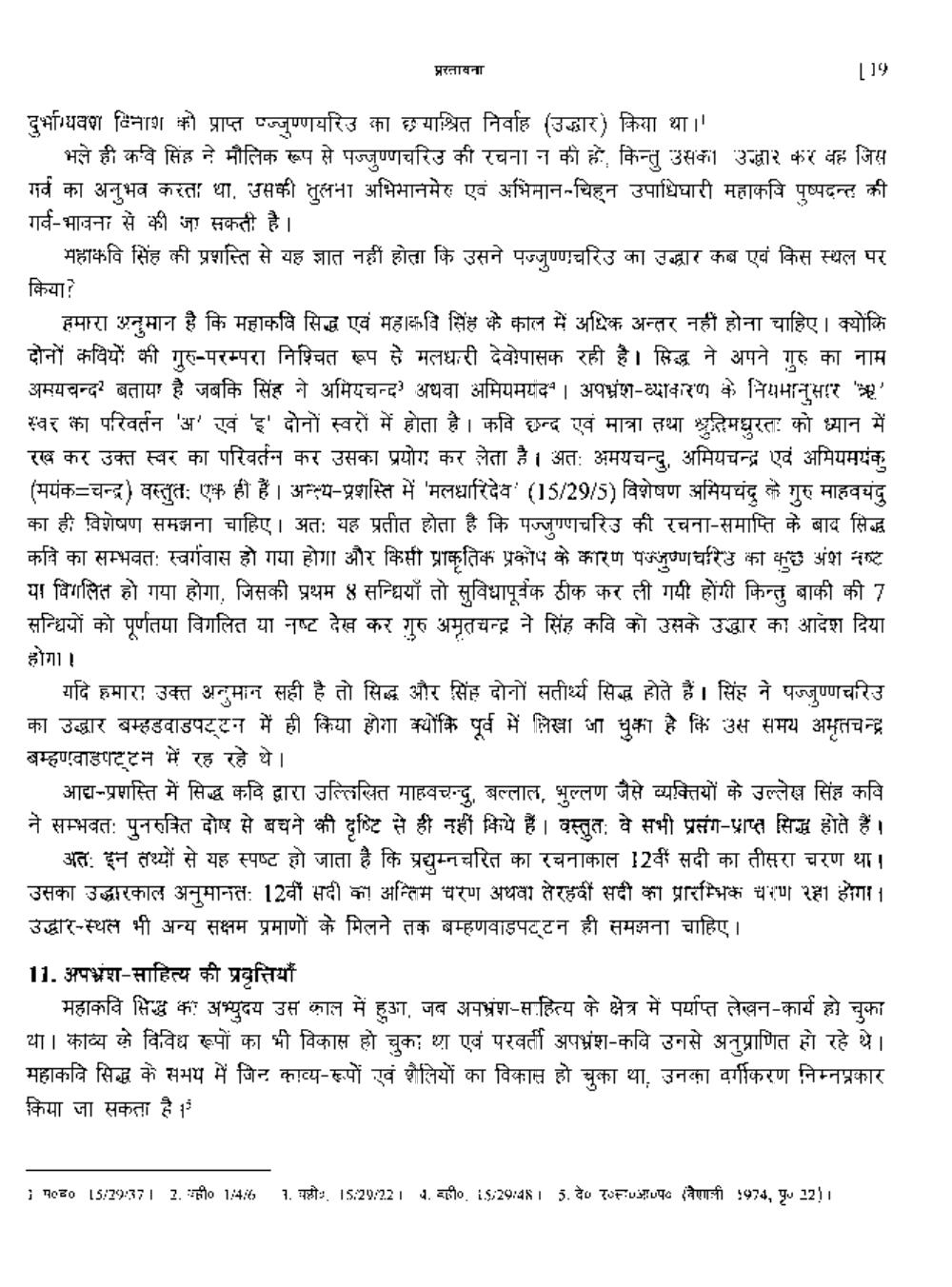________________
प्रस्तावना
[19
दुर्भाग्यवश विनाश को प्राप्त प्रज्जुण्णयरिउ का छयाश्रित निर्वाह (उद्धार) किया था।।
भले ही कवि सिंह ने मौलिक रूप से पज्जुण्णचरिउ की रचना न की है, किन्तु उसका उद्धार कर वह जिस गर्व का अनुभव करता था. उसकी तुलना अभिमानमेरु एवं अभिमान-चिह्न उपाधिघारी महाकवि पुष्पदन्त की गर्व-भावना से की जा सकती है।
महाकवि सिंह की प्रशस्ति से यह ज्ञात नहीं होता कि उसने पज्जुण्णचरिउ का उद्धार कब एवं किस स्थल पर किया?
हमारा अनुमान है कि महाकवि सिद्ध एवं महाकवि सिंह के काल में अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोनों कवियों की गुरु-परम्परा निश्चित रूप से मलधरी देवोपासक रही है। सिद्ध ने अपने गुरु का नाम अमयचन्द बताया है जबकि सिंह ने अमियचन्द अथवा अमियमयद । अपभ्रंश-व्याकरण के नियमानुसार '' स्वर का परिवर्तन 'अ' एवं 'इ' दोनों स्वरों में होता है। कवि छन्द एवं मात्रा तथा श्रुतिमधुरताः को ध्यान में रख कर उक्त स्वर का परिवर्तन कर उसका प्रयोग कर लेता है। अत: अमयचन्दु, अमियचन्द्र एवं अमियमयंकु (मयंक चन्द्र) वस्तुत: एक ही हैं। अन्त्य-प्रशस्ति में 'मलधारिदेव (15/29/5) विशेषण अमियचंदु के गुरु माहवयंदु का ही विशेषण समझना चाहिए। अत: यह प्रतीत होता है कि पज्जुण्णचरिउ की रचना-समाप्ति के बाद सिद्ध कवि का सम्भवत: स्वर्गवास हो गया होगा और किसी प्राकृतिक प्रकोप के कारण पज्जुण्णचरिउ का कुछ अंश नष्ट या विगलित हो गया होगा, जिसकी प्रथम 8 सन्धियाँ तो सुविधापूर्वक ठीक कर ली गयी होंगी किन्तु बाकी की 7 सन्धियों को पूर्णतया विगलित या नष्ट देख कर गुरु अमृतचन्द्र ने सिंह कवि को उसके उद्धार का आदेश दिया होगा।
दि हमारा उक्त अनुमान सही है तो सिद्ध और सिंह दोनों सतीर्थ सिद्ध होते हैं। सिंह ने पज्जुण्णचरिउ का उद्धार बम्हडवाडपट्टन में ही किया होगा क्योंकि पूर्व में लिखा जा चुका है कि उस समय अमृतचन्द्र बम्हणवाडपट्टन में रह रहे थे। ___आद्य-प्रशस्ति में सिद्ध कवि द्वारा उल्लिखित माहवचन्दु, बल्लाल, भुल्लण जैसे व्यक्तियों के उल्लेख सिंह कवि ने सम्भवत: पुनरुक्ति दोष से बचने की दृष्टि से ही नहीं किये हैं। वस्तुत: वे सभी प्रसंग-प्राप्त सिद्ध होते हैं। __ अत: इन तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रद्युम्नचरित का रचनाकाल 12वीं सदी का तीसरा चरण था। उसका उद्धारकाल अनुमानत: 12वीं सदी का अन्तिम चरण अथवा तेरहवीं सदी का प्रारम्भिक चरण रहा होगा। उद्धार-स्थल भी अन्य सक्षम प्रमाणों के मिलने तक बम्हणवाइपट्टन ही समझना चाहिए। 11. अपभ्रंश-साहित्य की प्रवृत्तियाँ
महाकवि सिद्ध का अभ्युदय उस काल में हुआ. जब अपभ्रंश-साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त लेखन-कार्य हो चुका था। काव्य के विविध रूपों का भी विकास हो चुका था एवं परवर्ती अपभ्रंश-कवि उनसे अनुप्राणित हो रहे थे। महाकवि सिद्ध के समय में जिन काव्य-रूपों एवं शैलियों का विकास हो चुका था, उनका वर्गीकरण निम्नप्रकार किया जा सकता है ।
3 420 15:29:37। 2. ही01:46 1. बलो. 15:29:22। 4. वही0. 15529:46। 5. दे० र०Fu0प
वाली 1974, पृ. 12}।