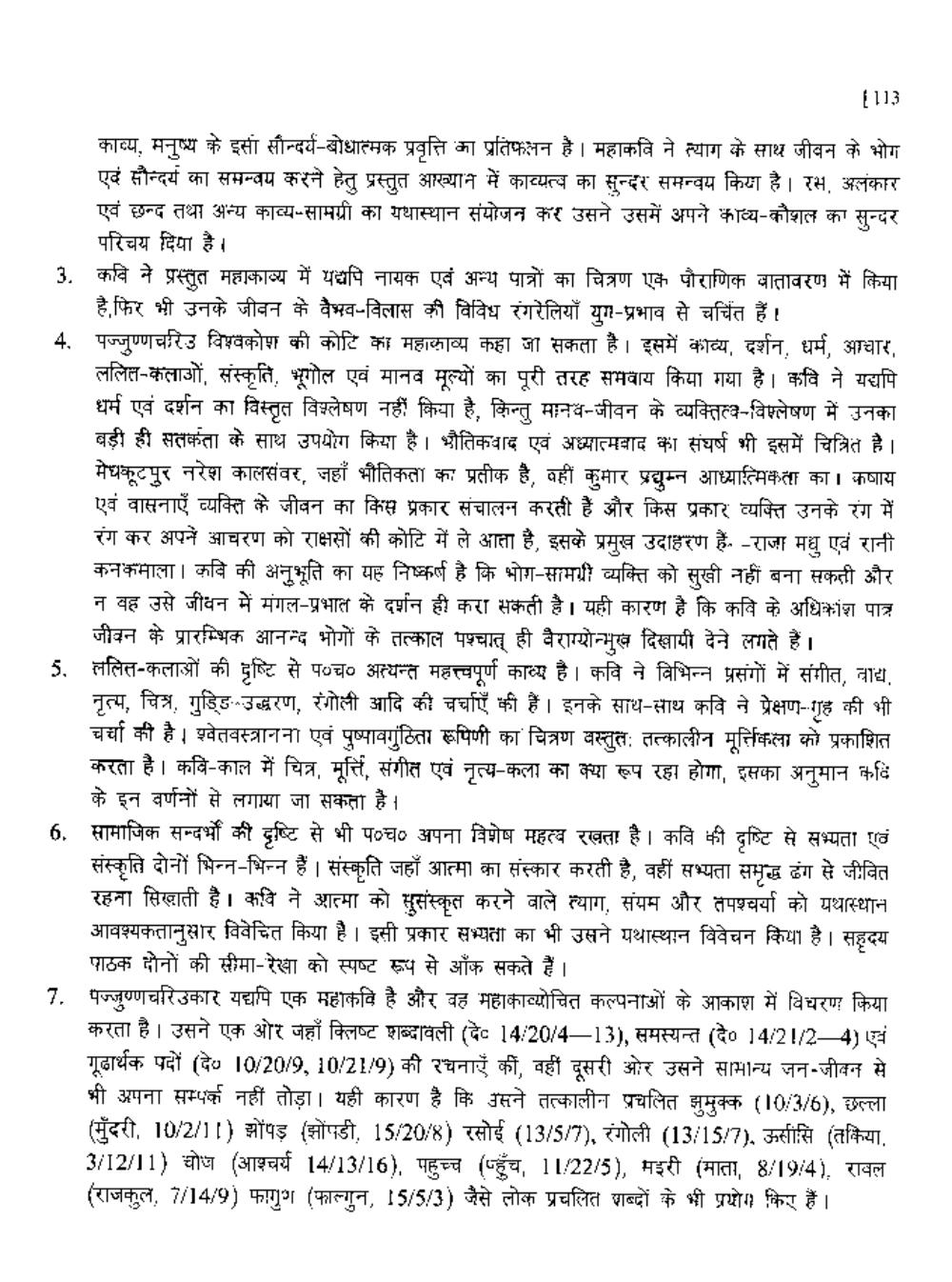________________
1113
काव्य, मनुष्य के इसी सौन्दर्य-बोधात्मक प्रवृत्ति का प्रतिफलन है। महाकवि ने त्याग के साथ जीवन के भोग एवं सौन्दर्य का समन्वय करने हेतु प्रस्तुत आख्यान में काव्यत्व का सुन्दर समन्वय किया है। रस, अलंकार एवं छन्द तथा अन्य काव्य-सामग्री का यथास्थान संयोजन कर उसने उसमें अपने काव्य-कौशल का सुन्दर
परिचय दिया है। 3. कवि ने प्रस्तुत महाकाव्य में यद्यपि नायक एवं अन्य पात्रों का चित्रण एक पौराणिक वातावरण में किया
है, फिर भी उनके जीवन के वैभव-विलास की विविध रंगरेलियाँ युग-प्रभाव से चर्चित हैं। 4, पज्जुण्णचरिउ विश्वकोश की कोटि का महाकाव्य कहा जा सकता है। इसमें काव्य, दर्शन, धर्म, आचार,
ललित-कलाओं, संस्कृति, भूगोल एवं मानव मूल्यों का पूरी तरह समवाय किया गया है। कवि ने यद्यपि धर्म एवं दर्शन का विस्तृत विश्लेषण नहीं किया है, किन्तु मानव-जीवन के व्यक्तित्व-विश्लेषण में उनका बड़ी ही सतर्कता के साथ उपयोग किया है। भौतिकवाद एवं अध्यात्मबाद का संघर्ष भी इसमें चित्रित है। मेघकूटपुर नरेश कालसंवर, जहाँ भौतिकता का प्रतीक है, वहीं कुमार प्रद्युम्न आध्यात्मिकता का। कषाय एवं वासनाएँ व्यक्ति के जीवन का किस प्रकार संचालन करती हैं और किस प्रकार व्यक्ति उनके रंग में रंग कर अपने आचरण को राक्षसों की कोटि में ले आता है, इसके प्रमुख उदाहरण हैं. - राजा मधु एवं रानी कनकमाला। कवि की अनुभूति का यह निष्कर्ष है कि भोग-सामग्री व्यक्ति को सुखी नहीं बना सकती और न वह उसे जीवन में मंगल-प्रभात के दर्शन ही करा सकती है। यही कारण है कि कवि के अधिकांश पात्र
जीवन के प्रारम्भिक आनन्द भोगों के तत्काल पश्चात् ही वैराग्योन्मुख दिखायी देने लगते हैं। 5. ललित-कलाओं की दृष्टि से प०च० अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काव्य है। कवि ने विभिन्न प्रसंगों में संगीत, वाद्य.
नृत्य, चित्र, गुड्डि उद्धरण, रंगोली आदि की चर्चाएँ की हैं। इनके साथ-साथ कवि ने प्रेक्षण-गृह की भी चर्चा की है। श्वेतवस्त्रानना एवं पुष्पावगुंठिता रूपिणी का चित्रण वस्तुत: तत्कालीन मूर्तिकला को प्रकाशित करता है। कवि-काल में चित्र, मूर्ति, संगीत एवं नृत्य-कला का क्या रूप रहा होगा, इसका अनुमान कदि
के इन वर्णनों से लगाया जा सकता है। 6. सामाजिक सन्दर्भो की दृष्टि से भी प०च० अपना विशेष महत्व रखता है। कवि की दृष्टि से सभ्यता एवं
संस्कृति दोनों भिन्न-भिन्न हैं। संस्कृति जहाँ आत्मा का संस्कार करती है, वहीं सभ्यता समृद्ध ढंग से जीवित रहना सिखाती है। कवि ने आत्मा को सुसंस्कृत करने वाले त्याग, संयम और तपश्चर्या को यथास्थान आवश्यकतानुसार विवेचित किया है। इसी प्रकार सभ्यता का भी उसने यथास्थान विवेचन किया है। सहृदय
पाठक दोनों की सीमा-रेखा को स्पष्ट रूप से आँक सकते हैं। 7. पज्जुण्णचरिउकार यद्यपि एक महाकवि है और वह महाकाव्योचित कल्पनाओं के आकाश में विधरण किया
करता है। उसने एक ओर जहाँ क्लिष्ट शब्दावली (दे० 14:20/4-13), समस्यन्त (दे० 14:21/2–4) एवं गूढार्थक पदों (दे० 10/20/9, 10/21/9) की रचनाएँ कीं, वहीं दूसरी ओर उसने सामान्य जन-जीवन से भी अपना सम्पर्क नहीं तोड़ा। यही कारण है कि उसने तत्कालीन प्रचलित झुमुक्क (103/6), छल्ला (मुंदरी, 10/2/11) झोंपड़ (झोंपडी, 15/20/8) रसोई (13/5/7), रंगोली (13/15/7), ऊसांसि (तकिया, 3/12/11) चोष (आश्चर्य 14/13/16), पहुच्च (पहुँच, 112215), मइरी (माता, 8194), रावल (राजकुल, 7/14/9) फागुण (फाल्गुन, 15/5/3) जैसे लोक प्रचलित शब्दों के भी प्रयोग किर हैं।