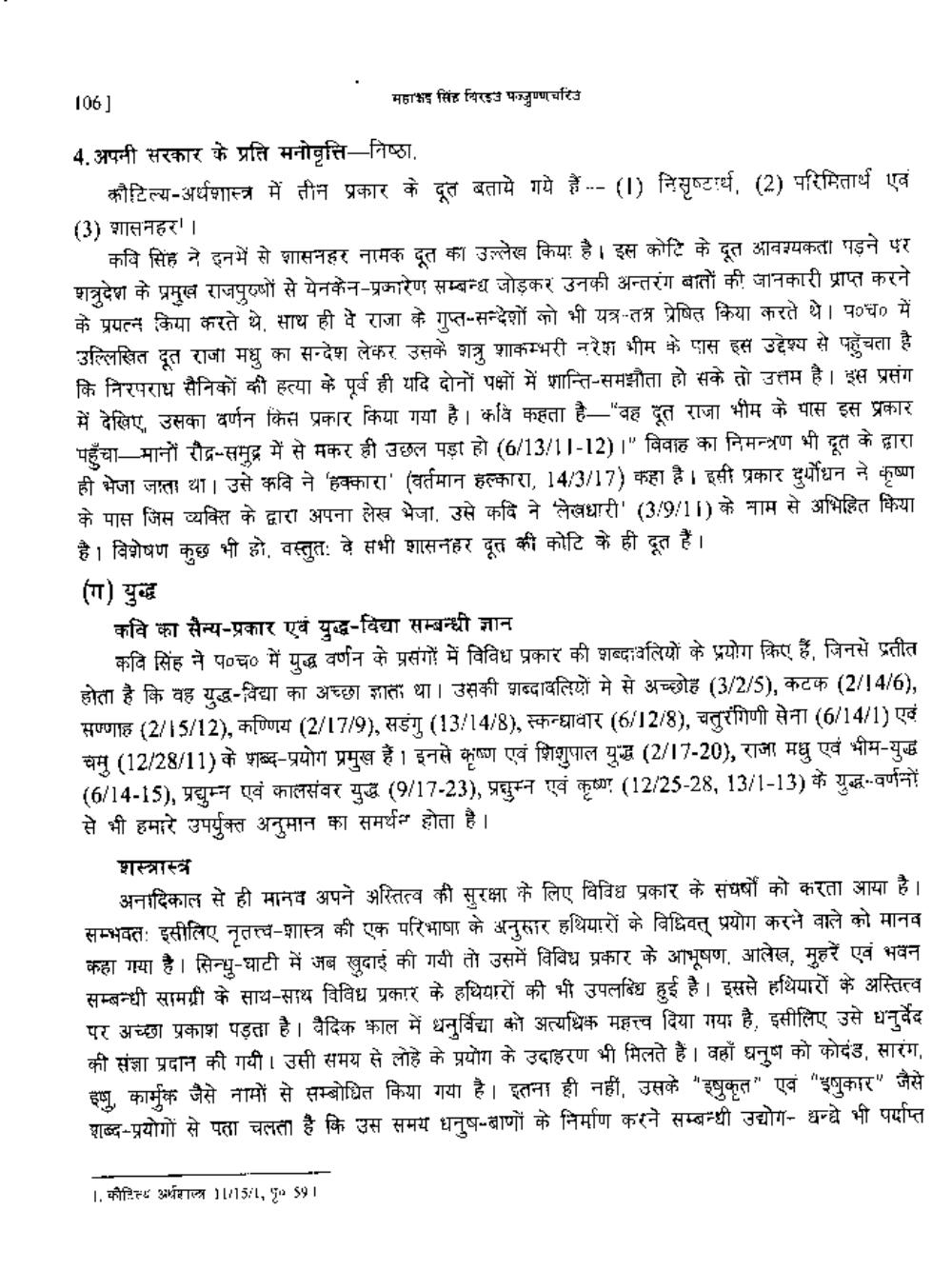________________
106]
महाभ सिंह विरइज पज्जुण्णचरित
4. अपनी सरकार के प्रति मनोवृत्ति-निष्ठा.
कौटिल्य-अर्थशास्त्र में तीन प्रकार के दूत बताये गये हैं ..- (I) निसृष्टार्थ, (2) परिमितार्थ एवं (3) शासनहर।।
कवि सिंह ने इनमें से शासनहर नामक दूत का उल्लेख किया है। इस कोटि के दूत आवश्यकता पड़ने पर शत्रुदेश के प्रमुख राजपुरुषों से येनकेन-प्रकारेण सम्बन्ध जोड़कर उनकी अन्तरंग बातों की जानकारी प्राप्त करने के प्रयत्न किया करते थे. साथ ही वे राजा के गुप्त-सन्देशों को भी यत्र-तत्र प्रेषित किया करते थे। पाच) में उल्लिखित दूत राजा मधु का सन्देश लेकर उसके शत्रु शाकम्भरी नरेश भीम के पास इस उद्देश्य से पहुंचता है कि निरपराध सैनिकों की हत्या के पूर्व ही यदि दोनों पक्षों में शान्ति-समझौता हो सके तो उत्तम है। इस प्रसंग में देखिए, उसका वर्णन किस प्रकार में टेखिए उसका वर्णन किस प्रकार किया गया है। कवि कहता है"वह दत राजा भीम के पास इस प्रकार पहुँचा—मानौं रौद्र-समुद्र में से मकर ही उछल पड़ा हो (6/13/11-12)।" विवाह का निमन्त्रण भी दूत के द्वारा ही भेजा जाता था। उसे कवि ने 'हक्कारा' (वर्तमान हल्कारा, 14/3/17) कहा है। इसी प्रकार दुर्योधन ने कृष्णा के पास जिस व्यक्ति के द्वारा अपना लेख भेजा. उसे कवि ने 'लेखधारी' (3:9:11) के नाम से अभिहित किया है। विशेषण कुछ भी हो. वस्तुत: वे सभी शासनहर दूत की कोटि के ही दूत हैं। (ग) युद्ध
कवि का सैन्य-प्रकार एवं युद्ध-विद्या सम्बन्धी ज्ञान
कवि सिंह ने प०च० में युद्ध वर्णन के प्रसंगों में विविध प्रकार की शब्दावलियों के प्रयोग किए हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि वह युद्ध-विद्या का अच्छा ज्ञाता था। उसकी शब्दावलियों मे से अच्छोह (3/2/5), कटक (2/14/6), सण्णाह (2/15/12), कण्णिय (2/17/9), सडंगु (13/14/8), स्कन्धावार (6/12/8), चतुरंगिणी सेना (6/14/1) एवं चमु (12/28/11) के शब्द-प्रयोग प्रमुख हैं। इनसे कृष्ण एवं शिशुपाल युद्ध (2/17-20), राजा मधु एवं भीम-युद्ध (6/14-15), प्रद्युम्न एवं कालसंवर युद्ध (9/17-23), प्रद्युम्न एवं कृष्ण (12/25-28, 13/1-13) के युद्ध वर्णनों से भी हमारे उपर्युक्त अनुमान का समर्थन होता है।
शस्त्रास्त्र
अनादिकाल से ही मानव अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए विविध प्रकार के संघर्षों को करता आया है। सम्भवतः इसीलिए नृतत्त्व-शास्त्र की एक परिभाषा के अनुसार हथियारों के विधिवत् प्रयोग करने वाले को मानव कहा गया है। सिन्धु-घाटी में जब खुदाई की गयी तो उसमें विविध प्रकार के आभूषण, आलेख, मुहरें एवं भवन सम्बन्धी सामग्री के साथ-साथ विविध प्रकार के हथियारों की भी उपलब्धि हुई है। इससे हथियारों के अस्तित्व पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। वैदिक काल में धनुर्विद्या को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है, इसीलिए उसे धनुर्वेद की संज्ञा प्रदान की गयी। उसी समय से लोहे के प्रयोग के उदाहरण भी मिलते हैं। वहाँ धनुष को कोदंड, सारंग, इषु, कार्मुक जैसे नामों से सम्बोधित किया गया है। इतना ही नहीं, उसके "इषुकृत" एवं "इशुकार" जैसे शाब्द-प्रयोगों से पता चलता है कि उस समय धनुष-बाणों के निर्माण करने सम्बन्धी उद्योग- धन्ये भी पर्याप्त
1. कौडित अर्थशला 11151, पृ. 591