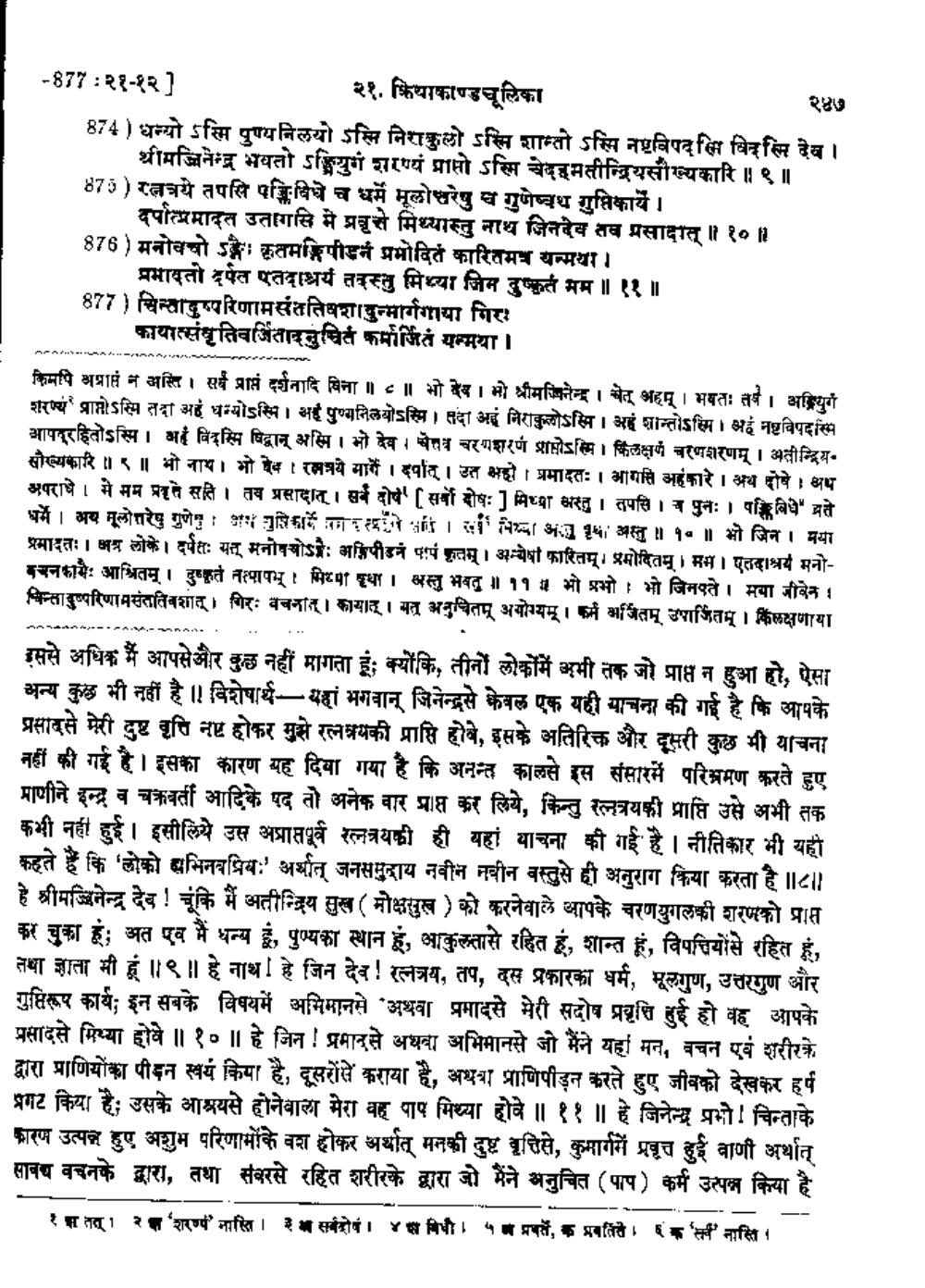________________
-877 :२१-१२] २१. क्रियाकाण्डचूलिका
२४७ 874 ) धन्यो ऽस्मि पुण्यनिलयो ऽस्मि निराकुलो ऽस्मि शाम्तो ऽसि नविपदसि विस्मि देव ।
श्रीमज्जिनेन्द्र भवतो ऽप्रियुगं शरण्यं प्राप्तोऽस्मि चेदहमतीन्द्रियसौख्यकारि ॥ ९ ॥ 875) रत्नत्रये तपसि पजिविधे च धर्मे मूलोस्तरेषु च गुणेष्वथ गुप्तिकायें।
दर्पात्प्रमादत उतागसि मे प्रवृसे मिथ्यास्तु नाथ जिनदेव तव प्रसादात् ॥ १०॥ 876) मनोवचो ऽहैः कृतमङ्गिपीडनं प्रमोदितं कारितमत्र यन्मया।
प्रमावतो दर्पत एतदाश्रयं तदस्तु मिथ्या जिम दुष्कृतं मम ॥ ११ ॥ 877) चिन्तादुष्परिणामसंततिषशावुन्मार्गगाया गिरर
फायात्संवृतिवर्जितावनुचितं कर्मार्जितं यन्मया ।
किमपि अप्राप्त अस्ति। सर्व प्राप्त दर्शनादि चिना ॥ ८॥ भो देव । भो श्रीमजिनेन्द्र । चेत् अहम् । भवतः तः। अभियुर्ग शरण्य प्राप्तोऽस्मि तदा अहं धन्योऽस्मि । अई पुण्यनिलयोऽस्मि। तदा अढू निराकुल्योऽस्मि । अहं शान्तोऽस्मि । अहं मष्टविपदाम आपदरहितोऽस्मि। अहं विदस्मि विद्वान् अस्ति । भो देव । तव चरमशरण शोऽस्मि । किलक्षणे चरणशरणम् । अतीन्द्रियसौख्यकारि ॥५॥ भो नाथ। भो वेद । रसत्रये मार्ग । दात् । उत महो। प्रमादतः । आगति अहंकारे । अथ दोथे। अब अपराधे। मे मम प्रवृते सति । तय प्रसादात् । सर्व दोषे [ सर्वो दोषः] मिथ्या अस्तु । तपसि। पुनः। पद्धिविधे" ते धर्मे । अय मूलोत्तरेषु गुणेषु । अधिकार हो । सीमिया या अस्तु ॥ १०॥ भो जिन । मया प्रमादतः । अत्र लोके। दर्पतः यत् मनोपयोऽऔः अङ्गिपीडनं पापं कृतम् । अन्येषां कारितम्। प्रमोदितम । मम । एतदाश्रय मनोपरनकामः आश्रितम् । दुरुकृतं नापम् । मिरमा कृथा । बस्तु भवतु ॥ 1१३ भो प्रभो। भो जिमयते । मया जीवन। चिन्तादुष्परिणामसंततिक्शात् । गिरः वचनात् । कायात् । मतु अनुचितम् अयोग्यम् । कर्म अर्जितम् उपार्जितम् । विलक्षणाया
इससे अधिक मैं आपसे और कुछ नहीं मागता इं; क्योंकि, तीनों लोकोंमें अभी तक जो प्राप्त न हुआ हो, ऐसा अन्य कुछ भी नहीं है ।। विशेषार्थ-यहां भगवान् जिनेन्द्रसे केवल एक यही याचना की गई है कि आपके प्रसादसे मेरी दुष्ट वृत्ति नष्ट होकर मुझे रत्नत्रयकी प्राप्ति होवे, इसके अतिरिक्त और दूसरी कुछ भी याचना नहीं की गई है। इसका कारण यह दिया गया है कि अनन्त कालसे इस संसारमें परिश्रमण करते हुए माणीने इन्द्र व चक्रवर्ती आदिके पद तो अनेक वार प्राप्त कर लिये, किन्तु रत्नत्रयकी प्राप्ति उसे अभी तक कभी नहीं हुई । इसीलिये उस अप्राप्तपूर्व रत्नत्रयकी ही यहां याचना की गई है । नीतिकार भी यही कहते हैं कि 'लोको अभिनवप्रियः' अर्थात् जनसमुदाय नवीन नवीन वस्तुसे ही अनुराग किया करता है ॥८॥ हे श्रीमजिनेन्द्र देव ! चूंकि मैं अतीन्द्रिय सुख ( मोक्षसुख ) को करनेवाले आपके चरणयुगलकी शरमको प्राप्त कर चुका हूं; अत एव मैं धन्य ई, पुण्यका स्थान हूं, आकुलतासे रहित हूं, शान्त हूं, विपचियोंसे रहित हूं, तथा ज्ञाता भी हूं ॥९॥ हे नाथ! हे जिन देव ! रत्नत्रय, तप, दस प्रकारका धर्म, मूलगुण, उत्तरगुण और गुप्तिरूप कार्य; इन सबके विषयमें अमिमानसे अथवा प्रमादसे मेरी सदोष प्रवृत्ति हुई हो वह आपके प्रसादसे मिथ्या होवे ॥ १० ॥ हे जिन ! प्रभारसे अथवा अभिमानसे जो मैंने यहां मन, वचन एवं शरीरके द्वारा प्राणियोंका पीदन स्वयं किया है, दूसरों से कराया है, अथवा प्राणिपीड़न करते हुए जीवको देखकर हर्प प्रगट किया है; उसके आश्रयसे होनेवाला मेरा वह पाप मिथ्या होवे ।। ११ ॥ हे जिनेन्द्र प्रभो! चिन्ताके कारण उत्पन्न हुए अशुभ परिणामोंके वश होकर अर्थात् मनकी दुष्ट वृत्तिसे, कुमार्गमें प्रवृत्त हुई वाणी अर्थात् सावध वचनके द्वारा, तथा संवरसे रहित शरीरके द्वारा जो मैंने अनुचित (पाप) कर्म उत्पन्न किया है
सतत् । २ 'शरप' मास्ति । ३ ॥ सर्वदोष । ४क्ष विधी । ५० प्रचतें, क प्रवर्तिते । ६ क ' नास्ति ।