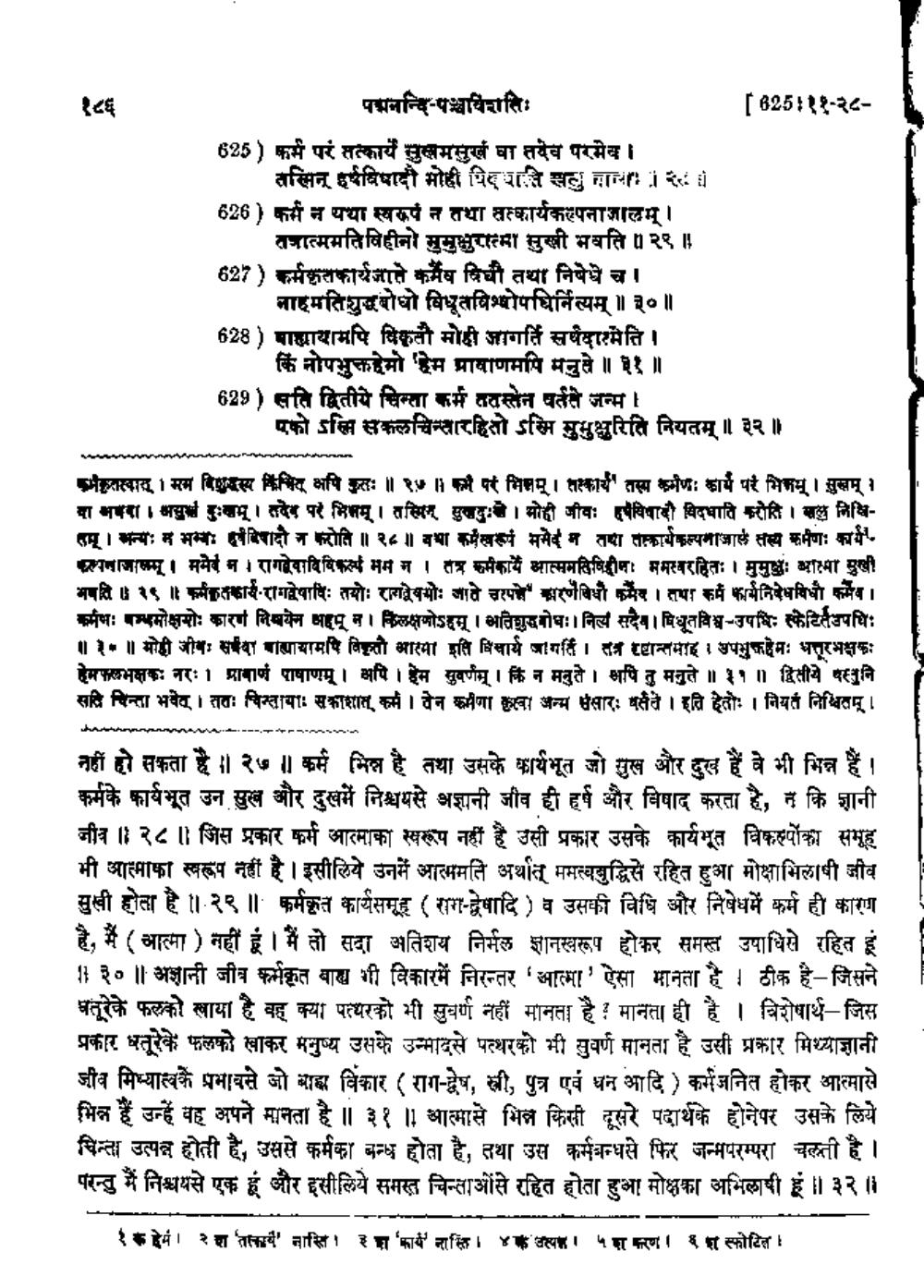________________
पअनन्दि-पञ्चविंशतिः
[825:११-२८625) कर्म परं तत्कायें सुलमसुर्ख वा तदेव परमेव ।
तसिन् इविधादी मोही विशात सतु माया । 626) कर्म न यथा स्वरूपं न तथा सत्कार्यकरपनाजालम् ।
तत्रात्ममतिविहीनो मुमुक्षुरात्मा सुखी भवति ॥ २९ ।। 627) कर्मकृतकार्यजाते कमेष विधी तथा निषेधे च ।
माहमतिशुद्धोधो विधूतविश्वोपधिनित्यम् ॥ ३०॥ 628 ) पाह्यायामपि विकृती मोही जागर्ति सदारमेति ।
किं मोपभुक्तहेमो 'हम प्रायाणमपि मनुते ॥ ३१॥ 629) सति द्वितीये चिन्ता कर्म ततस्तेन वर्तते जन्म ।
'पको ऽस्मि सकलचिन्तारहितोऽस्मि मुमुक्षुरिति नियतम् ॥ ३२ ॥
महतस्यात् । मम विशुदस्य निमित् अपि कुतः ॥ १५ ॥ फर्म पर मिलम् । तत्कार्य तस्म कर्मणः कार्य पर भिनम् । सुखम् । वा भावा । असुख दुःखम् । तदेव पर मिलम् । तस्मिन् सुखदुःखे । मोही जीवः हविषादी विदधाति करोति । मल निधिहसामन्यः मम्मा विषादौनकरोति ॥ २०॥ वथा कर्मखरूपं ममेदम तथा तस्कार्यकल्पनाजाल तस्य कर्मणः कार्य कल्पनाजालम् । ममेवे म । रागदेवाविविकल्प मम म । तत्र कर्मकार्य आत्ममविविडीमः ममस्वरहितः । मुमुक्षुः आत्मा मुखी भवति ॥ १९ ॥ कर्मकतकार्य रामद्वेषादिः तयोः रागद्वेषयोः जावे चरपो कारणेविधौ कमैर । तथा कर्म कार्मनिवेधविधी कमेव । कर्मणः पम्पमोक्षः कारगं निषयेन महम् म । किलक्षणोऽहम् । भविशुखबोषः। नित्यं सदैव विधूतविश्व-उपधिः स्केटितउपपिः ॥३॥ मोही जीवः सर्वथा बाह्यायामपि विस्तौ मारमा इति बिचार्य जागर्ति । तत्र रटान्तमाह । उपभुकदमः भत्तूरभक्षका हेमफलभक्षक नरः। प्रावाणं पाषाणम् । अपि । हेम सुवर्णम् । किं न मन्ते । अपि तु मनुते ॥ १॥ द्वितीये वस्तुनि सति चिन्ता भवेत् । ततः चिन्तायाः सकाशात् कर्म । वेन समेगा कृत्वा जन्म सारः वसते । इति हेतोः । नियत निश्चितम् ।
नहीं हो सकता है ॥ २७ ॥ कर्म भिन्न है तथा उसके कार्यभूत जो सुख और दुख हैं वे भी भिन्न हैं। कर्मके कार्यभूत उन सुख और दुखमें निश्चयसे अज्ञानी जीव ही हर्ष और विषाद करता है, न कि ज्ञानी जीव ।। २८ ।। जिस प्रकार कर्म आत्माका स्वरूप नहीं है उसी प्रकार उसके कार्यभूत विकल्पोंका समूह मी आत्माफा स्वरूप नहीं है । इसीलिये उनमें आत्ममति अर्थात् ममत्वबुद्धिसे रहित हुआ मोक्षाभिलाषी जीव सुखी होता है ॥२२॥ कर्मकृत कार्यसमूह ( राग-द्वेषादि) व उसकी विधि और निषेध कर्म ही कारण है, मैं (आत्मा) नहीं हूं। मैं तो सदा अतिशय निर्मल ज्ञानस्वरूप होकर समस्त उपाधिसे रहित हूं ॥ ३० ॥ अज्ञानी जीव कर्मकृत बाह्य भी विकारमें निरन्तर 'आत्मा' ऐसा मानता है । ठीक है-जिसने धतूरेके फलको खाया है वह क्या पत्थरको भी सुवर्ण नहीं मानता है। मानता ही है। विशेषार्थ-जिस प्रकार धतूरेके फलको खाकर मनुष्य उसके उन्मादसे पत्थरको भी सुवर्ण मानता है उसी प्रकार मिथ्याज्ञानी जीव मिथ्यात्वके प्रभावसे जो बाह्य विकार ( राग-द्वेष, स्त्री, पुत्र एवं धन आदि ) कर्मजनित होकर आत्मासे भिन्न हैं उन्हें वह अपने मानता है ।। ३१ ॥ आत्मासे भिन्न किसी दूसरे पदार्थके होनेपर उसके लिये चिन्ता उत्पन्न होती है, उससे कर्मका बन्ध होता है, तथा उस कर्मबन्धसे फिर जन्मपरम्परा चलती है। परन्तु मैं निश्चयसे एक हूं और इसीलिये समस्त चिन्ताओंसे रहित होता हुआ मोक्षका अभिलाषी हूं ।। ३२ ।।
१० हेमं। २ शतका' नास्ति। ३श 'कार्य' नास्ति। ४ उत्प। ५श करण। ६श स्फोटित ।