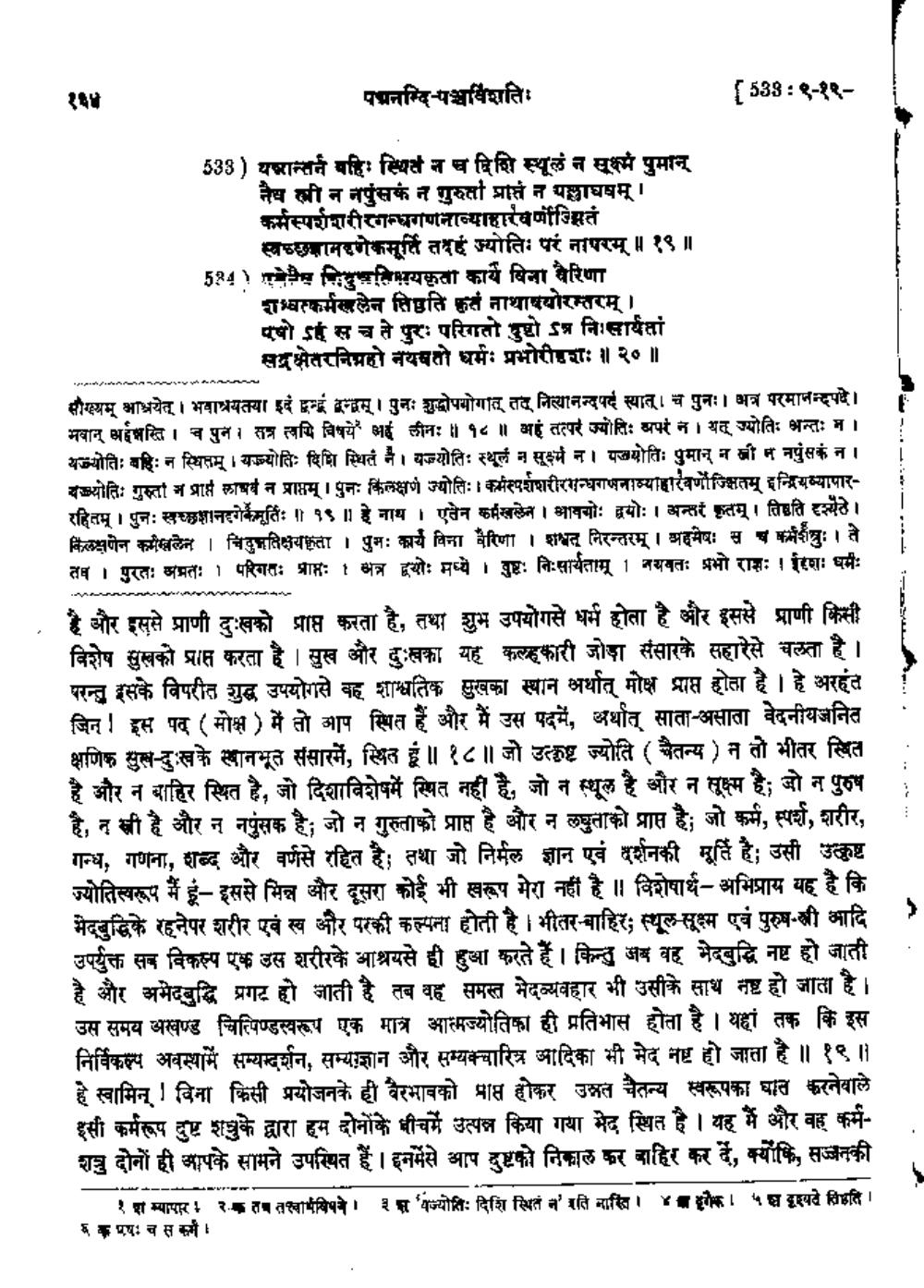________________
१६४
पद्मनन्दि-पञ्चविंशतिः
538 ) यान्त बहिः स्थितं न च दिशि स्थूलं न सूक्ष्मं पुमान् नैव स्त्री न नपुंसकं न गुरुतो प्राप्तं न पल्लाघषम् । कर्मस्पर्शशरीरगन्धगणनान्याहारेवणज्झितं स्वच्छज्ञामवणेकमूर्ति तदहं ज्योतिः परं नापरम् ॥ १९ ॥ 584) यकृता कार्य बिना वैरिणा शश्वत्कर्मखलेन तिष्ठति कृतं नाथावयोरन्तरम् । एषोऽहं सच से पुरः परिगतो तुष्टो ऽत्र निःसार्यतां सद्र क्षेतरनिग्रहो नयवतो धर्मः प्रभोरीदृशः ॥ २० ॥
[533 : ९-११
सौम् श्रयेत् । भवाश्रयतया इदं द्वन्द्वन्द्वम् । पुनः शुद्धोपयोगात् तद् नित्यानन्दपदं स्यात् । च पुनः । अत्र परमानन्दपदे । भवान् अस्ति । च पुन सत्र त्वयि विषये अई लीनः ॥ १८ ॥ अहं तत्परं ज्योतिः अपरं न यत् ज्योतिः अन्तः म । यज्योतिः बहिः न स्थितम् । यज्योतिः दिशि स्थितं नै । यज्योतिः स्थूलं न सूक्ष्मं न यजयोतिः पुमान् न स्त्री न नपुंसकं न । वख्योतिः गुरुतां न प्राप्त लाभ न प्राप्तम् । पुनः किंलक्षणे ज्योतिः । कर्मस्पर्शशरीरमन्धगणनाव्याहारवणज्शितम् इन्द्रियव्यापाररहितम् । पुनः स्वच्छशानदगेमूर्तिः ॥ १९ ॥ हे नाथ । एतेन कर्मखलेन । आवयोः द्वयोः । अन्तरं कृतम् । तिष्ठति दृश्यैते । किलक्षणेन कमैम्बलेन । चिदुमतिक्षयकृता । पुनः कार्य विना वैरिणा । शश्वत् निरन्तरम् । श्रहमेषः स च कर्मत्रुः । ते तव । पुरतः अमतः । परिगतः प्राप्तः । अत्र द्वयोः मध्ये । दुष्टः निःसार्यताम् । नयवतः प्रभो राशः । ईदृशः धर्मः
१ श व्यापार ६ क एषः च स कर्म
3
है और इससे प्राणी दुःखको प्राप्त करता है, तथा शुभ उपयोगसे धर्म होता है और इससे प्राणी किसी विशेष सुखको प्राप्त करता है। सुख और दुःखका यह कलहकारी जोड़ा संसारके सहारेसे चलता है । परन्तु इसके विपरीत शुद्ध उपयोगसे वह शाश्वतिक सुखका स्थान अर्थात् मोक्ष प्राप्त होता है । हे अरहंत जिन | इस पद (मोक्ष) में तो आप स्थित हैं और मैं उस पदमें, अर्थात् साता - असाता वेदनीयजनित क्षणिक सुख-दुःख के स्थानभूत संसारमें स्थित हूं ॥ १८ ॥ जो उत्कृष्ट ज्योति ( चैतन्य ) न तो भीतर स्थित है और न बाहिर स्थित है, जो दिशाविशेषमें स्थित नहीं है, जो न स्थूल है और न सूक्ष्म है; जो न पुरुष है, न स्त्री है और न नपुंसक है; जो न गुरुताको प्राप्त है और न लघुताको प्राप्त है; जो कर्म, स्पर्श, शरीर, गन्ध, गणना, शब्द और वर्णसे रहित है तथा जो निर्मल ज्ञान एवं दर्शनकी मूर्ति है; उसी उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप मैं हूं - इससे भिन्न और दूसरा कोई भी स्वरूप मेरा नहीं है । विशेषार्थ- अभिप्राय यह है कि भेदबुद्धिके रहनेपर शरीर एवं स्व और परकी कल्पना होती है। भीतर बाहिर; स्थूल सूक्ष्म एवं पुरुष - श्री आदि उपर्युक्त सब विकल्प एक उस शरीरके आश्रयसे ही हुआ करते हैं । किन्तु अब वह भेदबुद्धि नष्ट हो जाती है और अमेदबुद्धि प्रगट हो जाती है तब वह समस्त भेदव्यवहार भी उसीके साथ नष्ट हो जाता है। उस समय अखण्ड चित्पिण्डस्वरूप एक मात्र आत्मज्योतिका ही प्रतिभास होता है। यहां तक कि इस निर्विकल्प अवस्था में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र आदिका भी मेद नष्ट हो जाता है ॥ १९ ॥ हे स्वामिन् ! बिना किसी प्रयोजनके ही वैरभावको प्राप्त होकर उन्नत चैतन्य स्वरूपका घात करनेवाले इसी कर्मरूप दुष्ट शत्रुके द्वारा हम दोनोंके भीचमें उत्पन्न किया गया मेद स्थित है। यह मैं और वह कर्मशत्रु दोनों ही आपके सामने उपस्थित हैं। इनमें से आप दुष्टको निकाल कर बाहिर कर दें, क्योंकि, सज्जनकी
[२] तत्र तत्वार्थविभने । ३ ' वज्योतिः दिशि स्थितं न' इति नास्ति । ४ इक ५ दृश्यते तिष्ठति ।
।
}