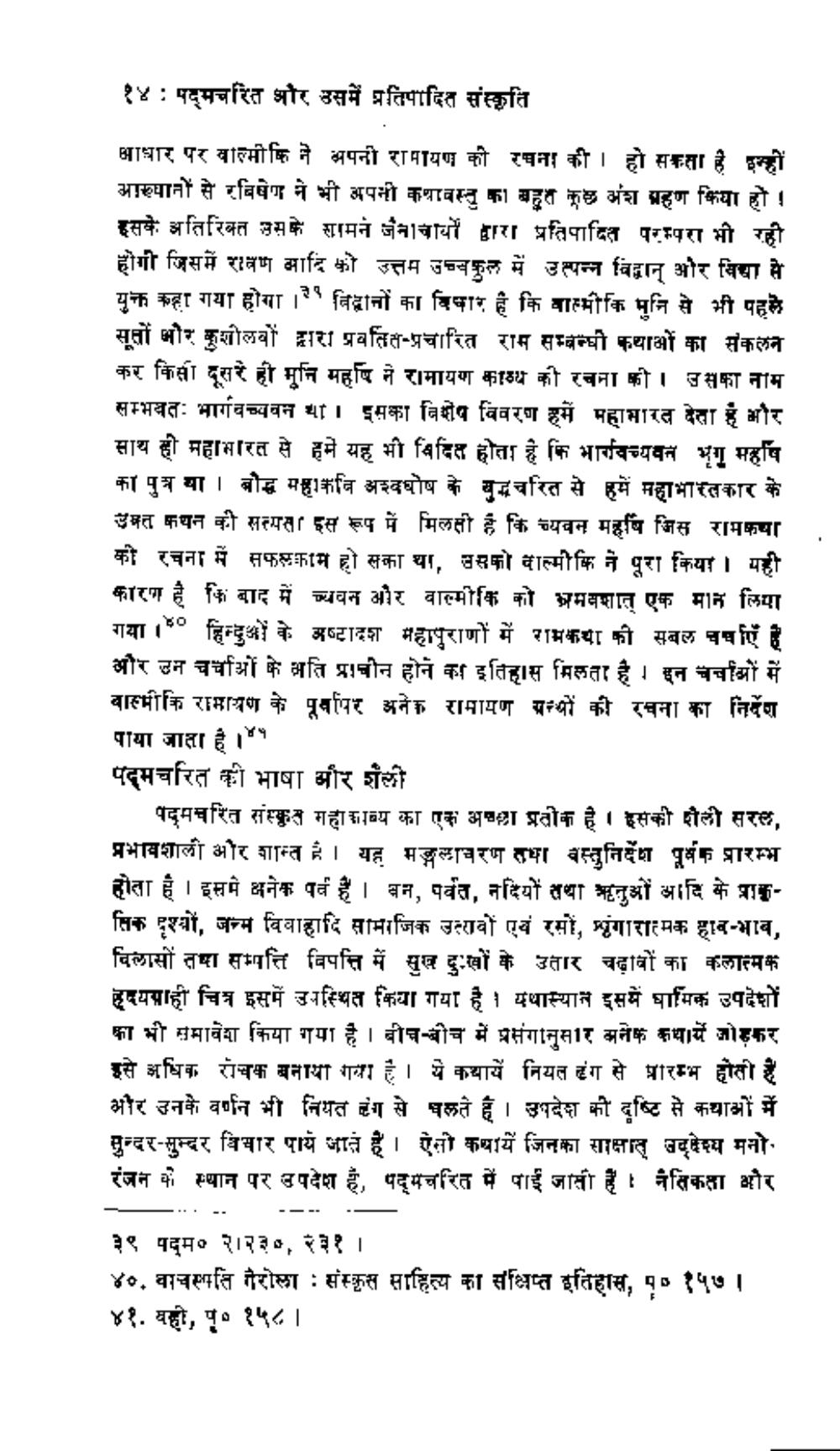________________
१४ पद्मचरित और उसमें प्रतिपादित संस्कृति
आधार पर वाल्मीकि ने अपनी रामायण की रचना की। हो सकता है इन्हीं आख्यानों से रविषेण ने भी अपनी कथावस्तु का बहुत कुछ अंश ग्रहण किया हो ! इसके अतिरिक्त उसके सामने जैनाचार्यों द्वारा प्रतिपादित परम्परा भी रही होगी जिसमें रावण मादि को उत्तम उच्चकुल में उत्पन्न विद्वान् और विद्या से युक्त कहा गया होगा । विद्वानों का विचार है कि वाल्मीकि मुनि से भी पहले सूतों और कुशीलवों द्वारा प्रवर्तित प्रचारित राम सम्बन्धी कथाओं का संकलन कर किसी दूसरे ही मुनि महर्षि ने रामायण काव्य की रचना की। उसका नाम सम्भवतः भार्गचच्यवन था। इसका विशेष विवरण हमें महाभारत देता है और साथ ही महाभारत से हमें यह भी विदित होता है कि भार्गवच्यवन भृगु महर्षि का पुत्र था। बौद्ध महाकवि अश्वघोष के बुद्धचरित से हमें महाभारतकार के उक्त कथन की सत्यता इस रूप में मिलती हैं कि व्यवन महर्षि जिस रामकथा की रचना में सफलकाम हो सका था, उसको वाल्मीकि ने पूरा किया। यही कारण है कि बाद में च्यवन और वाल्मीकि को भ्रमवशात् एक मान लिया गया । हिन्दुओं के अष्टादश महापुराणों में रामकथा की सबल वर्षाएँ है और उन चर्चाओं के अति प्राचीन होने का इतिहास मिलता है। इन चर्चाओं में बाल्मीकि रामायण के पूर्वापर अनेक रामायण ग्रन्थों की रचना का निर्देश पाया जाता है । ४५
४०
पद्मचरित की भाषा और शैली
पद्मचरित संस्कृत महाकाव्य का एक अच्छा प्रतीक है। इसकी शैली सरल, प्रभावशाली और शान्त है। यह मङ्गलाचरण तथा वस्तुनिर्देश पूर्वक प्रारम्भ होता है । इसमें अनेक पर्व हैं। वन, पर्वत, नदियों तथा ऋतुओं आदि के प्राकृ तिक दृश्यों, जन्म विवाहादि सामाजिक उत्सवों एवं रसों, श्रृंगारात्मक हाव-भाव, विलासों तथा सम्पत्ति विपत्ति में सुख दुःखों के उतार चढ़ावों का कलात्मक हृदयग्राही चित्र इसमें उपस्थित किया गया है । यथास्थान इसमें धार्मिक उपदेशों का भी समावेश किया गया है। बीच-बीच में प्रसंगानुसार अनेक कथायें जोड़कर इसे अधिक रोचक बनाया गया है। ये कथायें नियत ढंग से प्रारम्भ होती हैं और उनके वर्णन भी नियत ढंग से चलते हैं । उपदेश की दृष्टि से कथाओं में सुन्दर सुन्दर विचार पायें जाते हैं। ऐसी कथायें जिनका साक्षात् उद्देश्य मनो रंजन के स्थान पर उपदेश है, पद्मचरित में पाई जाती है। नैतिकता और
३९ पद्म० २।२३०, २३१ ।
४०. वाचस्पति गैरोला संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, पृ० १५७ । ४१. वही, पृ० १५८ |