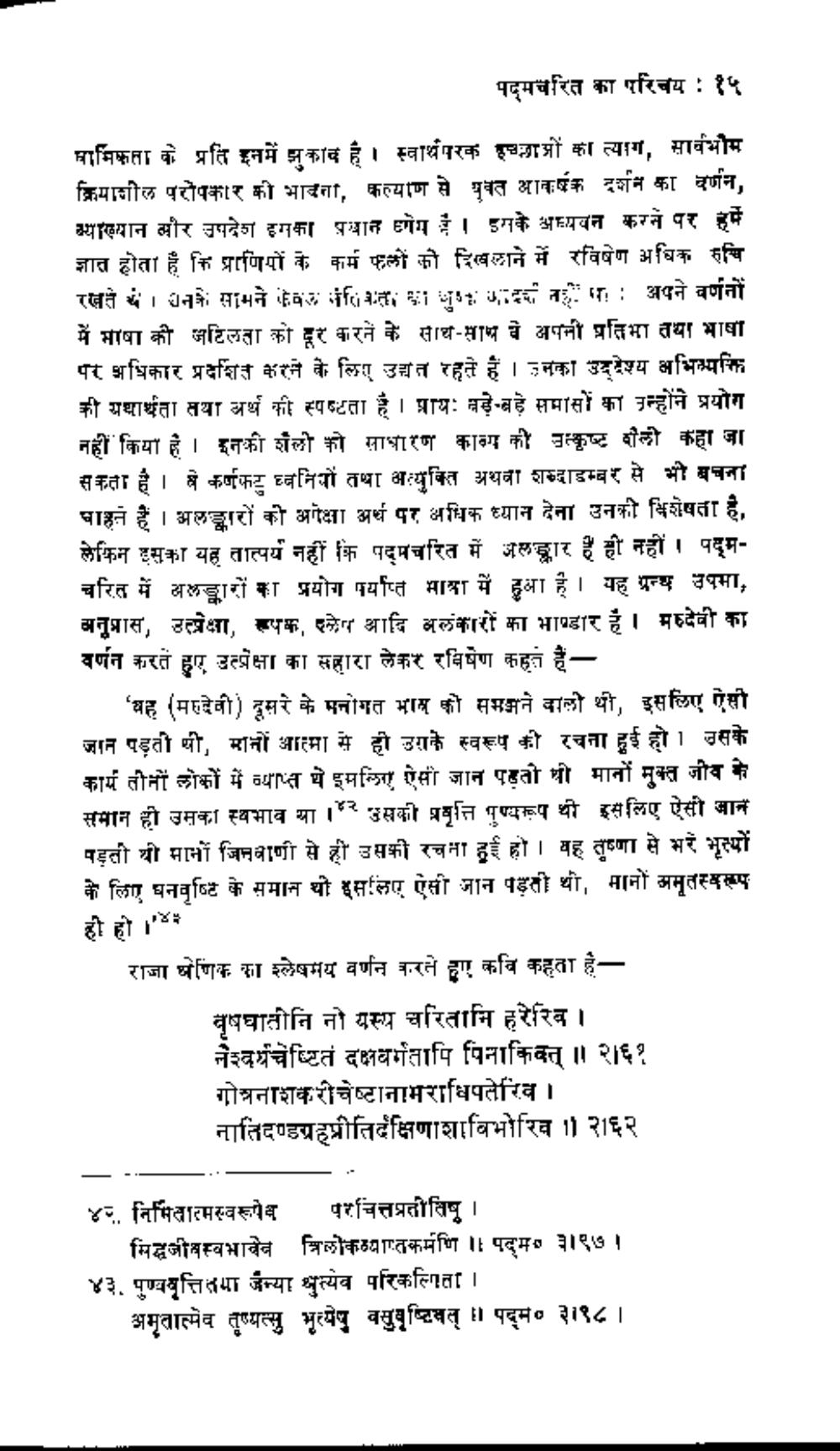________________
पद्मचरित का परिचय : १५
घामिफप्ता के प्रति इनमें झुकाव है। स्वार्थपरक इच्छाओं का त्याग, सार्वभौम क्रियाशील परोपकार की भावना, कल्याण से युक्त आकर्षक दर्शन का वर्णन, व्याख्यान सौर उपदेश हमका प्रधान होय है। इसके अध्ययन करने पर हमें ज्ञात होता है कि प्राणियों के कर्म फलों को दिखलाने में रविषेण अधिक रुचि रखते थे। उनमें सामने पल बिता का शु दर्श नहीं पा : अपने वर्णनों में भाषा की जटिलता को दूर करने के साथ-साथ वे अपनी प्रतिभा तथा भाषा पर अधिकार प्रदर्शित करने के लिए उच्यत रहते हैं। उनका उद्देश्य अभिव्यक्ति की अथार्थता तथा अर्थ की स्पष्टता है। प्रायः बड़े-बड़े समासों का उन्होंने प्रयोग नहीं किया है। इनकी शैली को साधारण काव्य की उत्कृष्ट दौली कहा जा सकता है। ये कर्णफट ध्वनियों तथा अत्युक्ति अथवा शम्दाडम्बर से भी बचना चाहते हैं । अलङ्कारों की अपेक्षा अर्थ पर अधिक ध्यान देना उनकी विशेषता है, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि पद्मचरित में अलङ्कार है ही नहीं। पद्मचरित में अलङ्कारों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में हुआ है। यह ग्रन्छ उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक, इलेप आदि अलंकारों का भाण्डार है। महदेवी का वर्णन करते हुए उत्प्रेक्षा का सहारा लेकर रविषेण कहते हैं
'वह (मएदेवी) दुसरे के मनोगत मात्र को समझने वाली थी, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी, मानों आत्मा में ही उसके स्वरूप को रचना हुई हो। उसके कार्य तीनों लोकों में व्याप्त थे इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानों मुक्त जीव के समान ही उसका स्वभाव या । १२ उसकी प्रवृत्ति पुण्यरूप थी इसलिए ऐसी जान पढ़ती थी मानों जिनवाणी से ही उसकी रचना हुई हो। यह तृष्णा से भरे भृत्यों के लिए धनवृष्टि के समान थी इसलिए ऐसी जान पड़ती थी, मानों अमृतस्वरूप ही हो ।'४५ राजा णिक का श्लेषमय वर्णन करते हुए कवि कहता है
वृषघातीनि नो यस्य चरितानि हरेरिव । नैश्वर्थचेष्टितं दक्षवतापि पिनाकिवत् ॥ २०६१ गोत्रनाशकरीचेष्टानामराधिपतेरिव । नातिदण्डग्रहप्रीतिक्षिणाशाविभोरिव ।) २१६२
४६. निर्मितारमस्वरूपेव परचित्तप्रतीतिषु ।
मिद्धजीवस्वभावेव त्रिलोकव्याप्तकर्मणि ।। पद्मा ३।९७ । ४३. पुण्यवृत्तितमा जन्या श्रुत्येव परिकलिगता ।
अमृतात्मैव तृष्यत्सु भृत्येषु वसुवृष्टिवत् ।। पद्म० ३३९८ ।