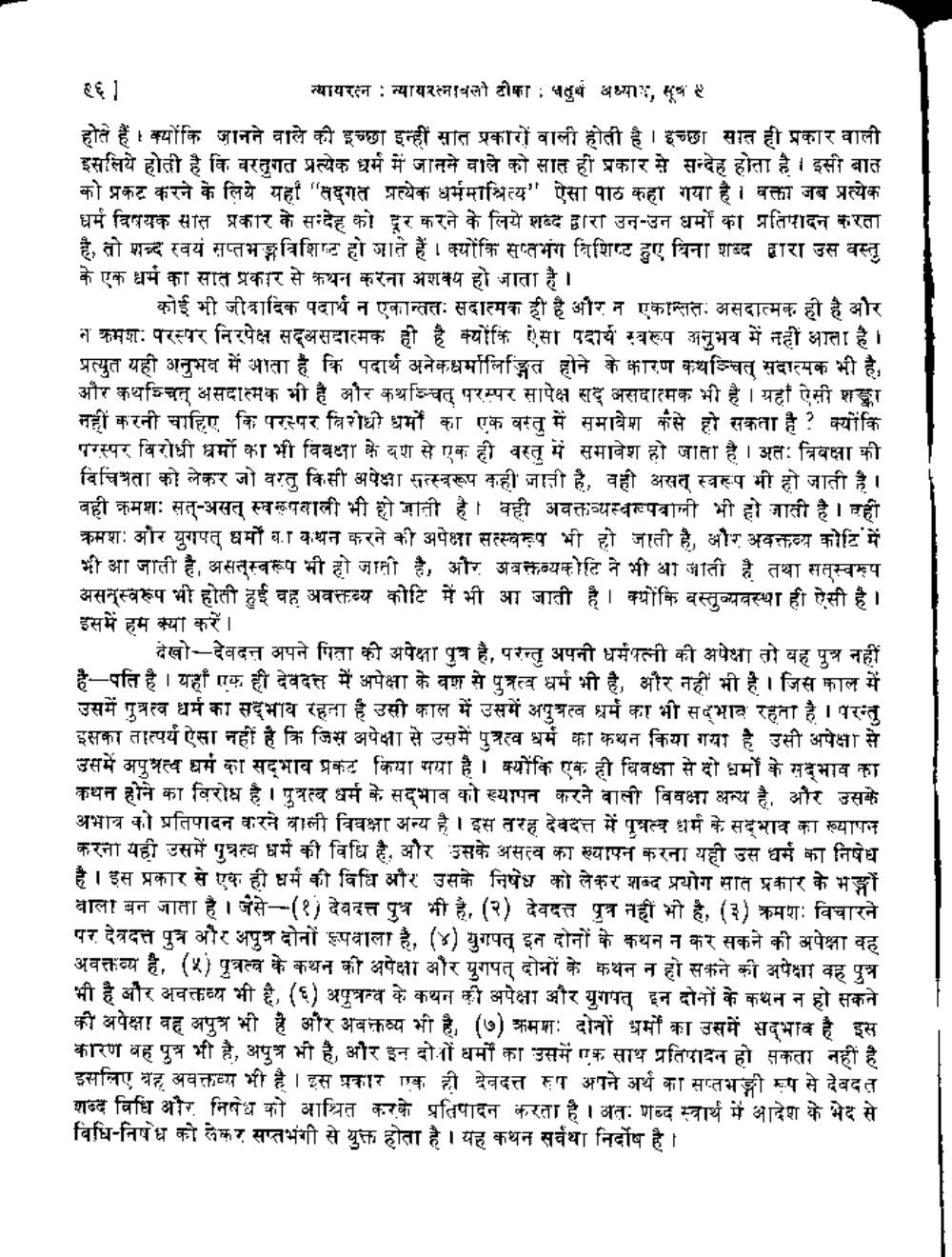________________
न्यायरत्न : न्यायरत्नावलो टीका : पतुर्थ अध्याः, सूत्र होते हैं। क्योंकि जानने वाले की इच्छा इन्हीं सात प्रकारों वाली होती है । इच्छा सात ही प्रकार वाली इसलिये होती है कि वरतुगत प्रत्येक धर्म में जानने वाले को सात ही प्रकार से सन्देह होता है। इसी बात को प्रकट करने के लिये यहाँ "तद्गत प्रत्येक धर्ममाश्रित्य" ऐसा पाठ कहा गया है। वक्ता जब प्रत्येक
यक सास प्रकार के सन्देन को दर करने के लिये शब्द द्वारा उन-उन धर्मों का प्रतिपादन करता है, तो शन्द स्वयं सप्तभङ्गविशिष्ट हो जाते हैं । क्योंकि सप्तभंग विशिष्ट हुए विना शब्द द्वारा उस वस्तु के एक धर्म का सात प्रकार से कथन करना अशक्य हो जाता है।
कोई भी जीवादिक पदार्थ न एकान्ततः सदात्मक ही है और न एकान्ततः असदात्मक ही है और न क्रमशः परस्पर निरपेक्ष सदअसदात्मक ही है क्योंकि ऐसा पदार्थ स्वरूप अनुभव में नहीं आता है। प्रत्युत यही अनुभव में आता है कि पदार्थ अनेकधर्मालिङ्गित होने के कारण कथञ्चित सदात्मक भी है, और कश्चित् असदात्मक भी है और कञ्चित् परम्पर सापेक्ष साद् असदात्मक भी है । यहाँ ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए कि परस्पर विरोधी धर्मों का एक वस्तु में समावेश कसे हो सकता है ? क्योंकि परस्पर विरोधी धर्मों का भी विवक्षा के वश से एक ही वस्तु में समावेश हो जाता है । अतः विवक्षा की विचित्रता को लेकर जो वरत किसी अपेक्षा सत्स्वरूप कही जाती है, वही असत स्वरूप भी हो जाती है। वही क्रमशः सत्-असत् स्वरूपाली भी हो जाती है। वही अवक्तव्यस्वरूपवानी भी हो जाती है। वहीं क्रमशः और युगपत् धमों या कथन करने की अपेक्षा सत्स्वरूप भी हो जाती है, और अवक्तव्य कोटि में भी आ जाती है, असत्स्वरूप भी हो जाती है, और अबक्तव्यकोटि ने भी आ जाती है तथा सत्स्वरूप असत्स्वरूप भी होती हुई वह अवक्तव्य कोटि में भी आ जाती है। क्योंकि वस्तुव्यवस्था ही ऐसी है। इसमें हम क्या करें।
देखो-देवदन अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है, परन्तु अपनी धर्मपत्नी की अपेक्षा तो बह पुत्र नहीं है-पति है । यहाँ एक ही देवदत्त में अपेक्षा के वश से पुत्रत्व धर्म भी है, और नहीं भी है। जिस काल में उसमें पुत्रत्व धर्म का सद्भाव रहता है उसी काल में उसमें अघुत्रत्व धर्म का भी सदभाव रहता है। परन्तु इसका तात्पर्य ऐसा नहीं है कि जिस अपेक्षा से उसमें पुत्रत्व धर्म का कथन किया गया है उसी अपेक्षा उसमें अपुत्रत्व धर्म का सद्भाव प्रकट किया गया है। क्योंकि एक ही विवक्षा से दो धर्मों के सद्भाव का कथन होने का विरोध है । पुत्रत्व धर्म के सद्भाव को ख्यापन करने वाली विवक्षा अन्य है, और उसके अभात्र को प्रतिपादन करने वाली विवक्षा अन्य है। इस तरह देवदत्त में पुत्रत्व धर्म के सद्भाव का ख्यापन करना यही उसमें पुत्रत्व धर्म की विधि है, और उसके असत्व का ख्यापन करना यही उस धर्म का निषेध है । इस प्रकार से एक ही धर्म की विधि और उसके निषेध को लेकर शब्द प्रयोग सात प्रकार के भङ्गों वाला बन जाता है । जैसे-(१) देवदत्त पुत्र भी है, (२) देवदत्त पुत्र नहीं भी है, (३) क्रमशः विचारने पर देवदत्त पुत्र और अपुत्र दोनों पवाला है, (४) युगपत् इन दोनों के कथन न कर सकने की अपेक्षा वह अवक्तव्य है, (५) पुत्रत्व के कथन की अपेक्षा और युगपत् दोनों के कथन न हो सकने की अपेक्षा वह पुत्र भी है और अवक्तव्य भी है, (६) अपुत्रत्व के कथन की अपेक्षा और युगपत् इन दोनों के कथन न हो सकने की अपेक्षा वह अपुत्र भी है और अबक्तव्य भी है, (७) क्रममाः दोनों धर्मों का उसमें सद्भाव है इस कारण बह पुत्र भी है, अपुत्र भी है, और इन दोनों धर्मों का उसमें एक साथ प्रतिपादन हो सकता नहीं है इसलिए बह अवक्तव्य भी है । इस प्रकार एक ही देवदत्त रूप अपने अर्थ का सप्तभङ्गी रूप से देवदत शब्द विधि और निषेध को आश्रित करके प्रतिपादन करता है । अतः शब्द स्वार्थ में आदेश के भेद से विधि-निषध को लेकर सप्तभंगी से युक्त होता है । यह कथन सर्वथा निर्दोष है।