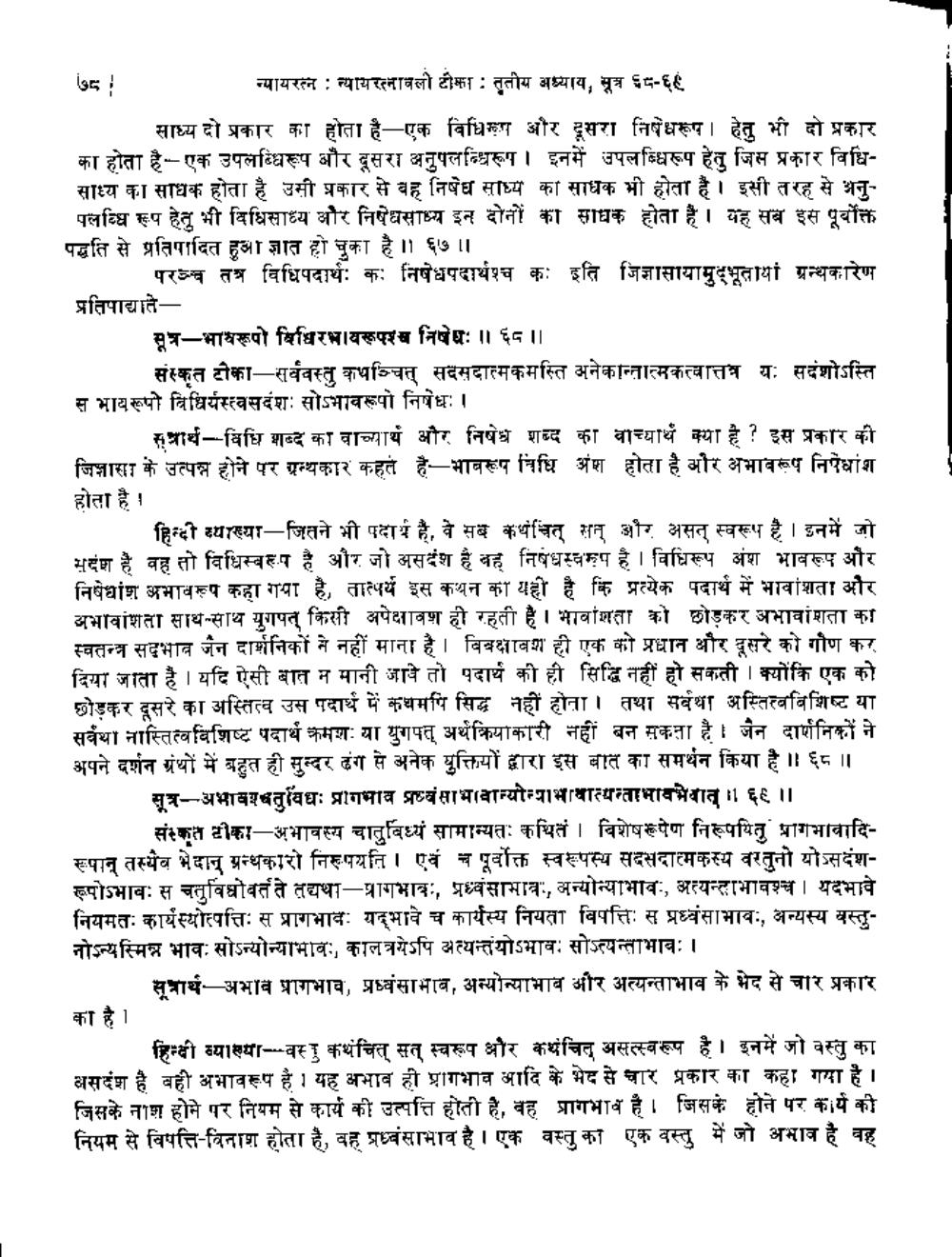________________
७८
न्यायरत्न : न्यायरत्नावली टीका : तृतीय अध्याय, मूत्र ६५-६६ साध्य दो प्रकार का होता है—एक विधिका और दूसरा निषेधरूप। हेतु भी दो प्रकार का होता है-एक उपलब्धिरूप और दूसरा अनुपलब्धिरूप। इनमें उपलब्धिरूप हेतु जिस प्रकार विधिसाध्य का साधक होता है उसी प्रकार से बह निषेध साध्य का साधक भी होता है। इसी तरह से अनुपलब्धि रूप हेतु भी विधिसाध्य और निषेधसाध्य इन दोनों का साधक होता है। यह सब इस पूर्वोक्त पद्धति से प्रतिपादित हुआ ज्ञात हो चुका है।। ६७ ।।
परञ्च तत्र विधिपदार्थः कः निषेधपदार्थश्च कः इति जिज्ञासायामुद्भूतायां ग्रन्थकारण प्रतिपाद्याते
सूत्र-भावरूपो विधिरभावरूपश्च निषेधः ।। ६५ ।।
संस्कृत टोका–सर्ववस्तु कञ्चित् सदसदात्मकमस्ति अनेकान्तात्मकत्वात्तत्र यः सदंशोऽस्ति स भायरूपो विधिर्यस्त्वसदंशः सोऽभावरूपो निषेधः ।
स्त्रार्थ-विधि शब्द का वाच्यार्थ और निषेध शब्द का वाच्यार्थ क्या है ? इस प्रकार की जिज्ञासा के उत्पन्न होने पर ग्रन्थकार कहत है—भावरूप विधि अंश होता है और अभावरूप निफ्धांश होता है।
हिन्दी व्याख्या-जितने भी पदार्थ है, वे सब कथंचित् सन् और असत् स्वरूप है । इनमें जो भदंश है वह तो विधिस्वरूप है और जो असदंश है वह निषधस्वरूप है । विधिरूप अंश भावरूप और निषेधांश अभावरूप कहा गया है, तात्पर्य इस कथन का यही है कि प्रत्येक पदार्थ में भावांशता और अभावांशता साथ-साथ यूगपत् किसी अपेक्षावश ही रहती है। भावांशता को छोड़कर अभावांशता का स्वतन्त्र सदभाव जैन दार्शनिकों ने नहीं माना है। विवक्षावश ही एक को प्रधान और दूसरे को गौण कर दिया जाता है । यदि ऐसी बात म मानी जाये तो पदार्थ की ही सिद्धि नहीं हो सकती । क्योंकि एक को छोड़कर दूसरे का अस्तित्व उस पदार्थ में कथमपि सिद्ध नहीं होता। तथा सर्वथा अस्तित्वविशिष्ट या सर्वथा नास्तित्वविशिष्ट पदार्थ क्रमशः या युगपत् अर्थक्रियाकारी नहीं बन सकता है। जैन दार्शनिकों ने अपने दर्शन ग्रंथों में बहुत ही सुन्दर ढंग से अनेक युक्तियों द्वारा इस बात का समर्थन किया है ॥ ६८ ।।
सूत्र-अभावश्चतुविधः प्रागभाव प्रध्वंसाभावान्योन्याभावात्यन्ताभावभेवात् ।। ६६ ।।
संस्कृत टीका-अभावस्य चातुविध्यं सामान्यतः कथितं । विशेषरूपेण निरूपयितु प्रागभावादिरूपान् तस्यैव भेदान् ग्रन्थकारो निरूपयति । एवं च पूर्वोक्त स्वरूपस्थ सदसदात्मकस्य वरतुनो योऽसदंशरूपोऽभावः स चतुर्विधोवर्तते तद्यथा-प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अन्योन्याभावः, अत्यन्टाभावश्च । यदभावे नियमतः कार्यस्योत्पत्तिः स प्रागभावः यद्भावे च कार्यस्य नियता विपत्तिः स प्रध्वंसाभावः, अन्यस्य यस्तुनोऽन्य स्मिन्न भावः सोऽन्योन्याभावः, कालत्रयेऽपि अत्यन्तयोऽभावः सोऽत्यन्ताभावः ।
सूत्रार्थ-अभाव प्रागभाव, प्रध्वंसाभाब, अन्योन्याभाब और अत्यन्ताभाव के भेद से चार प्रकार का है।
हिन्दी व्याख्या-वस्तु कथंचित् सत् स्वरूप और कथंचित् असत्स्वरूप है। इनमें जो वस्तु का असदंश है बही अभावरूप है । यह अभाव ही प्रागभाव आदि के भेद से चार प्रकार का कहा गया है। जिसके नाश होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है, वह प्रागभाव है। जिसके होने पर कार्य की नियम से विपत्ति-विनाश होता है, वह प्रध्वंसाभाव है । एक वस्तु का एक वस्तु में जो अभाव है वह