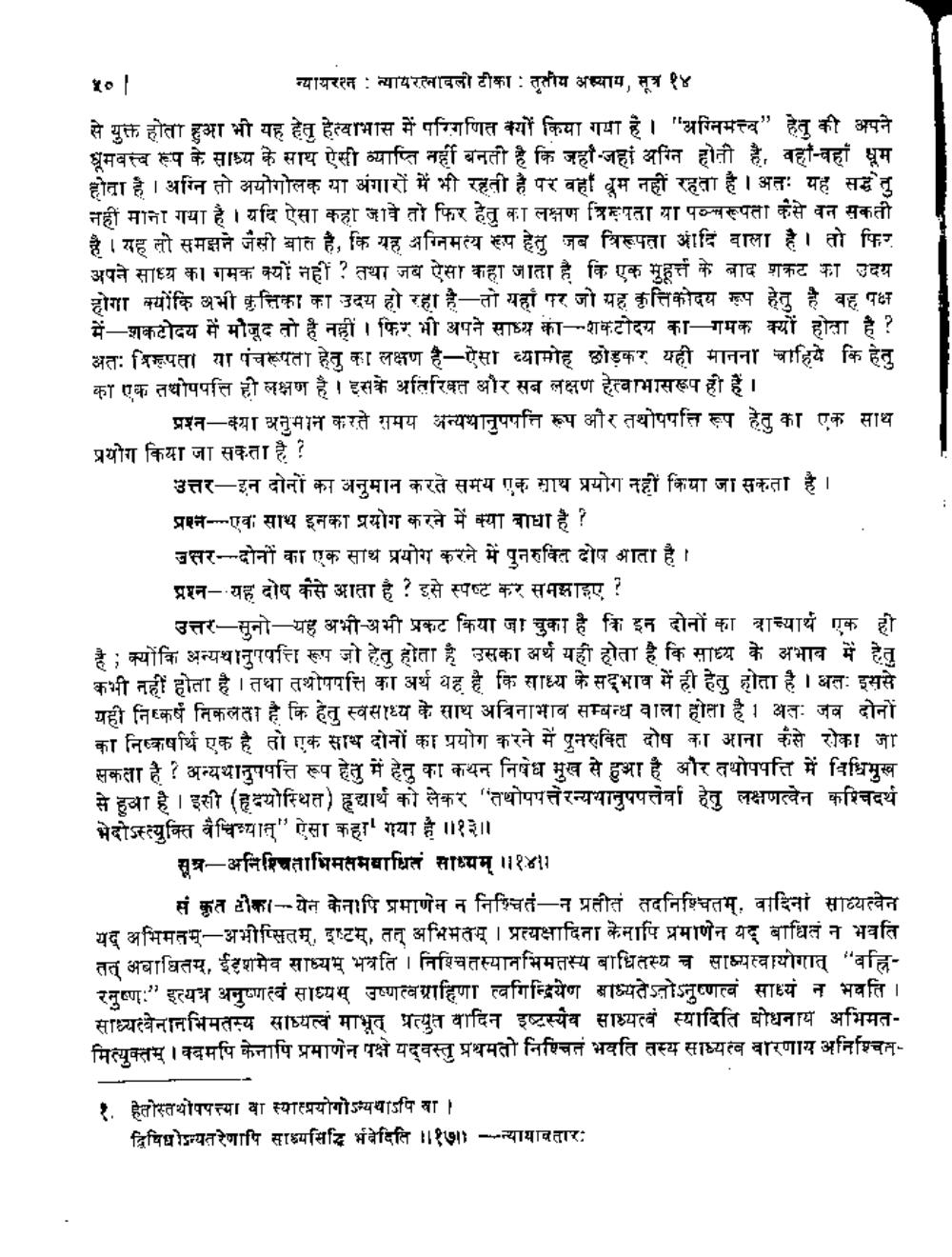________________
न्यायरत्न : न्यायरत्नावली टीका : तृतीय अध्याय, सूत्र १४ से युक्त होता हुआ भी यह हेतु हेत्वाभास में परिगणित क्यों किया गया है। "अग्निमत्त्व" हेतु की अपने धूमवत्त्व रूप के साक्ष्य के साथ ऐसी व्याप्ति नहीं बनती है कि जहाँ-जहां अग्नि होती है, वहां-वहाँ धूम होता है । अग्नि तो अयोगोलक या अंगारों में भी रहती है पर वहाँ दुम नहीं रहता है । अतः यह सतु नहीं माना गया है । यदि ऐसा कहा जावे तो फिर हेतु का लक्षण त्रिरूपता या पञ्चरूपता कैसे बन सकती है । यह तो समझने जैसी बात है, कि यह अग्निमत्य रूप हेतु जब विरूपता आदि बाला है। तो फिर अपने साध्य का गमक क्यों नहीं ? तथा जब ऐसा कहा जाता है कि एक मुहूर्त के बाद शकट का उदय होगा क्योंकि अभी कृत्तिका का उदय हो रहा है तो यहाँ पर जो यह कृत्तिकोदय रूप हेतु है वह पक्ष में शकटोदय में मौजूद तो है नहीं । फिर भी अपने साध्य का-शक्टोदय का गमक क्यों होता है ? अतः विरूपता या पंचरूपता हेतु का लक्षण है-ऐसा व्यामोह छोडकर यही मानना चाहिये कि हेत का एक तथोपपत्ति ही लक्षण है । इसके अतिरिक्त और सब लक्षण हेत्वाभासरूप ही हैं।
प्रश्न-क्या अनुमान करते समय अन्यथानुपपत्ति रूप और तथोपपत्ति रूप हेतु का एक साथ प्रयोग किया जा सकता है ?
उत्तर-इन दोनों का अनुमान करते समय एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न- एक साथ इनका प्रयोग करने में क्या बाधा है ? उत्तर-दोनों का एक साथ प्रयोग करने में पुनरुक्ति दोष आता है। प्रश्न- यह दोष कैसे आता है ? इसे स्पष्ट कर समझाइए?
उत्तर-सुनो-यह अभी-अभी प्रकट किया जा चुका है कि इन दोनों का वाच्यार्थ एक ही है ; क्योंकि अन्यथानुपपत्ति रूप जो हेतु होता है उसका अर्थ यही होता है कि साध्य के अभाव में हेतु कभी नहीं होता है । तथा तथोपपत्ति का अर्थ यह है कि साध्य के सद्भाव में ही हेतु होता है । अतः इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि हेतु स्वसाध्य के साथ अविनाभाव सम्बन्ध वाला होता है। अतः जब दोनों का निष्कर्षार्थ एक है तो एक साथ दोनों का प्रयोग करने में पुनरुक्ति दोष का आना कसे रोका जr सकता है ? अन्यथानुपपत्ति रूप हेतु में हेतु का कथन निषेध मुख से हुआ है और तथोपपत्ति में विधिमूत्र से हया है । इसी (हृदयोस्थित) हृद्यार्थ को लेकर "तथोपपत्तेरन्यथानुपपत्तेर्वा हेतु लक्षणत्वेन कश्चिदर्थ भेदोऽस्त्युक्ति वैचिभ्यान्" ऐसा कहा गया है ।।१३।।
सूत्र-अनिश्चिताभिमतमबाधितं साध्यम् ॥१४१५
सं कृत टीका-येन केनापि प्रमाणेन न निश्चितं न प्रतीत सदनिश्चितम्, वादिना साध्यत्वेन यद् अभिमतम्-अभीप्सितम्, इष्टम्, तत् अभिमतम् । प्रत्यक्षादिना केनापि प्रमाणेन यद् बाधितं न भवति तत् अबाधितम्, ईदशमेव साध्यम् भवति । निश्चितस्यानभिमतस्य बाधितस्य च साध्यत्वायोगात् "वह्रिरनुष्णः" इत्यत्र अनुष्णत्वं साध्यम् उष्णत्वग्राहिणा त्वगिन्द्रियेण बाध्यतेऽतोऽनुष्णत्वं साध्यं न भवति । साध्यत्वेनानभिमतस्य साध्यत्वं माभूत् प्रत्युत वादिन इष्टस्यैव साध्यत्वं स्यादिति बोधनाय अभिमतमित्युक्तम् । क्वमपि केनापि प्रमाणेन पक्षे यद्वस्तु प्रथमतो निश्चितं भवति तस्य साध्यत्व वारणाय अनिश्चित
१. हतोस्तथोपपत्त्या वा स्यात्प्रयोगोऽन्यथाऽपि वा।
विषिधोडन्यतरेणापि साध्यसिद्धि भवेदिति ॥१७॥ --न्यायावतार: