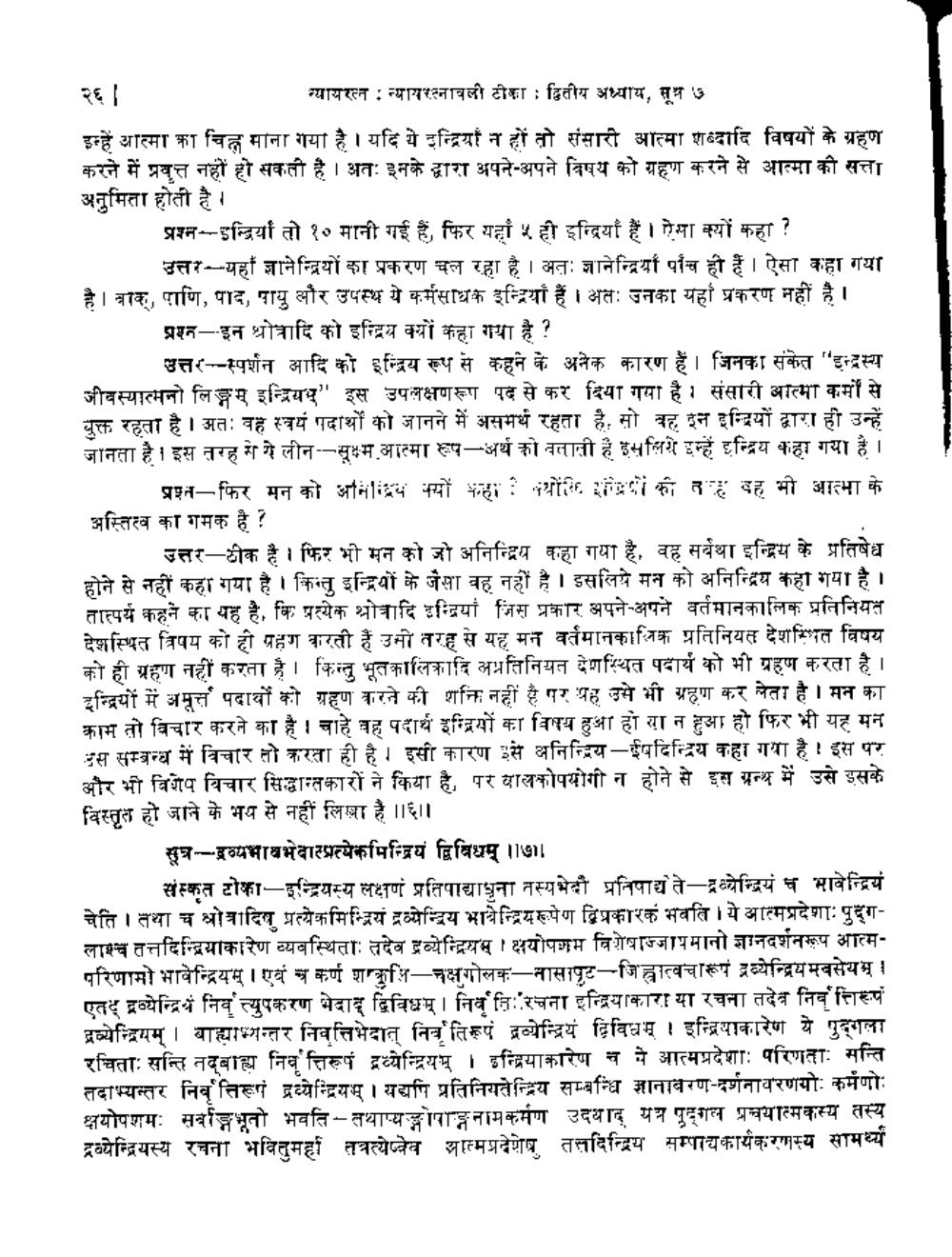________________
ग्यायरत्न : न्यायरत्नावली टीका : द्वितीय अध्याय, सूत्र ७ इन्हें आत्मा का चिह्न माना गया है। यदि ये इन्द्रियों न हों तो संसारी आत्मा शब्दादि विषयों के ग्रहण करने में प्रवृत्त नहीं हो सकती है । अतः इनके द्वारा अपने-अपने विषय को ग्रहण करने से आत्मा की सत्ता अनुमिता होती है।
प्रश्न---इन्द्रियाँ तो १० मानी गई हैं, फिर यहाँ ५ ही इन्द्रियाँ हैं । ऐसा क्यों कहा?
उत्तर- यहाँ ज्ञानेन्द्रियों का प्रकरण चल रहा है । अतः ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच ही हैं । ऐसा कहा गया है। बाक्, पाणि, पाद, 'पायु और उपस्थ ये कर्मसाधक इन्द्रियाँ हैं । अतः उनका यहाँ प्रकरण नहीं है।
प्रश्न-इन श्रोत्रादि को इन्द्रिय क्यों कहा गया है ?
उत्तर-स्पर्शन आदि को इन्द्रिय रूप से कहने के अनेक कारण हैं। जिनका संकेत "इन्द्रस्य जीवस्यात्मनो लिङ्गम् इन्द्रिय' इस उपलक्षणरूप पद से कर दिया गया है। संसारी आत्मा को से बुक्त रहता है । अतः वह स्वयं पदार्थों को जानने में असमर्थ रहता है. सो वह इन इन्द्रियों द्वारा ही उन्हें जानता है । इस तरह से ये लीन-सूक्ष्म आत्मा रूप-अर्थ को बताती है इसलिये इन्हें इन्द्रिय कहा गया है ।
प्रश्न-फिर मन को निद्रिय क्यों महायोगियों की तरह वह भी आत्मा के अस्तित्व का गमक है?
उत्तर-ठीक है। फिर भी मन को जो अनिन्द्रिय कहा गया है, वह सर्वथा इन्द्रिय के प्रतिषेध होने से नहीं कहा गया है। किन्तु इन्द्रियों के जैसा वह नहीं है। इसलिये मन को अनिन्द्रिय कहा गया है। तात्पर्य कहने का यह है, कि प्रत्येक श्रोत्रादि इन्द्रियां जिस प्रकार अपने-अपने वर्तमानकालिक प्रतिनियत देशस्थित विषय को ही ग्रहण करती हैं उमी तरह से यह मन वर्तमानकालिक प्रतिनियत देशस्थित विषय को ही ग्रहण नहीं करता है। किन्तु भूतकालिकादि अनतिनियत देशस्थित पदार्य को भी ग्रहण करता है। इन्द्रियों में अमूर्त पदावों को ग्रहण करने की शक्ति नहीं है पर यह उसे भी ग्रहण कर लेता है । मन का काम तो विचार करने का है। चाहे वह पदार्थ इन्द्रियों का विषय हुआ हा या न हुआ हो फिर भी यह मन उस सम्बन्ध में विचार तो करता ही है। इसी कारण इसे अनिन्द्रिय-ईषदिन्द्रिय कहा गया है । इस पर और भी विशेष विचार सिद्धान्तकारों ने किया है, पर बालकोपयोगी न होने से इस ग्रन्थ में उसे इसके विस्तृत हो जाने के भय से नहीं लिखा है ।।६।।
सूत्र-द्रव्यभावभेदारप्रत्येकमिन्द्रियं द्विविधम् ॥७॥ __ संस्कृत टोका-इन्द्रियस्य लक्षणं प्रतिपाद्याधुना नस्यभेदी प्रतिपाद्यते-द्रव्येन्द्रियं च भावेन्द्रियं चेति । तथा च श्रोत्रादिषु प्रत्येकमिन्द्रियं द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रियरूपेण द्विप्रकारकं भवति । ये आत्मप्रदेशाः पुद्गलाश्च तत्तदिन्द्रियाकारेण व्यवस्थिताः तदेव द्रव्येन्द्रियम् । क्षयोपगम विशेषाज्जाप मानो ज्ञानदर्शनरूप आत्मपरिणामो भावेन्द्रियम् । एवं त्र कर्ण शाक्रुषि-नक्षगोलक-नासापुट-जिह्वात्वचारूपं द्रव्येन्द्रियमबसेयम् । एतद् द्रव्येन्द्रियं नित्त्युपकरण भेदाद् द्विविधम् । निर्वनिरचना इन्द्रियाकारा या रचना तदेव निर्वृत्तिरूप द्रव्येन्द्रियम् । बाह्याभ्यन्तर निवृत्तिभेदात् नि तिरूपं द्रव्येन्द्रियं द्विविधम् । इन्द्रियाकारेण ये पुद्गला रचिताः सन्ति तदबाब निवृत्तिरूप द्रव्येन्द्रियम् । इन्द्रियाकारेण चचे आत्मनदेशा: परिणताः मन्ति तदाभ्यन्तर निर्वृत्तिरूप द्रव्येन्द्रियम् । यद्यपि प्रतिनियतेन्द्रिय सम्बन्धि ज्ञानाबरण-दर्शनावरणयोः कर्मणोः क्षयोपशमः सर्वाङ्गभूतो भवति - तथाप्यङ्गोपाङ्गनामकर्मण उदयाद् यत्र पुद्गल प्रचयात्मकस्य तस्य द्रव्येन्द्रियस्य रचना भवितुमहीं तत्रत्येष्वेव आत्मप्रदेशेषु ततदिन्द्रिय सम्पायकार्यकारणस्य सामर्थ्य