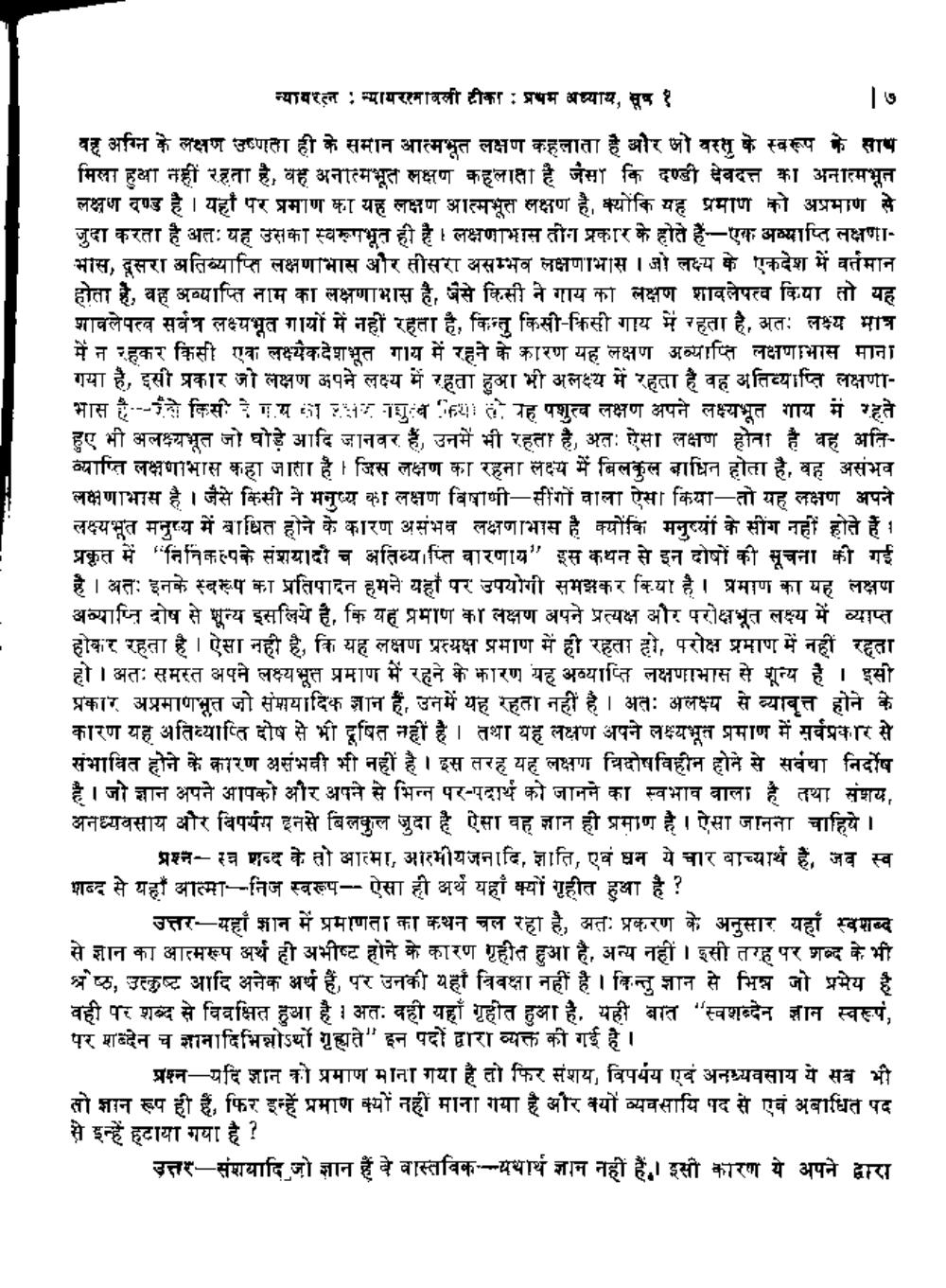________________
न्यावरत्न : न्यायररमावली टीका: प्रथम अध्याय, सष१
वह अग्नि के लक्षण उष्णता ही के समान आत्मभूत लक्षण कहलाता है और जो वस्तु के स्वरूप के साथ मिला हुआ नहीं रहता है, वह अनात्मभूत लक्षण कहलाता है जैसा कि दण्डी देवदत्त का अनात्मभूत लक्षण वण्ड है। यहाँ पर प्रमाण का यह लक्षण आत्मभूत लक्षण है, क्योंकि यह प्रमाण को अप्रमाण से जुदा करता है अतः यह उसका स्वरूपभूत ही है । लक्षणाभास तीन प्रकार के होते हैं-एक अध्याप्ति लक्षणाभास, दूसरा अतिव्याप्ति लक्षणाभास और तीसरा असम्भव लक्षणाभास । जो लक्ष्य के एकदेश में वर्तमान होता है, वह अव्याप्ति नाम का लक्षणाभास है, जैसे किसी ने गाय का लक्षण शावलेपत्त्व किया तो यह शावलेपत्व सर्वत्र लक्ष्यभूत गायों में नहीं रहता है, किन्तु किसी-किसी गाय में रहता है, अतः लक्ष्य मात्र में न रहकर किसी एका लक्ष्यैकदेशभूत गाय में रहने के कारण यह लक्षण अव्याप्ति लक्षणाभास माना गया है, इसी प्रकार जो लक्षण अपने लक्ष्य में रहता हुआ भी अलक्ष्य में रहता है वह अतिव्याप्ति लक्षणाभास है---दो किसी के मय काम शुः या ते. वह पशुत्व लक्षण अपने लक्ष्यभूत गाय में रहते हुए भी अलक्ष्यभूत जो घोड़े आदि जानवर हैं, उनमें भी रहता है, अतः ऐसा लक्षण होता है वह अतिव्याप्ति लक्षणाभास कहा जाता है । जिस लक्षण का रहना लक्ष्य में बिलकुल बाधिन होता है, वह असंभव लक्षणाभास है। जैसे किसी ने मनुष्य का लक्षण विषाणी-सींगों वाला ऐसा किया तो यह लक्षण अपने लक्ष्यभूत मनुष्य में बाधित होने के कारण असंभव लक्षणाभास है क्योंकि मनुष्यों के सींग नहीं होते हैं । प्रकृत में "नितिकल्पके संशयादी च अतिव्याप्ति वारणाय" इस कथन से इन दोषों की सूचना की गई है । अतः इनके स्वरूप का प्रतिपादन हमने यहाँ पर उपयोगी समझकर किया है। प्रमाण का यह लक्षण अव्याप्ति दोष से शून्य इसलिये है, कि यह प्रमाण का लक्षण अपने प्रत्यक्ष और परोक्षभूत लक्ष्य में व्याप्त होकर रहता है । ऐसा नहीं है, कि यह लक्षण प्रत्यक्ष प्रमाण में ही रहता हो, परोक्ष प्रमाण में नहीं रहता हो। अतः समस्त अपने लक्ष्यभूत प्रमाण में रहने के कारण यह अव्याप्ति लक्षणाभास से शून्य है । इस प्रकार अप्रमाणभूत जो समयादिक ज्ञान हैं, उनमें यह रहता नहीं है । अत: अलक्ष्य से ब्यावृत्त होने के कारण यह अतिव्याप्ति दोष से भी दूषित नहीं है। तथा यह लक्षण अपने लक्ष्यभूत प्रमाण में सर्वप्रकार से संभावित होने के कारण असंभवी भी नहीं है। इस तरह यह लक्षण विदोषविहीन होने से सर्वथा निर्दोष है । जो ज्ञान अपने आपको और अपने से भिन्न पर-पदार्थ को जानने का स्वभाव वाला है तथा संशय, अनध्यवसाय और विपर्यय इनसे बिलकुल जुदा है ऐसा वह ज्ञान ही प्रमाण है । ऐसा जानना चाहिये।
प्रश्न- स्त्र शब्द के तो आत्मा, आत्मीयजनादि, ज्ञाति, एवं धन ये चार वाच्यार्थ हैं, जब स्व शब्द से यहाँ आत्मा-निज स्वरूप-- ऐसा ही अर्थ यहाँ क्यों गृहीत हुआ है ?
उत्तर-यहाँ शान में प्रमाणता का कथन चल रहा है, अतः प्रकरण के अनुसार यहाँ स्वशब्द से ज्ञान का आत्मरूप अर्थ ही अभीष्ट होने के कारण गृहीत हुआ है, अन्य नहीं। इसी तरह पर शब्द के भी श्रेष्ठ, उत्कुष्ट आदि अनेक अर्थ हैं, पर उनकी यहाँ विवक्षा नहीं है। किन्तु ज्ञान से भिन्न जो प्रमेय है वही पर शब्द से विवक्षित हुआ है । अतः वही यहाँ गृहीत हुआ है, यही बात "स्वशब्देन ज्ञान स्वरूप, पर शब्देन च ज्ञानादिभिन्नोऽर्थो गृह्यते” इन पदों द्वारा व्यक्त की गई है।
प्रश्न–यदि ज्ञान को प्रमाण माना गया है तो फिर संशय, विपर्यय एवं अनध्यवसाय ये सब भी तो ज्ञान रूप ही हैं, फिर इन्हें प्रमाण क्यों नहीं माना गया है और क्यों व्यवसायि पद से एवं अबाधित पद से इन्हें हटाया गया है ?
उत्तर-संशयादि जो ज्ञान हैं वे वास्तविक यथार्थ ज्ञान नहीं हैं। इसी कारण ये अपने द्वारा