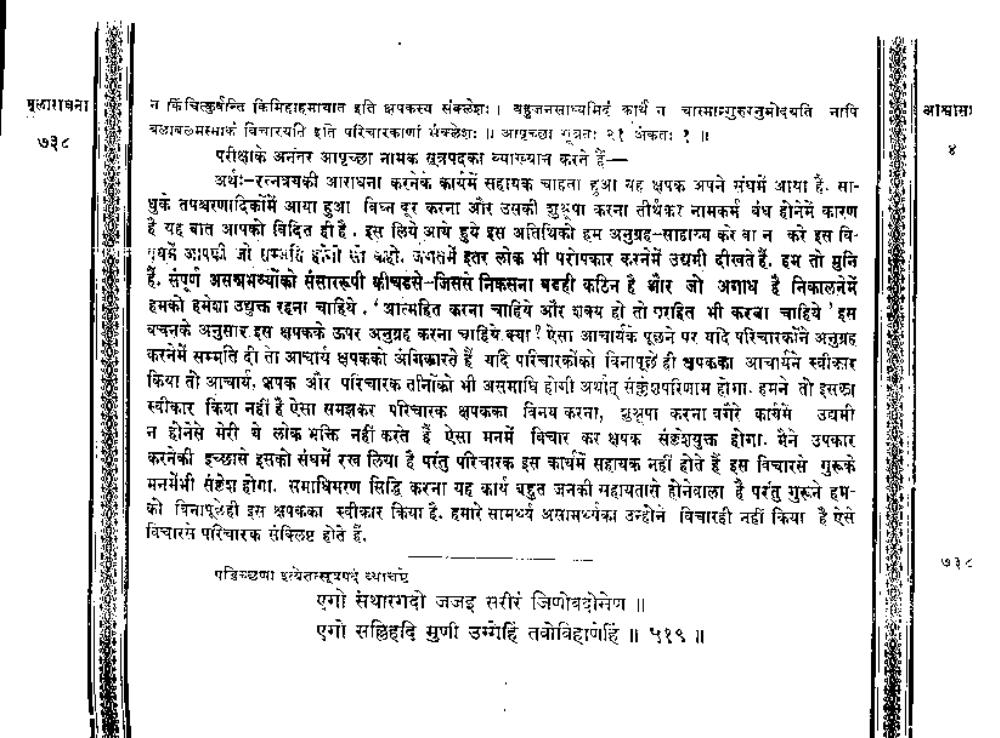________________
मूलाराधना
লাঘাষ
न किं चित्कुर्वन्ति किमिहाहमायात इति अपकस्य संक्लेशः । बहुजनसाध्यमिदं कार्य न चास्मा गुरुग्नुमोद यति नापि बलाबलमस्माकं विचारयति इति परिचारका संक्लेशः ।। आकछात२१ अंकतः १ ॥
परीक्षाके अनंतर आपृच्छा नामक सूत्रपदका व्याख्यान करने है
अर्थः-रत्नत्रयकी आराधना करनेक कायम सहायक चाहता हुआ यह क्षपक अपने संघमें आया है. साधुके तपश्चरणादिकोंमें आया हुआ विघ्न दूर करना और उसकी शुरुषा करना तीर्थकर नामकर्म बंध होने में कारण है यह बात आपको विदित ही है . इस लिये आये हुये इस अतिथिको हम अनुग्रह-साहाय्य करे वा न करे इस वि. गध पफी जो धम्मसिहानी सा कहो. जगतमें इतर लोक भी परोपकार करने में उद्यमी दीखते हैं. हम तो मुनि हैं. संपूर्ण असमभव्योंको संसाररूपी कीचडसे-जिससे निकसना परही कठिन है और जो अगाध है निकालने में हमको हमेशा उद्युक्त रहना चाहिये . 'आत्महित करना चाहिये और शक्य हो तो परहित भी करना चाहिये' इस बचनके अनुसार इस क्षपकके ऊपर अनुग्रह करना चाहिये क्या? ऐसा आचार्यक पूछने पर याद परिचारकाने अनुग्रह करने में सम्मति दी तो आचार्य क्षपकको अंगिकारते हैं यदि परिचारकोंको बिना पूछे ही धपकका आचार्यने स्वीकार किया तो आचार्य, भपक और परिचारक तनिॉको भी असमाधि होगी अर्थात् संकुशपरिणाम होगा. हमने तो इसका स्वीकार किया नहीं है ऐसा समझकर परिचारक क्षपकका विनय करना, शुश्रुपा करना वगैरे कार्य उद्यमी न होनेसे मेरी ये लोक भक्ति नहीं करते है ऐसा मनमें विचार कर क्षपक संशयुक्त होगा. मैने उपकार करनेकी इच्छासे इसको संघमें रख लिया है परंतु परिचारक इस कार्य में सहायक नहीं होते हैं इस विचारसे गुरूके मनमेंभी संवेश होगा. समाधिमरण सिद्धि करना यह कार्य बहुत जनकी सहायतासे होनेवाला है परंतु गुरुने हमको चिनापूले ही इस पकका स्वीकार किया है. हमारे सामर्थ्य असामथ्र्यका उन्होने विचारही नहीं किया है ऐसे विचारसे परिचारक संश्लिष्ट होते है.
पविटणा इत्येतासूरपदं ध्याचष्ट
एगो संथारगदो जजइ सरीरं जिणोबदोमेण ।। एगो सल्लिहदि मुणी उम्गेहिं तवोविहाणहिं ॥ ५१९ ।।