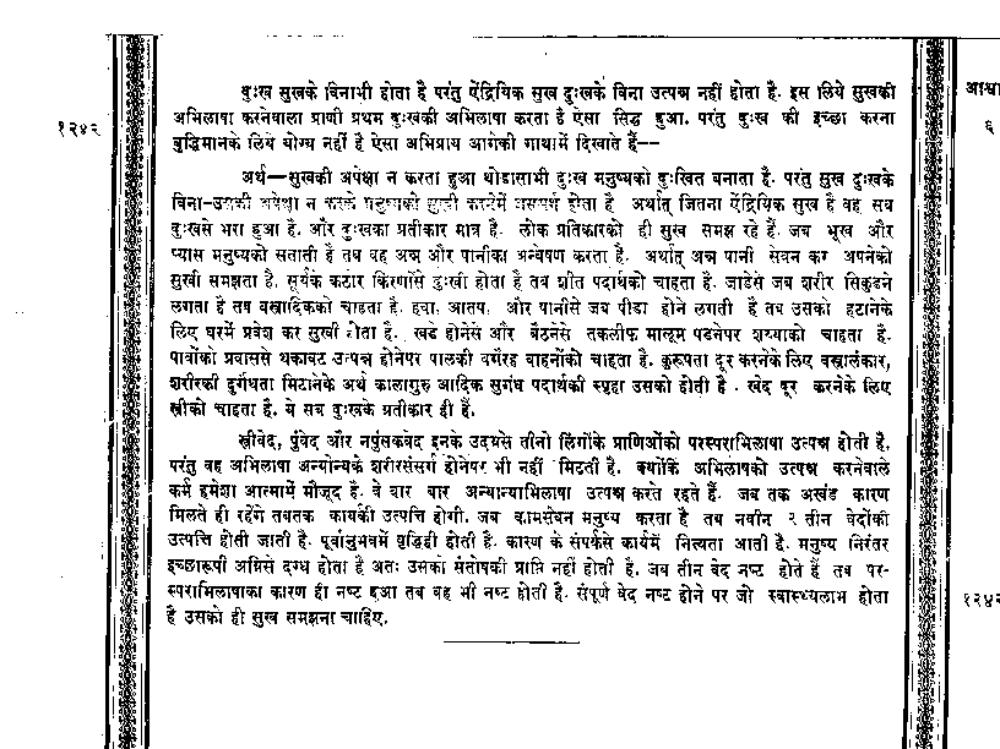________________
आधा
१२४२
दुःख सुखके बिनाभी होता है परंतु ऐंद्रियिक सुख दुःखके विना उत्पन्न नहीं होता है. इस लिये सुखकी अभिलाषा करनेवाला प्राणी प्रथम दुःखकी अभिलाषा करता है ऐसा सिद्ध हुआ. परंतु दुःख की इच्छा करना बुद्धिमानके लिये योग्य नहीं है ऐसा अभिप्राय आगेकी गाथा में दिखाते हैं--
अर्थ-सुखकी अपेक्षा न करता हुआ थोडासाभी दुःख मनुष्यको दुःखित बनाता है. परंतु सुख दुःखके विना-उसकी अपेक्षा न करले गरूको हाली कामें जसपर्ण होता है अर्थात् जितना ऐंद्रियिक सुख हैं वह सब दुःखसे भरा हुआ है. और दुःखका प्रतीकार मात्र है. लोक प्रतिकारको ही सुख समझ रहे हैं. जब भूख और
प्यास मनुष्यको सताती हैं तब वह अभ और पानीका अन्वेषण करता है. अर्थात् अन्न पानी सेवन कर अपनेको | सुखी समझता है, सूर्यक कटार किरणोंसे दुःखी होता है तब शीत पदार्थको चाहता है. जाडेसे जब शरीर सिकुहने
लगता है तष वस्त्रादिकको चाहता है. हचा, आतप, और यानीसे जब पीडा होने लगती है तब उसको हटाने के लिए घरमें प्रवेश कर सुखी होता है. खडे होनेस और बैठनेसे तकलीफ मालूम पडनेपर शय्याको चाहता है. पावोंको प्रवाससे थकावट उत्पन्न होनेएर पालकी वगैरह वाहनोंको चाहता है. कुरूपता दूर करने के लिए वस्त्रालंकार, शरीरकी दुर्गंधता मिटानेके अर्थ कालागुरु आदिक सुगंध पदार्थकी स्पृहा उसको होती है . खेद पूर करने के लिए स्त्रीको चाहता है. ये सब दुःखके प्रतीकार ही हैं.
स्त्रीवेद, पुंयेद और नपुंसकवेद इनके उदयसे तीनो लिंगोंके प्राणिओंको परस्परामिलाषा उत्पन्न होती है, परंतु वह अभिलाषा अन्योन्यके शरीरसंसर्ग होनेपर भी नहीं मिटती है. क्योंकि अभिलाषको उत्पष करनेवाले कर्म हमेशा आत्मामें मौजूद है. वे चार बार अन्यान्याभिलाषा उत्पथ करते रहते हैं. जब तक अखंड कारण मिलते ही रहेंगे तबतक कार्यकी उत्पत्ति होगी. जब बामसेवन मनुष्य करता है तय नवीन २ तीन चेदोंकी उत्पत्ति होसी जाती है. पूर्वानुमवमें वृद्धिही होती है. कारण के संपर्कसे कार्य में नित्यता आती है. मनुष्य निरंतर इच्छारूपी अनिसे दग्ध होता है अतः उसका संतोषकी प्राप्ति नहीं होती है. जब तीन वेद नष्ट होते हैं तब परपराभिलाषाका कारण ही नष्ट आ तब वह भी नष्ट होती है. संपूर्ण घेद नष्ट होने पर जो स्वास्थ्यलाभ होता है उसको ही सुख समझना चाहिए,
१२४३