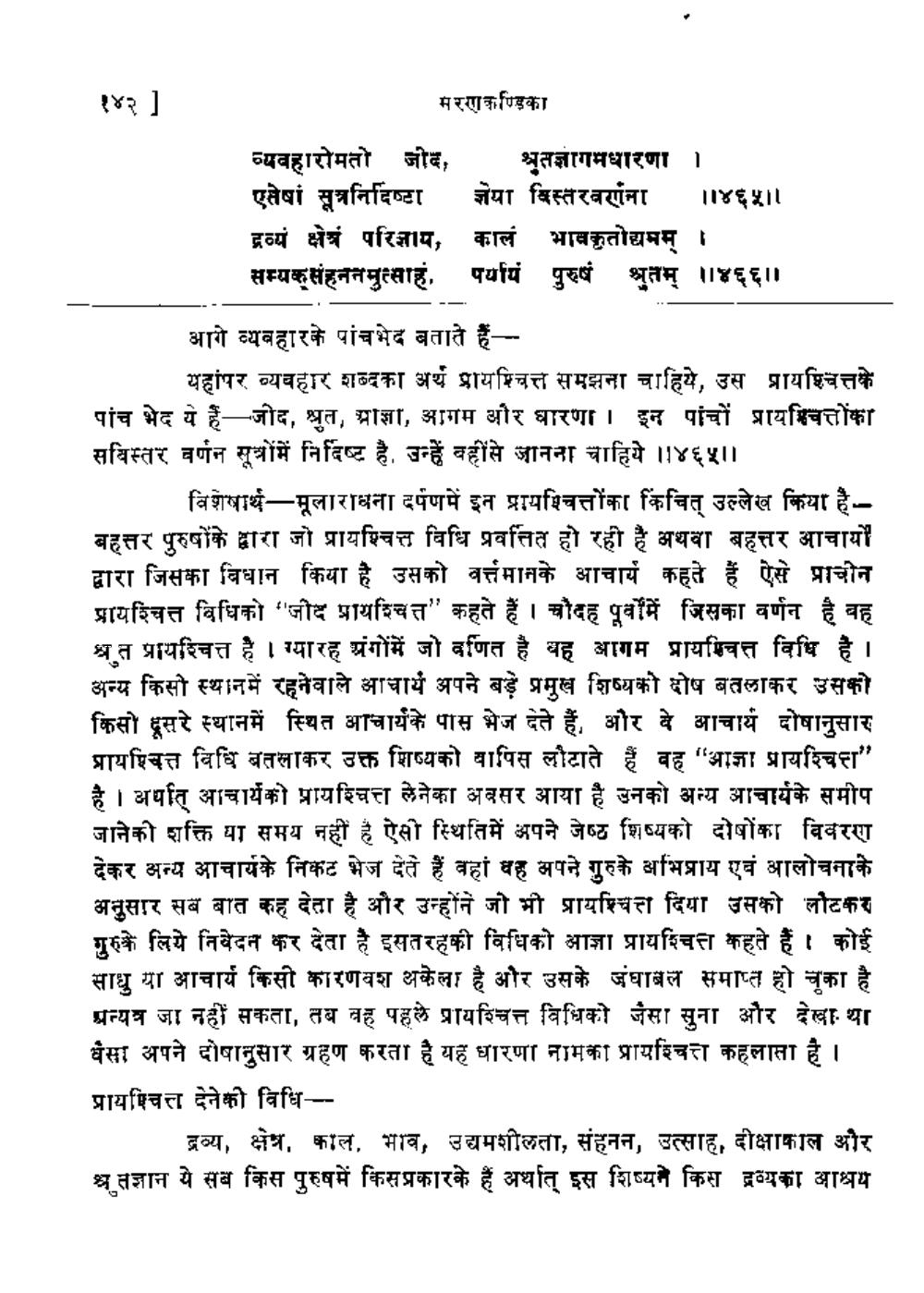________________
१४२ ]
मरणण्डिका
व्यवहारोमतो जीद, एतेषां सूत्रनिर्दिष्टा द्रव्यं क्षेत्रं परिज्ञाय,
सम्यक् संहननमुत्साहं,
श्रुतज्ञागमधारणा । ज्ञेया विस्तरवरांना
भाषकृतोद्यमम् ।
पुरुषं श्रुतम् ॥४६६ ॥
कालं
पर्यायं
।।४६५।।
आगे व्यवहारके पांचभेद बताते हैं
यहां पर व्यवहार शब्दका अर्थ प्रायश्चित्त समझना चाहिये, उस प्रायश्चित्तके पांच भेद ये हैं-जीद, श्रुत, प्राज्ञा, आगम और धारणा । इन पांचों प्रायश्चित्तोंका सविस्तर वर्णन सूत्रों में निर्दिष्ट है, उन्हें वहीं से जानना चाहिये ||४६५।।
विशेषार्थ — मूलाराधना दर्पण में इन प्रायश्चित्तोंका किंचित् उल्लेख किया हैबहतर पुरुषोंके द्वारा जो प्रायश्चित्त विधि प्रवर्तित हो रही है अथवा बहत्तर आचार्यों द्वारा जिसका विधान किया है उसको वर्त्तमानके आचार्य कहते हैं ऐसे प्राचीन प्रायश्चित्तविधिको "जीद प्रायश्चित्त" कहते हैं। चौदह पूर्वोमें जिसका वर्णन है वह श्रुत प्रायश्चित्त है । ग्यारह अंगोंमें जो वर्णित है वह आगम प्रायश्चित विधि है । अन्य किसी स्थान में रहनेवाले आचार्य अपने बड़े प्रमुख शिष्यको दोष बतलाकर उसको किसी दूसरे स्थान में स्थित आचार्यके पास भेज देते हैं, और वे आचार्य दोषानुसार प्रायश्चित्तविधि बतलाकर उक्त शिष्यको वापिस लौटाते हैं वह "आज्ञा प्रायश्चित्त" है । अर्थात् आचार्यको प्रायश्चित्त लेनेका अवसर आया है उनको अन्य आचार्य के समीप जानेकी शक्ति या समय नहीं है ऐसी स्थिति में अपने जेष्ठ शिष्यको दोषोंका विवरण देकर अन्य आचार्य के निकट भेज देते हैं वहां वह अपने गुरुकै अभिप्राय एवं आलोचना के अनुसार सब बात कह देता है और उन्होंने जो भी प्रायश्चित्त दिया उसको लोटकर गुरुके लिये निवेदन कर देता है इसतरह की विधिको आज्ञा प्रायश्चित्त कहते हैं । कोई साधु या आचार्य किसी कारणवश अकेला है और उसके जंघाबल समाप्त हो चुका है अन्यत्र जा नहीं सकता, तब वह पहले प्रायश्चित्त विधिको जैसा सुना और देखा था वैसा अपने दोषानुसार ग्रहण करता है यह धारणा नामका प्रायश्चित्त कहलाता है । प्रायश्चित्त देने की विधि --
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, उद्यमशीलता, संहनन, उत्साह, दीक्षाकाल और श्रुतज्ञान ये सब किस पुरुषमें किसप्रकारके हैं अर्थात् इस शिष्यमे किस द्रव्यका आश्रय