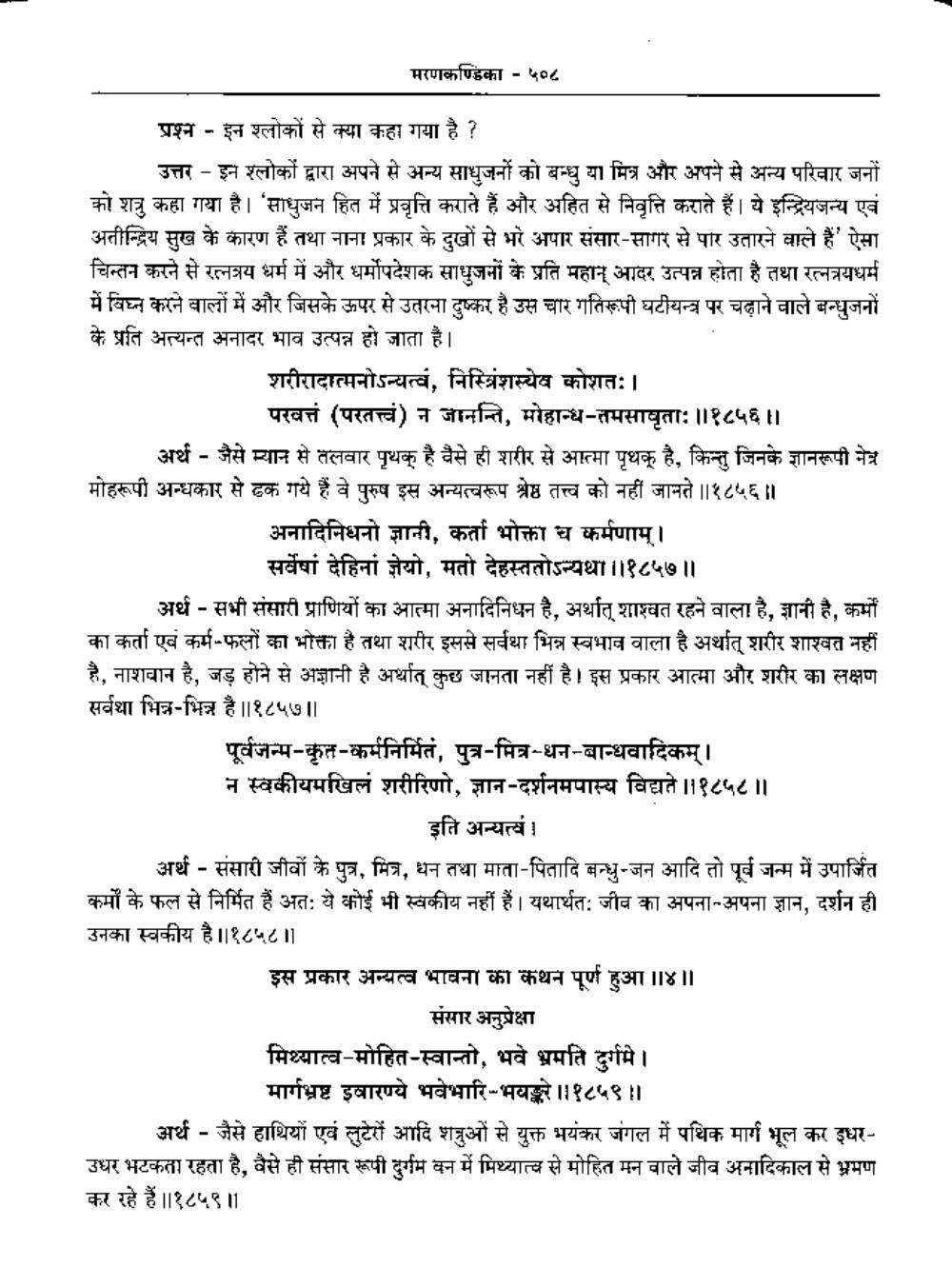________________
मरणकण्डिका -५०८
प्रश्न - इन श्लोकों से क्या कहा गया है ?
उत्तर - इन श्लोकों द्वारा अपने से अन्य साधुजनों को बन्धु या मित्र और अपने से अन्य परिवार जनों को शत्रु कहा गया है। ‘साधुजन हित में प्रवृत्ति कराते हैं और अहित से निवृत्ति कराते हैं। ये इन्द्रियजन्य एवं अतीन्द्रिय सुख के कारण हैं तथा नाना प्रकार के दुखों से भरे अपार संसार-सागर से पार उतारने वाले हैं ऐसा चिन्तन करने से रत्नत्रय धर्म में और धर्मोपदेशक साधुजनों के प्रति महान् आदर उत्पन्न होता है तथा रत्नत्रयधर्म में विघ्न करने वालों में और जिसके ऊपर से उतरना दुष्कर है उस चार गतिरूपी घटीयन्त्र पर चढ़ाने वाले बन्धुजनों के प्रति अत्यन्त अनादर भाव उत्पन्न हो जाता है।
शरीरादात्मनोऽन्यत्वं, निस्त्रिंशस्येव कोशतः ।
परवत्तं (परतत्त्वं) न जानन्ति, मोहान्ध-तमसावृताः॥१८५६।। अर्थ - जैसे म्यान से तलवार पृथक् है वैसे ही शरीर से आत्मा पृथक् है, किन्तु जिनके ज्ञानरूपी नेत्र मोहरूपी अन्धकार से ढक गये हैं वे पुरुष इस अन्यत्वरूप श्रेष्ठ तत्त्व को नहीं जानते ॥१८५६॥
अनादिनिधनो ज्ञानी, कर्ता भोक्ता च कर्मणाम्।
सर्वेषां देहिनां ज्ञेयो, मतो देहस्ततोऽन्यथा ।।१८५७॥ अर्थ - सभी संसारी प्राणियों का आत्मा अनादिनिधन है, अर्थात् शाश्वत रहने वाला है, ज्ञानी है, कर्मों का कर्ता एवं कर्म-फलों का भोक्ता है तथा शरीर इससे सर्वथा भिन्न स्वभाव वाला है अर्थात् शरीर शाश्वत नहीं है, नाशवान है, जड़ होने से अज्ञानी है अर्थात् कुछ जानता नहीं है। इस प्रकार आत्मा और शरीर का लक्षण सर्वथा भिन्न-भिन्न है ।।१८५७ ।।
पूर्वजन्म-कृत-कर्मनिर्मितं, पुत्र-मित्र-धन-बान्धवादिकम् । न स्वकीयमखिलं शरीरिणो, ज्ञान-दर्शनमपास्य विद्यते ।।१८५८ ॥
इति अन्यत्व। अर्थ - संसारी जीवों के पुत्र, मित्र, धन तथा माता-पितादि बन्धु-जन आदि तो पूर्व जन्म में उपार्जित कर्मों के फल से निर्मित हैं अतः ये कोई भी स्वकीय नहीं हैं। यथार्थत: जीव का अपना-अपना ज्ञान, दर्शन ही उनका स्वकीय है।।१८५८ ॥ इस प्रकार अन्यत्व भावना का कथन पूर्ण हुआ ॥४॥
संसार अनुप्रेक्षा मिथ्यात्व-मोहित-स्वान्तो, भवे भ्रमति दुर्गमे ।
मार्गभ्रष्ट इवारण्ये भवेभारि-भयङ्करे ।। १८५९ ।। अर्थ - जैसे हाथियों एवं लुटेरों आदि शत्रुओं से युक्त भयंकर जंगल में पथिक मार्ग भूल कर इधरउधर भटकता रहता है, वैसे ही संसार रूपी दुर्गम वन में मिथ्यात्व से मोहित मन वाले जीव अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं ।।१८५९॥