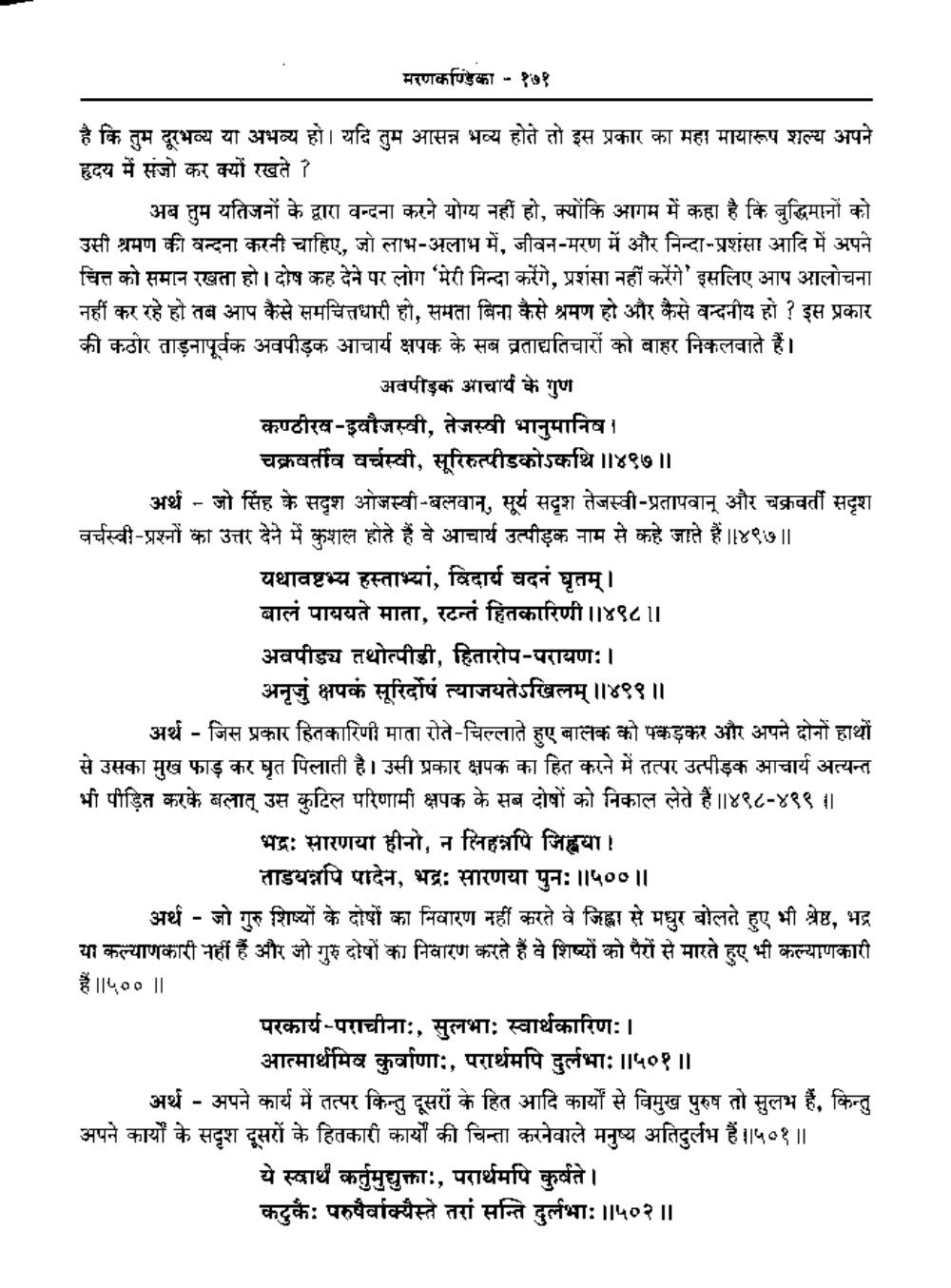________________
मरणकण्डिका - १७१
है कि तुम दूरभव्य या अभव्य हो। यदि तुम आसन्न भव्य होते तो इस प्रकार का महा मायारूप शल्य अपने हृदय में संजो कर क्यों रखते ?
अब तुम यतिजनों के द्वारा वन्दना करने योग्य नहीं हो, क्योंकि आगम में कहा है कि बुद्धिमानों को उसी श्रमण की वन्दना करनी चाहिए, जो लाभ-अलाभ में, जीवन-मरण में और निन्दा-प्रशंसा आदि में अपने चित्त को समान रखता हो। दोष कह देने पर लोग 'मेरी निन्दा करेंगे, प्रशंसा नहीं करेंगे' इसलिए आप आलोचना नहीं कर रहे हो तब आप कैसे समचित्तधारी हो, समता बिना कैसे श्रमण हो और कैसे वन्दनीय हो ? इस प्रकार की कठोर ताड़नापूर्वक अवपीड़क आचार्य क्षपक के सब व्रताद्यतिचारों को बाहर निकलवाते हैं।
अवपीड़क आचार्य के गुण कण्ठीरव-इवौजस्वी, तेजस्वी भानुमानिष ।
चक्रवर्तीव वर्चस्वी, सूरिरुत्पीडकोऽकथि ॥४९७ ॥ अर्थ - जो सिंह के सदृश ओजस्वी-बलवान, सूर्य सदृश तेजस्वी-प्रतापवान् और चक्रवर्ती सदृश वर्चस्वी-प्रश्नों का उत्तर देने में कुशल होते हैं वे आचार्य उत्पीड़क नाम से कहे जाते हैं ।।४९७ ।।
यथावष्टभ्य हस्ताभ्यां, विदार्य वदनं घृतम् । बालं पाययते माता, रटन्तं हितकारिणी ।।४९८ ।। अवपीड्य तथोत्पीड़ी, हितारोप-परायणः ।
अनृणु क्षपकं सूरिर्दोषं त्याजयतेऽखिलम् ॥४९९ ॥ अर्थ - जिस प्रकार हितकारिणी माता रोते-चिल्लाते हुए बालक को पकड़कर और अपने दोनों हाथों से उसका मुख फाड़ कर घृत पिलाती है। उसी प्रकार क्षपक का हित करने में तत्पर उत्पीड़क आचार्य अत्यन्त भी पीड़ित करके बलात् उस कुटिल परिणामी क्षपक के सब दोषों को निकाल लेते हैं।४९८-४९९ ।।
भद्रः सारणया हीनो, न लिहन्नपि जिह्वया।
ताडयन्नपि पादेन, भद्रः सारणया पुनः॥५००। अर्थ - जो गुरु शिष्यों के दोषों का निवारण नहीं करते वे जिह्वा से मधुर बोलते हुए भी श्रेष्ठ, भद्र या कल्याणकारी नहीं हैं और जो गुरु दोषों का निवारण करते हैं वे शिष्यों को पैरों से मारते हुए भी कल्याणकारी हैं ।।५०० ।।
परकार्य-पराचीनाः, सुलभाः स्वार्थकारिणः ।
आत्मार्थमिव कुर्वाणा:, परार्थमपि दुर्लभाः ।।५०१॥ अर्थ - अपने कार्य में तत्पर किन्तु दूसरों के हित आदि कार्यों से विमुख पुरुष तो सुलभ हैं, किन्तु अपने कार्यों के सदृश दूसरों के हितकारी कार्यों की चिन्ता करनेवाले मनुष्य अतिदुर्लभ हैं ।।५०१ ।।
ये स्वार्थ कर्तुमुद्युक्ताः, परार्थमपि कुर्वते । कटुकैः परुषैर्वाक्यैस्ते तरां सन्ति दुर्लभाः॥५०२ ।।