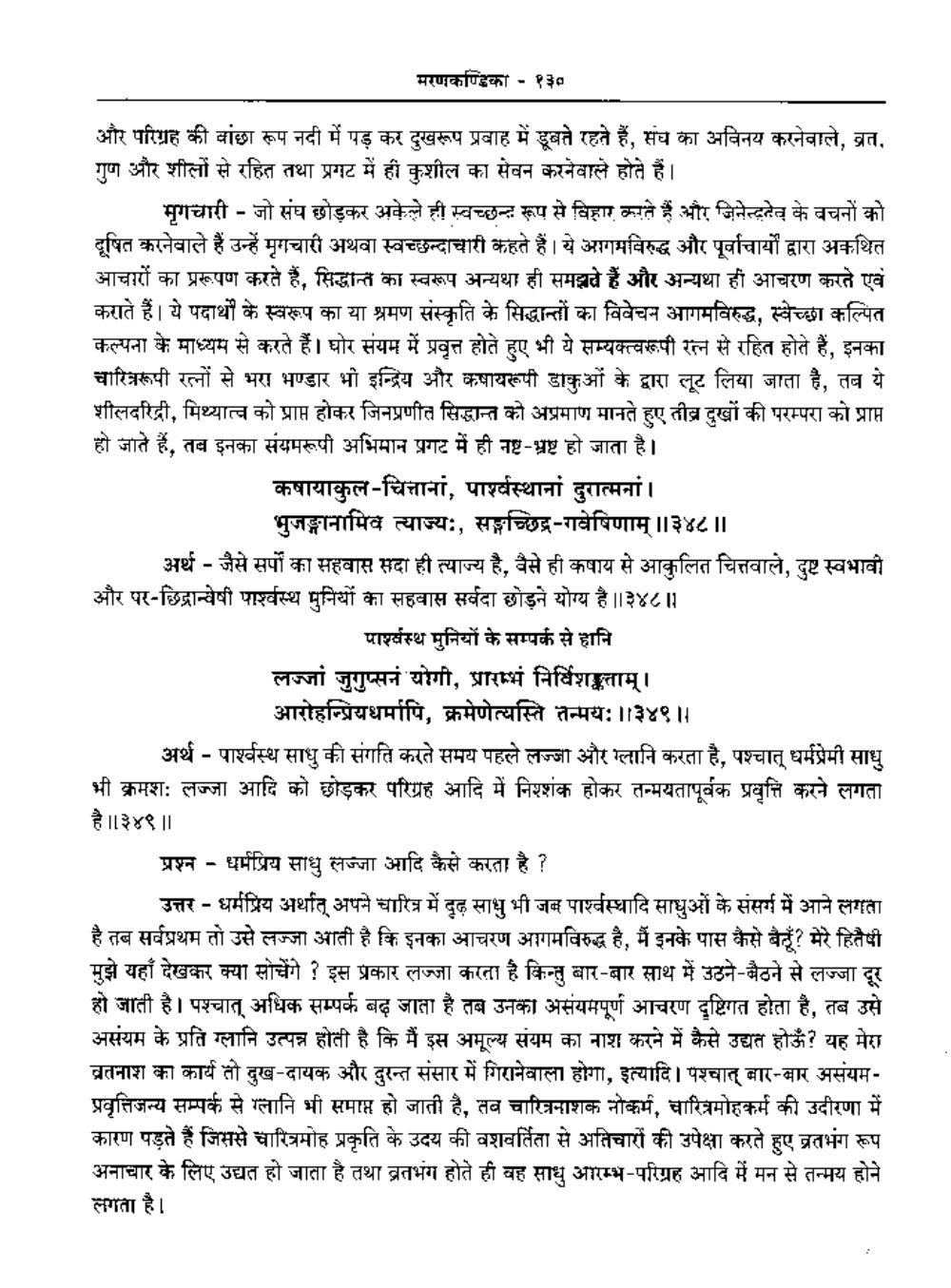________________
मरणकण्डिका - १३०
और परिग्रह की वांछा रूप नदी में पड़ कर दुखरूप प्रवाह में डूबते रहते हैं, संच का अविनय करनेवाले, व्रत, गुण और शीलों से रहित तथा प्रगट में ही कुशील का सेवन करनेवाले होते हैं।
मृगचारी - जो संघ छोड़कर अकेले ही स्वच्छन्द्र रूप से विहार करते हैं और जिनेन्द्रदेव के वचनों को दूषित करनेवाले हैं उन्हें मृगचारी अथवा स्वच्छन्दाचारी कहते हैं। ये आगमविरुद्ध और पूर्वाचार्यों द्वारा अकथित आचारों का प्ररूपण करते हैं, सिद्धान्त का स्वरूप अन्यथा ही समझते हैं और अन्यथा ही आचरण करते एवं कराते हैं। ये पदार्थों के स्वरूप का या श्रमण संस्कृति के सिद्धान्तों का विवेचन आगमविरुद्ध, स्वेच्छा कल्पित कल्पना के माध्यम से करते हैं। घोर संयम में प्रवृत्त होते हुए भी ये सम्यक्त्वरूपी रत्न से रहित होते हैं, इनका चारित्ररूपी रत्नों से भरा भण्डार भी इन्द्रिय और कषायरूपी डाकुओं के द्वारा लूट लिया जाता है, तब ये शीलदरिद्री, मिथ्यात्व को प्राप्त होकर जिनप्रणीत सिद्धान्त को अप्रमाण मानते हुए तीव्र दुखों की परम्परा को प्राप्त हो जाते हैं, तब इनका संयमरूपी अभिमान प्रगट में ही नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है।
कषायाकुल-चित्तानां, पार्श्वस्थानां दुरात्मनां ।
भुजङ्गानामिव त्याज्य:, सङ्गच्छिद्र-गवेषिणाम् ।।३४८ ॥ अर्थ - जैसे सपों का सहवास सदा ही त्याज्य है, वैसे ही कषाय से आकुलित चित्तवाले, दुष्ट स्वभावी और पर-छिद्रान्वेषी पार्श्वस्थ मुनियों का सहवास सर्वदा छोड़ने योग्य है ।।३४८ ।।
पार्श्वस्थ मुनियों के सम्पर्क से हानि लज्जां जुगुप्सनं योगी, प्राराभं निर्विशङ्कताम्।
आरोहन्प्रियधर्मापि, क्रमेणेत्यस्ति तन्मयः ।।३४९।। अर्थ - पार्श्वस्थ साधु की संगति करते समय पहले लज्जा और ग्लानि करता है, पश्चात् धर्मप्रेमी साधु भी क्रमश: लज्जा आदि को छोड़कर परिग्रह आदि में निश्शंक होकर तन्मयतापूर्वक प्रवृत्ति करने लगता है॥३४९॥
प्रश्न - धर्मप्रिय साधु लज्जा आदि कैसे करता है ?
उत्तर - धर्मप्रिय अर्थात् अपने चारित्र में दृढ़ साधु भी जब पार्श्वस्थादि साधुओं के संसर्ग में आने लगता है तब सर्वप्रथम तो उसे लज्जा आती है कि इनका आचरण आगमविरुद्ध है, मैं इनके पास कैसे बै? मेरे हितैषी मुझे यहाँ देखकर क्या सोचेंगे ? इस प्रकार लज्जा करता है किन्तु बार-बार साथ में उठने-बैठने से लज्जा दूर हो जाती है। पश्चात् अधिक सम्पर्क बढ़ जाता है तब उनका असंयमपूर्ण आचरण दृष्टिगत होता है, तब उसे असंयम के प्रति ग्लानि उत्पन्न होती है कि मैं इस अमूल्य संयम का नाश करने में कैसे उद्यत होऊँ? यह मेरा व्रतनाश का कार्य तो दुख-दायक और दुरन्त संसार में गिरानेवाला होगा, इत्यादि। पश्चात् बार-बार असंयमप्रवृत्तिजन्य सम्पर्क से ग्लानि भी समाप्त हो जाती है, तब चारित्रनाशक नोकर्म, चारित्रमोहकर्म की उदीरणा में कारण पड़ते हैं जिससे चारित्रमोह प्रकृति के उदय की वशवर्तिता से अतिचारों की उपेक्षा करते हुए व्रतभंग रूप अनाचार के लिए उद्यत हो जाता है तथा व्रतभंग होते ही वह साधु आरम्भ-परिग्रह आदि में मन से तन्मय होने लगता है।