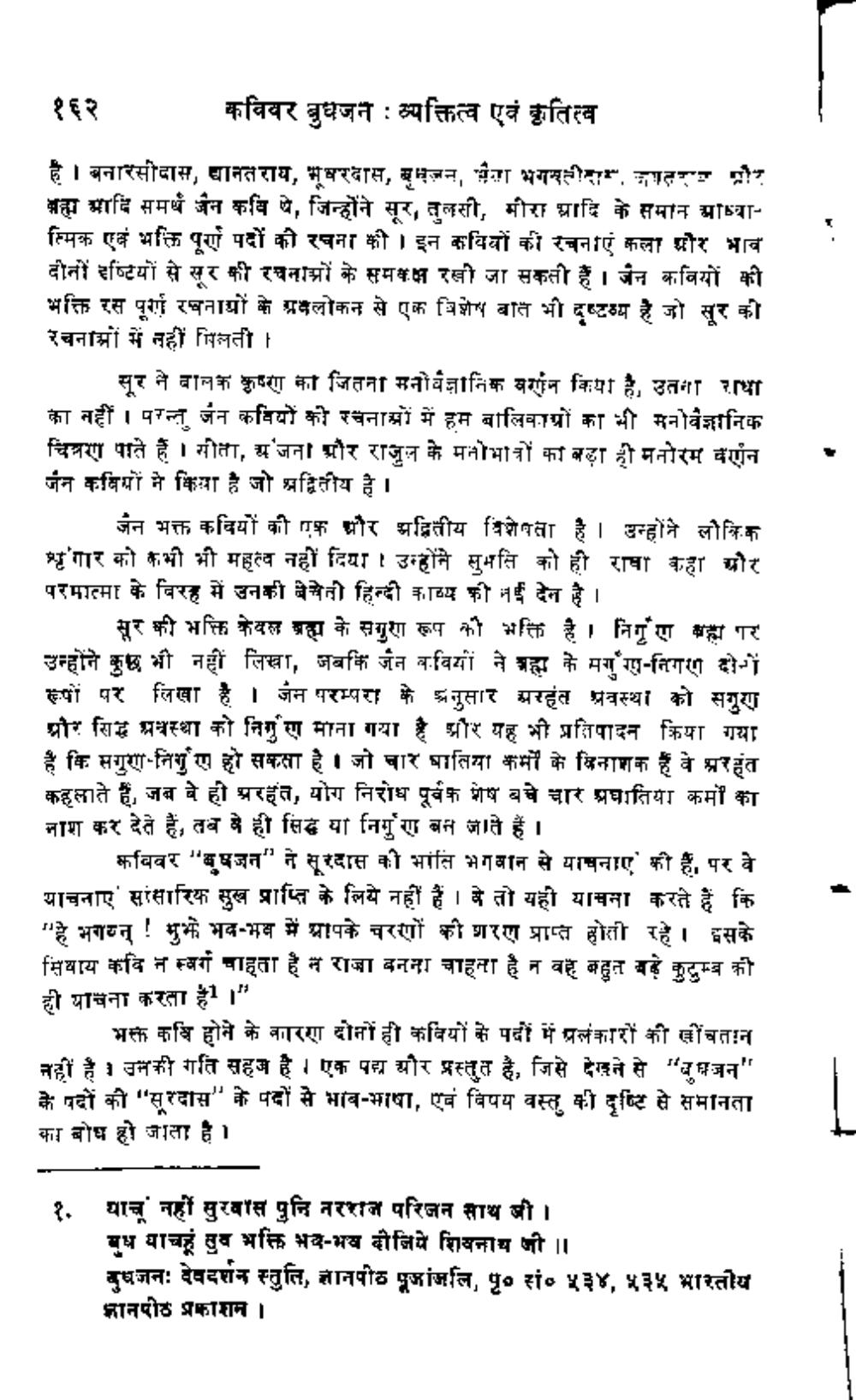________________
१६२
कविवर बुधजन : व्यक्तित्व एवं कृतित्व
है । बनारसीदास, चानत राय, भघरदास, बमज़न, ता भगमतीदार.मातरः प्रोट ब्रह्म मादि समर्थ जैन कवि थे, जिन्होंने सूर, तुलसी, मीरा प्रादि के समान आध्यास्मिक एवं भक्ति पूर्ण पदों की रचना की। इन कवियों की रचनाएं कला और भाव दोनों दृष्टियों से सूर की रचनाओं के समक्ष रखी जा सकती हैं । जैन कवियों की भक्ति रस पूर्ण रचनायों के अवलोकन से एक विशेष बात भी दृष्टव्य है जो सूर की रचनाओं में नहीं मिलती।
___ सूर ने बालक कृष्ण का जितना मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है, उतना राधा का नहीं । परन्तु जन कवियों को रचनामों में हम बालिवानों का भी मनोवैज्ञानिक चित्रण पाते हैं । सीता, अजना प्रौर राजुल के मनोभात्रों का बड़ा ही मनोरम वर्णन जन कवियों ने किया है जो अद्वितीय है।
जन भक्त कवियों की एक और अद्वितीय विशेषता है। उन्होंने लौकिक श्रृंगार को कभी भी महत्व नहीं दिया। उन्होंने सुभति को ही राषा कहा और परमात्मा के विरह में उनकी बैचेती हिन्दी काव्य की नई देन है।
सूर की भक्ति केवल ब्रह्म के सगुण रूप की भक्ति है। निर्गुण ब्रह्म पर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, जबकि जन ववियों ने ब्रह्म के मा-निगण दोगें रूपों पर लिखा है । जन परम्परा के अनुसार अरहंत प्रवस्था को सगुण और सिद्ध अवस्था को निर्गुण माना गया है और यह भी प्रतिपादन किया गया है कि सगुण-निर्गुण हो सकता है । जो चार घालिया कर्मों के किनाशक हैं वे परहंत कहलाते हैं, जब बे ही प्ररहंत, योग निरोध पूर्वक शेष बचे चार प्रघातिया कर्मों का नाश कर देते हैं, तब केही सिद्ध या निर्गुण बन जाते हैं।
कविवर "बुधजन" ने सूरदास की भांति भगवान से याचनाए' की हैं, पर वे याचनाए' सांसारिक सुख प्राप्ति के लिये नहीं हैं । ये तो यही याचना करते हैं कि
हे भगन् ! मुझे भव-भव में प्रापके चरणों की शरण प्राप्त होती रहे। इसके सिवाय कवि न स्वर्ग चाहता है न राजा बनना चाहता है न वह बहुत बड़े कुटुम्ब की ही याचना करता है।"
भक्त कवि होने के कारण दोनों ही कवियों के पदों में प्रलंकारों की खींचतान नहीं है। उनकी गति सहन है । एक पद्म और प्रस्तुत है, जिसे देखने से "प्रजन" के पदों को "सूरदास' के पदों से भाव-भाषा, एवं विषय वस्तु की दृष्टि से समानता का बोध हो जाता है।
१. याचं नहीं सुरवास पुनि नरराज परिजन साथ जी।
सुध याचहूं सुव भक्ति भव-भव दौजिये शिवनाथ जी ।। बुधजनः देवदर्शन स्तुलि, ज्ञानपीठ पूजामलि, पृ० सं० ५३४, ५३५ भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन ।