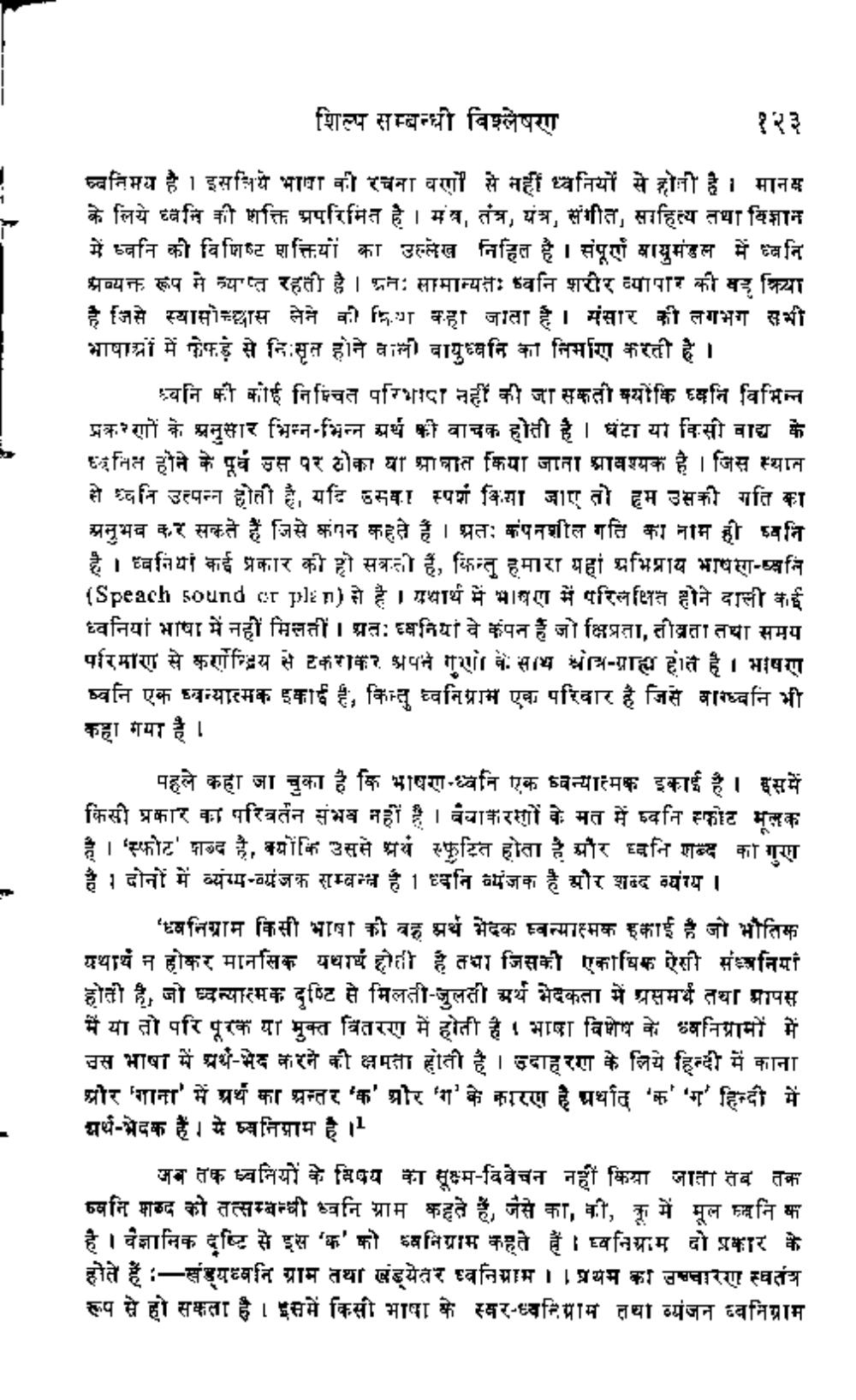________________
शिल्प सम्बन्धी विश्लेषण
ध्वनिमय है । इसलिये भाषा की रचना वर्णों से नहीं ध्वनियों से होती है। मानस के लिये ध्वनि की शक्ति अपरिमित है । मंत्र, तंत्र, यंत्र, संगीत, साहित्य तथा विज्ञान में ध्वनि की विशिष्ट शक्तियों का उल्लेख निहिल है । संपूर्ण वायुमंडल में ध्वनि अव्यक्त रूप में व्याप्त रहती है । प्रन: सामान्यतः ध्वनि शरीर व्यापार की यह क्रिया है जिसे स्थासोन्यास लेने व रिग कहा जाता है । मंसार की लगभग सभी भाषाओं में केफड़े से निःसृत होने वाली वायुध्वनि का निर्माण करती है।
ध्वनि की कोई निचित परिभाषा नहीं की जा सकती क्योंकि ध्वनि विभिन्न प्रकरणों के अनुसार भिन्न-भिन्न अर्थ की वाचक होती है | घंटा या किसी वाद्य के
मित होने के पूर्व उस पर टोका या पानात किया जाना आवश्यक है । जिस स्थान से ध्वनि उत्पन्न होती है, यदि उसका स्पर्श किया जाए तो हम उसकी गति का अनुभव कर सकते हैं जिसे कंपन कहते हैं । अतः कंपनशील गति का नाम ही इवनि है । ध्वनियां कई प्रकार की हो सकती हैं, किन्तु हमारा यहां अभिप्राय भाषरग-ध्वनि (Speach sound er pl. T) से है । यथार्थ में भाषण में परिलक्षित होने दाली कई ध्वनियां भाषा में नहीं मिलती । प्रत: ध्वनियां वे कंपन है जो क्षिप्रता, तीव्रता तथा समय परिमाण से कर्णन्द्रिय से टकराकर अपने गुणों के साथ भाग-ग्राह्य होते है । भाषण ध्वनि एक ध्वन्यात्मक इकाई है, किन्तु ध्वनिग्राम एवा परिवार है जिसे बारध्वनि भी कहा गया है।
पहले कहा जा चुका है कि भाषण ध्वनि एक ध्वन्यात्मक इकाई है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है । बचाकरसों के मत में इवनि सकोट मलक है । 'स्फोट' पाब्द है, क्योंकि उससे अयं स्फुरित होता है और ध्वनि शब्द का गुण है । दोनों में व्यंग्य-व्यंजक सम्बन्ध है 1 ध्वनि व्यंजक है और शब्द व्यंग्य ।।
ध्वनिग्राम किसी भाषा की वह अर्थ भेदक ध्वन्यात्मक इकाई है जो भौतिक यथार्थ न होकर मानसिक यथार्थ होती है तथा जिसकी एकाधिक ऐसी संध्वनियां होती है, जो ध्वन्यात्मक दृष्टि से मिलती-जुलती अर्थ भेदकता में असमर्थ तथा मापस में या तो परि पूरक या मुक्त वितरण में होती है । भाषा विशेष के ध्वनिग्रामों में उस भाषा में अर्थ-भेद करने की क्षमता होती है । उदाहरण के लिये हिन्दी में काना और 'गाना' में अर्थ का अन्तर 'क' और 'ग' के कारण है अर्थात 'क' 'ग' हिन्दी में अर्थ-भेदक हैं । मे व्यनिग्राम है।
अब तक ध्वनियों के विषय का सूक्ष्म-विवेचन नहीं किया जाता तब तक ध्वनि याब्द को तत्सम्बन्धी ध्वनि ग्राम कहते हैं, जैसे का, की, कु में मूल मनि का है । वैज्ञानिक दृष्टि से इस 'क' को ध्वनिग्राम कहते हैं। ध्वनियाम दो प्रकार के होते हैं:-खंड्यध्वनि ग्राम तथा खंड्येतर ध्वनिग्राम । । प्रथम का उपचारण स्वतंत्र रूप से हो सकता है। इसमें किसी भाषा के स्वर-ध्वनिग्राम तथा व्यंजन स्वनिग्राम