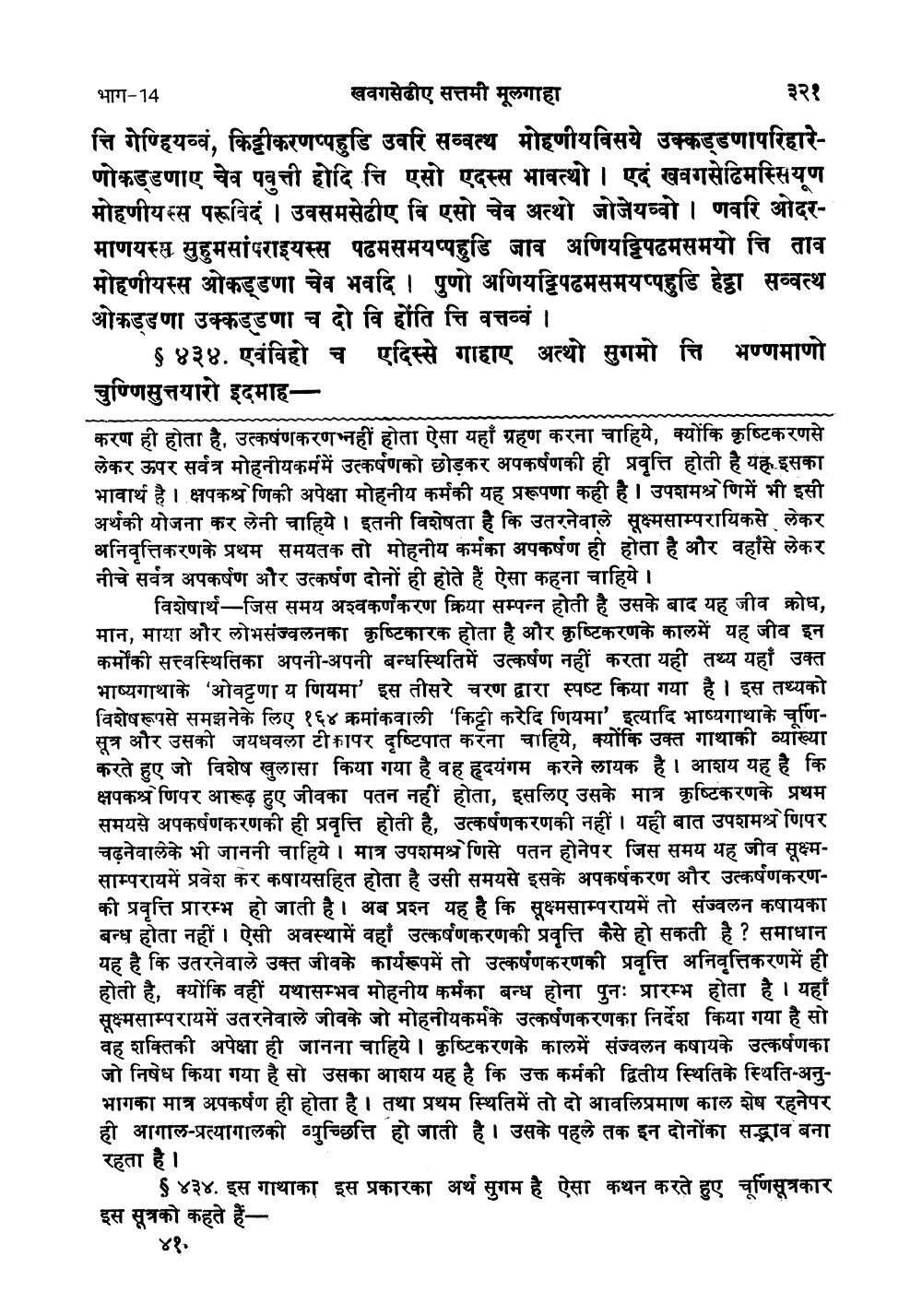________________
भाग-14 खवगसेढीए सत्तमी मूलगाहा
३२१ त्ति गेण्हियव्वं, किट्टीकरणप्पहुडि उवरि सव्वत्थ मोहणीयविसये उक्कड्डणापरिहारेणोकड्डणाए चेव पवुत्ती होदि त्ति एसो एदस्स भावत्थो । एदं खवगसेढिमस्सियूण मोहणीयस्स परूविदं । उवसमसेढीए वि एसो चेव अत्थो जोजेयव्यो । णवरि ओदरमाणयस्त सुहुमसांपराइयस्स पढमसमयप्पहुडि जाव अणियट्टिपढमसमयो त्ति ताव मोहणीयस्स ओकड्डणा चेव भवदि । पुणो अणियट्टिपढमसमयप्पहुडि हेट्ठा सव्वत्थ ओकड्डणा उक्कड्डणा च दो वि होंति त्ति वत्तव्वं ।।
४३४. एवंविहो च एदिस्से गाहाए अत्थो सुगमो ति भण्णमाणो चुण्णिसुत्तयारो इदमाहकरण ही होता है, उत्कर्षणकरण नहीं होता ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि कृष्टिकरणसे लेकर ऊपर सर्वत्र मोहनीयकर्ममें उत्कर्षणको छोड़कर अपकर्षणकी ही प्रवृत्ति होती है यह इसका भावार्थ है। क्षपकणिकी अपेक्षा मोहनीय कर्मकी यह प्ररूपणा कही है । उपशमणिमें भी इसी अर्थकी योजना कर लेनी चाहिये। इतनी विशेषता है कि उतरनेवाले सूक्ष्मसाम्परायिकसे लेकर अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयतक तो मोहनीय कर्मका अपकर्षण ही होता है और वहाँसे लेकर नीचे सर्वत्र अपकर्षण और उत्कर्षण दोनों ही होते हैं ऐसा कहना चाहिये।
विशेषार्थ-जिस समय अश्वकर्णकरण क्रिया सम्पन्न होती है उसके बाद यह जीव क्रोध, मान, माया और लोभसंज्वलनका कृष्टिकारक होता है और कृष्टिकरणके कालमें यह जीव इन कर्मोकी सत्त्वस्थितिका अपनी-अपनी बन्धस्थितिमें उत्कर्षण नहीं करता यही तथ्य यहाँ उक्त भाष्यगाथाके 'ओवट्टणा य णियमा' इस तीसरे चरण द्वारा स्पष्ट किया गया है। इस तथ्यको विशेषरूपसे समझनेके लिए १६४ क्रमांकवाली 'किट्टी करेदि णियमा' इत्यादि भाष्यगाथाके चूर्णिसूत्र और उसको जयधवला टीकापर दृष्टिपात करना चाहिये, क्योंकि उक्त गाथाकी व्याख्या करते हुए जो विशेष खुलासा किया गया है वह हृदयंगम करने लायक है। आशय यह है कि क्षपकणिपर आरूढ़ हुए जीवका पतन नहीं होता, इसलिए उसके मात्र कृष्टिकरणके प्रथम समयसे अपकर्षणकरणकी ही प्रवृत्ति होती है, उत्कर्षणकरणकी नहीं। यही बात उपशमश्रेणिपर चढ़नेवालेके भी जाननी चाहिये । मात्र उपशमश्रोणिसे पतन होनेपर जिस समय यह जीव सूक्ष्मसाम्परायमें प्रवेश कर कषायसहित होता है उसी समयसे इसके अपकर्षकरण और उत्कर्षणकरणकी प्रवृत्ति प्रारम्भ हो जाती है। अब प्रश्न यह है कि सूक्ष्मसाम्परायमें तो संज्वलन कषायका बन्ध होता नहीं। ऐसी अवस्थामें वहाँ उत्कर्षणकरणकी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है ? समाधान यह है कि उतरनेवाले उक्त जीवके कार्यरूपमें तो उत्कर्षणकरणकी प्रवृत्ति अनिवृत्तिकरणमें ही होती है, क्योंकि वहीं यथासम्भव मोहनीय कर्मका बन्ध होना पुनः प्रारम्भ होता है । यहाँ सूक्ष्मसाम्परायमें उतरनेवाले जीवके जो मोहनीयकर्मके उत्कर्षणकरणका निर्देश किया गया है सो वह शक्तिकी अपेक्षा ही जानना चाहिये । कृष्टिकरणके कालमें संज्वलन कषायके उत्कर्षणका जो निषेध किया गया है सो उसका आशय यह है कि उक्त कर्मकी द्वितीय स्थितिके स्थिति अनुभागका मात्र अपकर्षण ही होता है। तथा प्रथम स्थितिमें तो दो आवलिप्रमाण काल शेष रहनेपर ही आगाल-प्रत्यागालको व्युच्छित्ति हो जाती है। उसके पहले तक इन दोनोंका सद्भाव बना रहता है।
४३४. इस गाथाका इस प्रकारका अर्थ सुगम है ऐसा कथन करते हुए चूर्णिसूत्रकार इस सूत्रको कहते हैं