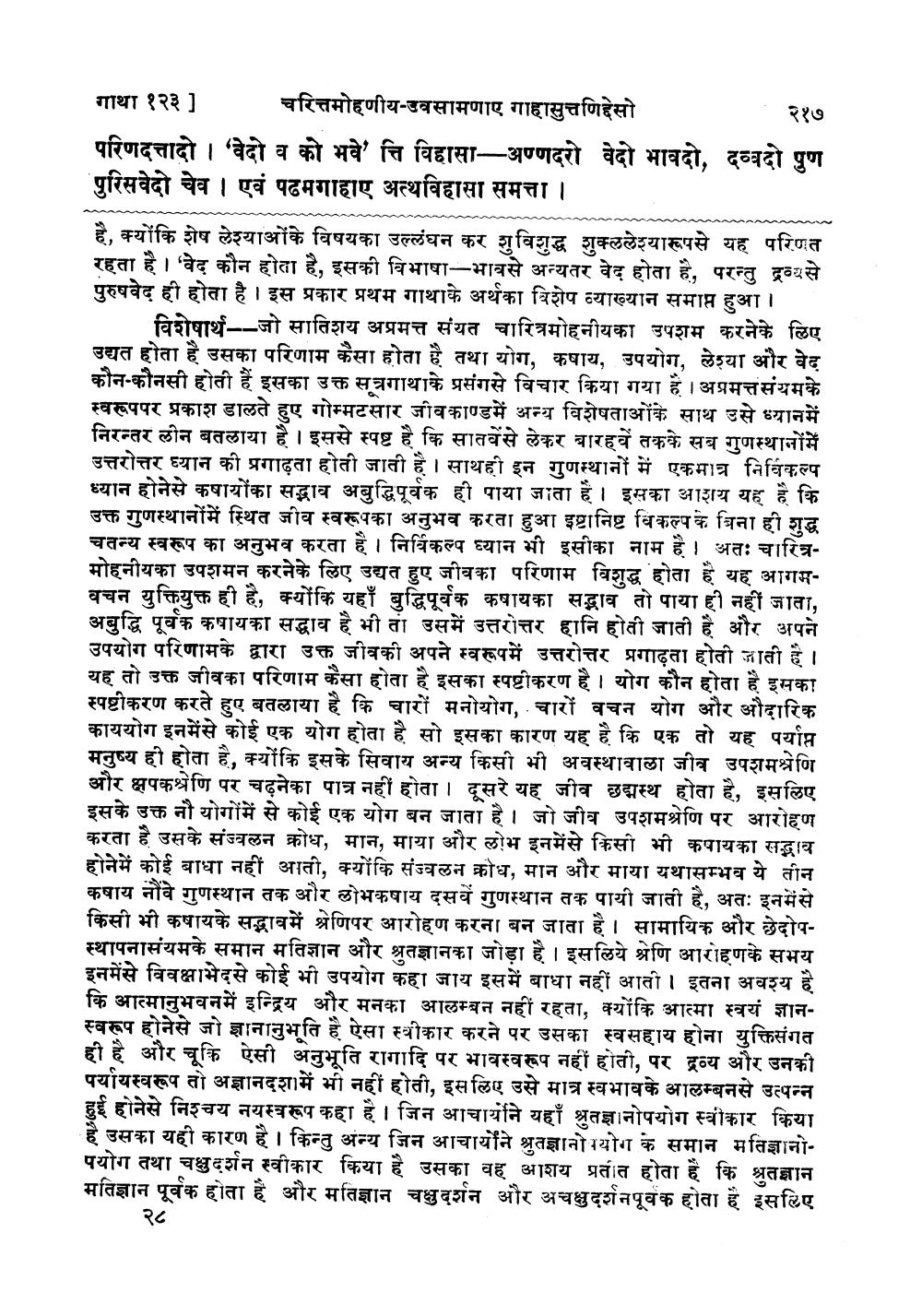________________
गाथा १२३] चरित्तमोहणीय-उवसामणाए गाहासुत्तणिद्देसो
२१७ परिणदत्तादो । 'वेदो व को भवे' त्ति विहासा-अण्णदरो वेदो भावदो, दव्वदो पुण पुरिसवेदो चेव । एवं पढमगाहाए अत्थविहासा समत्ता । है, क्योंकि शेष लेश्याओंके विषयका उल्लंघन कर शुविशुद्ध शुक्ललेश्यारूपसे यह परिणत रहता है। 'वेद कौन होता है, इसकी विभाषा-भावसे अन्यतर वेद होता है, परन्तु द्रव्य से पुरुषवेद ही होता है । इस प्रकार प्रथम गाथाके अर्थका विशेप व्याख्यान समाप्त हुआ।
विशेषार्थ--जो सातिशय अप्रमत्त संयत चारित्रमोहनीयका उपशम करनेके लिए उद्यत होता है उसका परिणाम कैसा होता है तथा योग, कषाय, उपयोग, लेश्या और वेद कौन-कौनसी होती हैं इसका उक्त सूत्रगाथाके प्रसंगसे विचार किया गया है । अप्रमत्तसंयमके स्वरूपपर प्रकाश डालते हुए गोम्मटसार जीवकाण्डमें अन्य विशेषताओंके साथ उसे ध्यानमें निरन्तर लीन बतलाया है । इससे स्पष्ट है कि सातवेंसे लेकर बारहवें तकके सब गुणस्थानोंमें उत्तरोत्तर ध्यान की प्रगाढ़ता होती जाती है। साथही इन गुणस्थानों में एकमात्र निर्विकल्प ध्यान होनेसे कषायोंका सद्भाव अबुद्धिपूर्वक ही पाया जाता है। इसका आशय यह है कि उक्त गुणस्थानोंमें स्थित जीव स्वरूपका अनुभव करता हुआ इष्टानिष्ट विकल्प के बिना ही शुद्ध चतन्य स्वरूप का अनुभव करता है । निर्विकल्प ध्यान भी इसीका नाम है। अतः चारित्रमोहनीयका उपशमन करनेके लिए उद्यत हुए जीवका परिणाम विशुद्ध होता है यह आगमवचन युक्तियुक्त ही है, क्योंकि यहाँ बुद्धिपूर्वक कषायका सद्भाव तो पाया ही नहीं जाता, अब
का सद्धाव है भी तो उसमें उत्तरोत्तर हानि होती जाती है और अपने उपयोग परिणामके द्वारा उक्त जीवकी अपने स्वरूपमें उत्तरोत्तर प्रगाढ़ता होती जाती है । यह तो उक्त जीवका परिणाम कैसा होता है इसका स्पष्टीकरण है। योग कौन होता है इसका स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया है कि चारों मनोयोग, चारों वचन योग और औदारिक काययोग इनमेंसे कोई एक योग होता है सो इसका कारण यह है कि एक तो यह पर्याप्त मनुष्य ही होता है, क्योंकि इसके सिवाय अन्य किसी भी अवस्थावाला जीव उपशमश्रेणि
और क्षपकश्रेणि पर चढ़नेका पात्र नहीं होता। दूसरे यह जीव छद्मस्थ होता है, इसलिए इसके उक्त नौ योगोंमें से कोई एक योग बन जाता है। जो जीव उपशमश्रेणि पर आरोहण करता है उसके संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ इनमेंसे किसी भी कपायका सद्भाव होने में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि संज्वलन क्रोध, मान और माया यथासम्भव ये तीन कषाय नौंवे गुणस्थान तक और लोभकषाय दसवें गुणस्थान तक पायी जाती है, अतः इनमें से किसी भी कषायके सद्भावमें श्रेणिपर आरोहण करना बन जाता है। सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमके समान मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका जोड़ा है। इसलिये श्रणि आराहणक समय इनमेंसे विवक्षाभेदसे कोई भी उपयोग कहा जाय इसमें बाधा नहीं आती। इतना अवश्य है कि आत्मानुभवनमें इन्द्रिय और मनका आलम्बन नहीं रहता, क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञानस्वरूप होनेसे जो ज्ञानानुभूति है ऐसा स्वीकार करने पर उसका स्वसहाय होना युक्तिसंगत ही है और चूकि ऐसी अनुभूति रागादि पर भावस्वरूप नहीं होती, पर द्रव्य और उनकी पर्यायस्वरूप तो अज्ञानदशामें भी नहीं होती, इसलिए उसे मात्र स्वभावके आलम्बनसे उत्पन्न हई होनेसे निश्चय नयस्वरूप कहा है। जिन आचार्याने यहाँ श्रतज्ञानोपयोग स्वीकार किर है उसका यही कारण है। किन्तु अन्य जिन आचार्योंने श्रुतज्ञानोपयोग के समान मतिज्ञानोपयोग तथा चक्षुदर्शन स्वीकार किया है उसका वह आशय प्रतीत होता है कि श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होता है और मतिज्ञान चक्षुदर्शन और अचक्षुदर्शनपूर्वक होता है इसलिए
२८