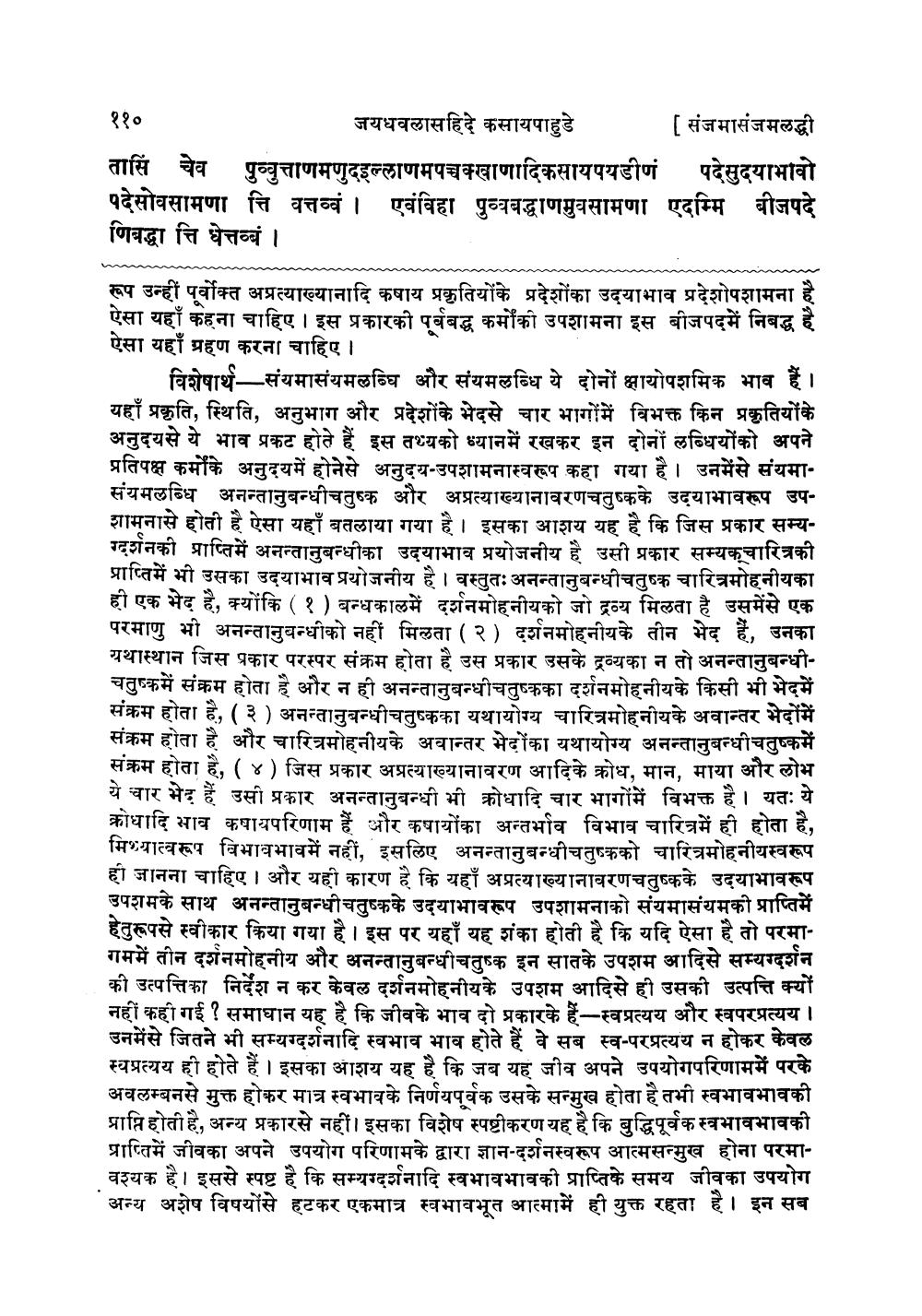________________
११०
जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [संजमासंजमलद्धी तासिं चेव पुव्वुत्ताणमणुदइल्लाणमपञ्चक्खाणादिकसायपयडीणं पदेसुदयाभावो पदेसोवसामणा त्ति वत्तव्वं । एवंविहा पुव्यबद्धाणमुवसामणा एदम्मि बीजपदे णिबद्धा त्ति घेत्तव्यं ।
रूप उन्हीं पूर्वोक्त अप्रत्याख्यानादि कषाय प्रकृतियोंके प्रदेशोंका उदयाभाव प्रदेशोपशामना है ऐसा यहाँ कहना चाहिए । इस प्रकारको पूर्वबद्ध कर्मोंकी उपशामना इस बीजपदमें निबद्ध है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए ।
विशेषार्थ-संयमासंयमलब्धि और संयमलब्धि ये दोनों क्षायोपशमिक भाव हैं। यहाँ प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंके भेदसे चार भागोंमें विभक्त किन प्रकृतियों के अनुदयसे ये भाव प्रकट होते हैं इस तथ्यको ध्यानमें रखकर इन दोनों लब्धियोंको अपने प्रतिपक्ष कर्मोंके अनुदयमें होनेसे अनुदय-उपशामनास्वरूप कहा गया है। उनमेंसे संयमासंयमलब्धि अनन्तानुबन्धीचतुष्क और अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके उदयाभावरूप उपशामनासे होती है ऐसा यहाँ बतलाया गया है। इसका आशय यह है कि जिस प्रकार सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिमें अनन्तानुबन्धीका उदयाभाव प्रयोजनीय है उसी प्रकार सम्यक प्राप्तिमें भी उसका उदयाभाव प्रयोजनीय है। वस्तुतः अनन्तानुबन्धीचतुष्क चारित्रमोहनीयका ही एक भेद है, क्योंकि ( १ ) बन्धकालमें दर्शनमोहनीयको जो द्रव्य मिलता है उसमेंसे एक परमाणु भी अनन्तानुबन्धीको नहीं मिलता ( २) दर्शनमोहनीयके तीन भेद हैं, उनका यथास्थान जिस प्रकार परस्पर संक्रम होता है उस प्रकार उसके द्रव्यका न तो अनन्तानुबन्धीचतुष्कमें संक्रम होता है और न ही अनन्तानुबन्धीचतुष्कका दर्शनमोहनीयके किसी भी भेदमें संक्रम होता है, (३) अनन्तानबन्धीचतष्कका यथायोग्य चारित्रमोहनीयके अवान्तर भेदोंमें संक्रम होता है और चारित्रमोहनीयके अवान्तर भेदोंका यथायोग्य अनन्तानुबन्धीचतुष्कमें संक्रम होता है, ( ४ ) जिस प्रकार अप्रत्याख्यानावरण आदिके क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार भेद हैं उसी प्रकार अनन्तानुबन्धी भी क्रोधादि चार भागोंमें विभक्त है। यतः ये क्रोधादि भाव कषायपरिणाम हैं और कषायोंका अन्तर्भाव विभाव चारित्रमें ही होता है, मिथ्यात्वरूप विभावभावमें नहीं, इसलिए अनन्तानुबन्धीचतुष्कको चारित्रमोहनीयस्वरूप ही जानना चाहिए । और यही कारण है कि यहाँ अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके उदयाभावरूप उपशमके साथ अनन्तानुबन्धीचतुष्कके उदयाभावरूप उपशामनाको संयमासंयमको प्राप्तिमें हेतुरूपसे स्वीकार किया गया है। इस पर यहाँ यह शंका होती है कि यदि ऐसा है तो परमागममें तीन दर्शनमोहनीय और अनन्तानुबन्धीचतुष्क इन सातके उपशम आदिसे सम्यग्दर्शन की उत्पत्तिका निर्देश न कर केवल दर्शनमोहनीयके उपशम आदिसे ही उसकी उत्पत्ति क्यों नहीं कही गई ? समाधान यह है कि जीवके भाव दो प्रकारके हैं-स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय । उनमें से जितने भी सम्यग्दर्शनादि स्वभाव भाव होते हैं वे सब स्व-परप्रत्यय न होकर केवल स्वप्रत्यय ही होते हैं। इसका आशय यह है कि जब यह जीव अपने उपयोगपरिणाममें परके अवलम्बनसे मुक्त होकर मात्र स्वभावके निर्णयपूर्वक उसके सन्मुख होता है तभी स्वभावभावकी प्राप्ति होती है, अन्य प्रकारसे नहीं। इसका विशेष स्पष्टीकरण यह है कि बुद्धिपूर्वक स्वभावभावकी प्राप्तिमें जीवका अपने उपयोग परिणामके द्वारा ज्ञान-दर्शनस्वरूप आत्मसन्मुख होना परमावश्यक है। इससे स्पष्ट है कि सम्यग्दर्शनादि स्वभावभावकी प्राप्तिके समय जीवका उपयोग अन्य अशेष विषयोंसे हटकर एकमात्र स्वभावभूत आत्मामें ही युक्त रहता है। इन सब