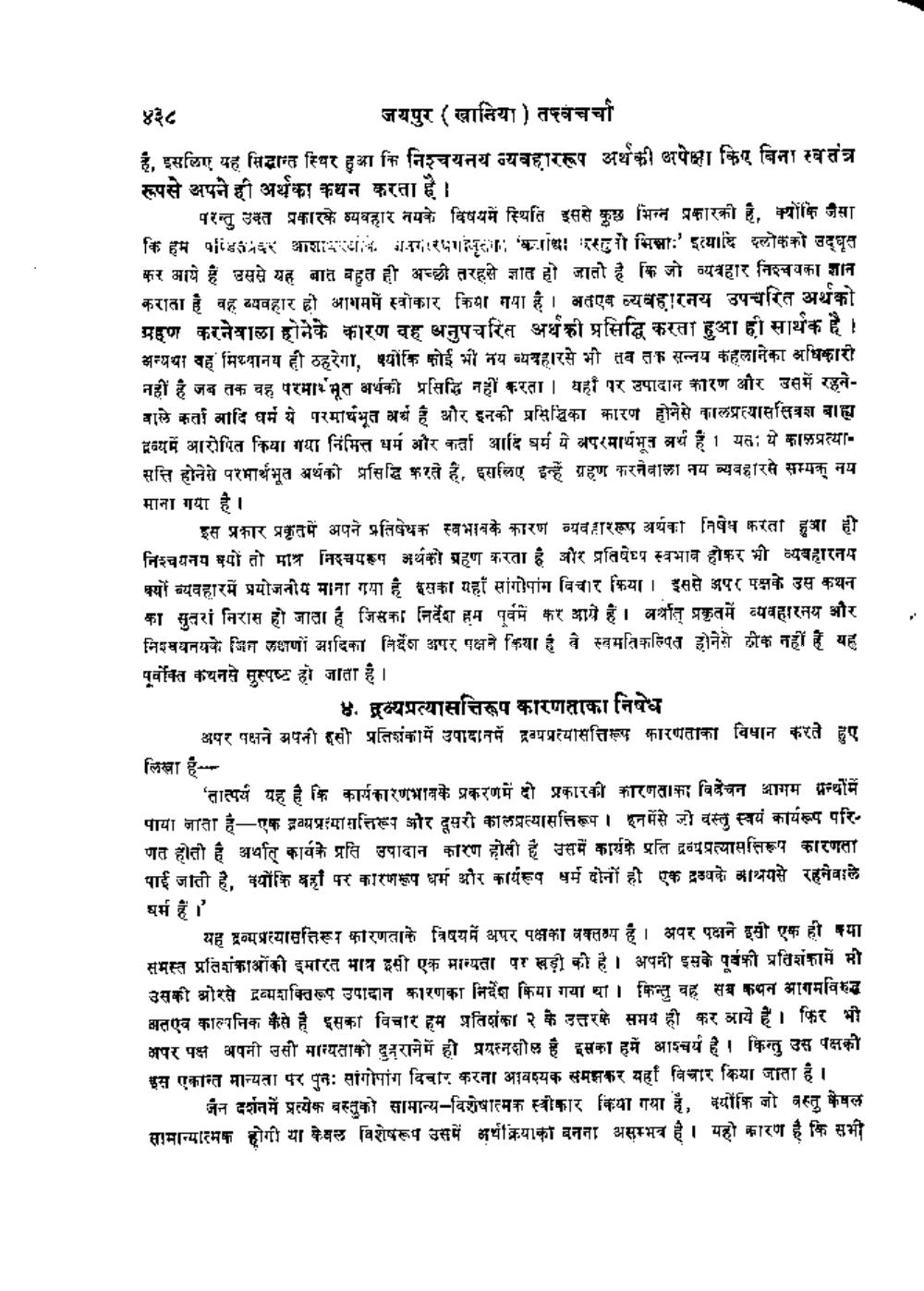________________
४३८
जयपुर (खानिया) तवचर्चा
हैं, इसलिए यह सिद्धान्त स्थिर हुआ कि निश्चयनय व्यवहाररूप अर्थकी अपेक्षा किए बिना स्वतंत्र रूपसे अपने ही अर्थका कथन करता है ।
परन्तु उक्त प्रकारके व्यवहार नयके विषय में स्थिति इससे कुछ भिन्न प्रकारकी है, क्योंकि जैसा कि हम पनि आशा अजगार भिन्नाः' इत्यादि दलोकको उद्घृत कर आये हैं उससे यह बात बहुत ही अच्छी तरहसे ज्ञात हो जाती है कि जो व्यवहार निश्चवका ज्ञान कराता है वह व्यवहार हो आगम में स्वीकार किया गया है। अतएव व्यवहारनय उपचरित अर्थको ग्रहण करनेवाला होनेके कारण वह अनुपचरित अर्धकी प्रसिद्धि करता हुआ ही सार्थक है । अन्यथा वह मिथ्यानय हो ठहरेगा, क्योंकि कोई भी नय व्यवहार से भी तब तक सन्नय कहलाने का अधिकारी नहीं है जब तक वह परमार्थभूत अर्थको प्रसिद्धि नहीं करता। यहाँ पर उपादान कारण और उसमें रहनेवाले कर्ता आदि धर्म ये परमार्थभूत अर्थ हैं और इनकी प्रसिद्धिका कारण होनेसे कालप्रत्यासतिश बाह्य arमें आरोपित किया गया निमित्त धर्म और कर्ता आदि धर्म ये अपरमार्थभूत अर्थ हैं । यतः ये कालप्रत्यासत्ति होने से परमार्थभूत अर्थको प्रसिद्धि करते हैं, इसलिए इन्हें ग्रहण करनेवाला नाय व्यवहारसे सम्यक् नय माना गया है ।
इस प्रकार प्रकृत में अपने प्रतिषेधक स्वभाव के कारण व्यवहाररूप अर्थका निषेध करता हुआ हो निश्चयनय क्यों तो मात्र निश्चयरूप अर्थको ग्रहण करता है और प्रतिषेध्य स्वभाव होकर भी व्यवहारनप व्यवहार में प्रयोजनीय माना गया है इसका यहाँ सांगोपांग विचार किया। इससे अपर पक्षके उस कथन का सुतरां निरास हो जाता है जिसका निर्देश हम पूर्वमें कर आये हैं । वर्षात् प्रकृतमें व्यवहारनय और निश्वयनयके जिन क्षणों आदिका निर्देश अगर पक्षने किया है वे स्वमतिकल्पित होनेसे ठीक नहीं है यह पूर्वोक्त कथन से सुस्पष्ट हो जाता है ।
४. द्रव्यप्रत्यासत्तिरूप कारणताका निषेध
अपर पक्षने अपनी इसी प्रतिशंका में उपादानमें द्रव्यप्रत्यासत्तिरूप कारणताका विधान करते हुए लिखा है---
'तात्पर्य यह है कि कार्यकारणभाव के प्रकरण में दो प्रकारको कारणता का विवेचन आगम ग्रन्थोंमें पाया जाता है— एक द्रव्यप्रत्यासत्तिरूप और दूसरी कालप्रत्यासतिरूप । इनमें से जो वस्तु स्वयं कार्यरूप परि त होती है अर्थात् कार्यके प्रति उपादान कारण होती है उसमें कार्यके प्रति द्रव्यप्रत्यासतिरूप कारणता पाई जाती है, क्योंकि वहीं पर कारणरूप धर्म और कार्यरूप धर्म दोनों ही एक द्रव्यके बाश्रयसे रहनेवाले धर्म हैं ।'
है।
अपर पक्षने इसी एक ही क्या अपनी इसके पूर्वी प्रतिशंका में मी
किन्तु वह सब कथन आगमविरुद्ध
यह द्रव्यत्यासत्तिरूप कारणता के विषय में अपर पक्षका वक्तव्य समस्त प्रतिशंकाओं की इमारत मात्र इसी एक मान्यता पर खड़ी की है। उसकी ओरसे द्रव्यशक्तिरूप उपादान कारणका निर्देश किया गया था अतएव काल्पनिक कैसे है इसका विचार हम प्रतिशंका २ के उत्तरके अपर पक्ष अपनी उसी मान्यताको दुहराने में ही प्रयत्नशील है इसका हमें आश्चर्य है । किन्तु उस पक्ष की
।
समय ही कर आये है। फिर भी
इस एकान्त मान्यता पर पुनः सांगोपांग विचार करना आवश्यक समझकर यहाँ विचार किया जाता है ।
जैन दर्शन में प्रत्येक बस्तुको सामान्य- विशेषात्मक स्वीकार किया गया है, सामान्यात्मक होगी या केवल विशेषरूप उसमें अर्थक्रियाका बनना असम्भव है ।
क्योंकि जो वस्तु केवल यही कारण है कि सभी