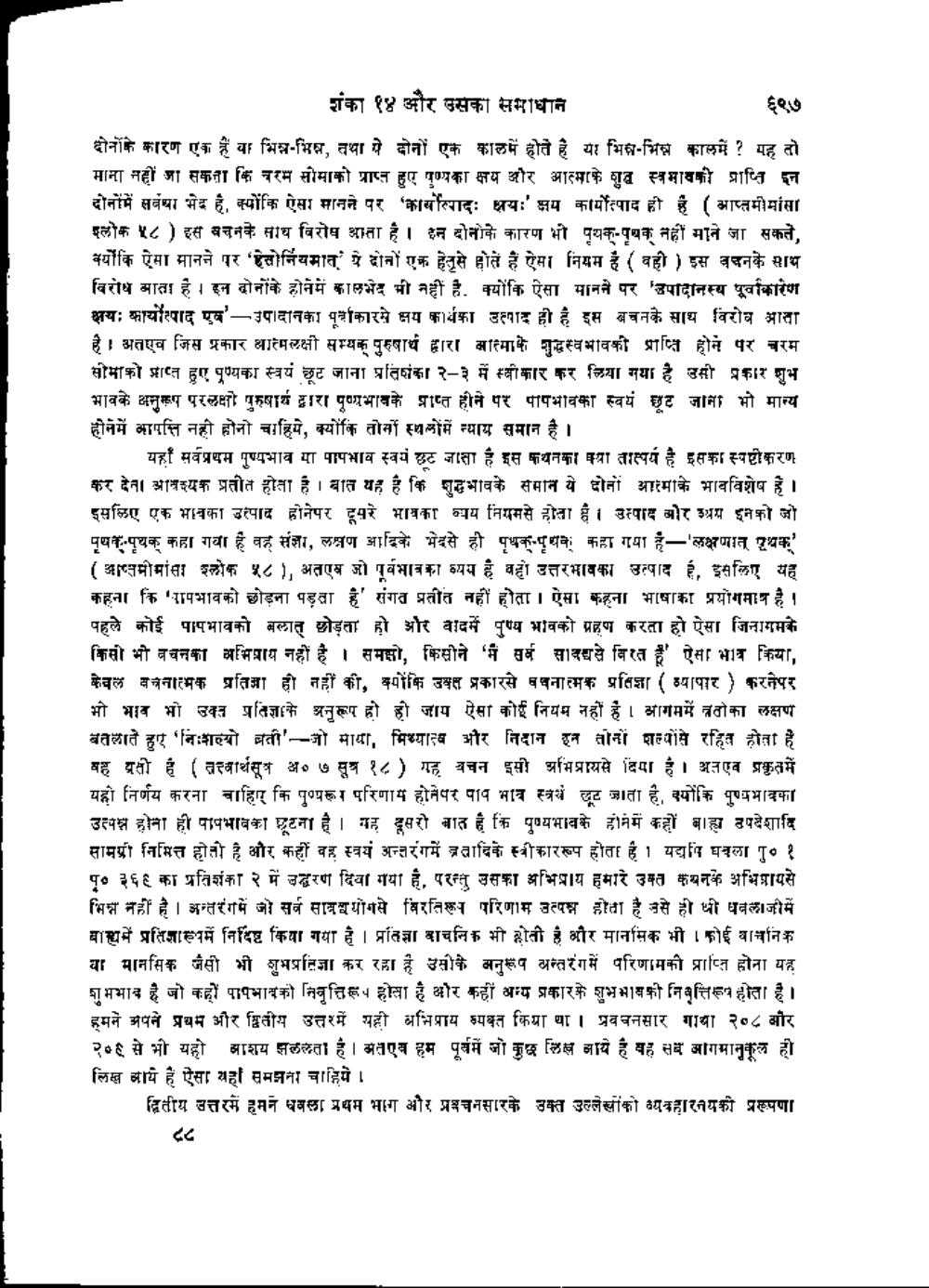________________
शंका १४ और उसका समाधान दोनोंके कारण एक हैं वा भिन्न-भिन्न, तथा ये दोनों एक कालमें होते है या भिन्न-भिन्न कालमें ? यह तो मामा नहीं जा सकता कि चरम सीमाको प्राप्त हए पूण्यका क्षय और आत्मा के शुद्ध स्त्रमावकी प्राप्ति इन दोनों में सर्वथा भेद है, क्योंकि ऐसा मानने पर कार्योत्पादः क्षयः'क्षय कार्योत्पाद ही है (आप्तमीमांसा श्लोक १८ ) इस वचन के साथ विरोष आता है। इन दोनोके कारण भी पृथक-पृथक नहीं माने जा सकते, क्योंकि ऐसा मानने पर 'हेसोनियमात ये दोनों एक हेतसे होते हैं ऐसा नियम है ( वही) इस वचनके साथ विरोध माता है । इन दोनोंके होने में कालभेद भी नहीं है. क्योंकि ऐसा मानने पर 'उपादानस्य पूर्वाकारण शयः कार्योत्पाद एवं'-उपादानका पत्रकारसे क्षय कार्यका उत्पाद ही है इस बचनके साथ विरोव आता है। अतएव जिस प्रकार यात्मलक्षी सम्यक पुरुषार्थ द्वारा आत्माके शुद्धस्वभावकी प्राप्ति होने पर चरम सीमाको प्राप्त हुए पुण्यका स्वयं छूट जाना प्रतिशंका २-३ में स्वीकार कर लिया गया है उसी प्रकार शुभ भावके अनुरूप परलक्षो पुरुषार्थ द्वारा पुण्यभावके प्राप्त होने पर पापभावका स्वयं छुट जाना भो मान्य होने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये, क्योंकि तोमो स्थलों में न्याय समान है।
यहाँ सर्वप्रथम पुण्यभाव या पापभाव स्वयं छट जाता है इस कथनका क्या तात्पर्य है इसका स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। बात यह है कि शुद्धभावके समान ये दोनों आत्माके भावविशेष है। इसलिए एक भावका उत्पाद होनेपर दूसरे भावका ब्यय नियमसे होता है। उत्पाद और श्रम इनको जो पृथक पृथक कहा गया है वह संज्ञा, लत्रण आदिके भेदसे ही पृथक्-पृथक कहा गया है-'लक्षणात पृथक ( आप्तमीमांसा श्लोक ५८), अतएव जो पूर्वभावका ध्यय है वहो उत्तरभावका उत्पाद है, इसलिए यह कहना कि 'रापभावको छोड़ना पड़ता है' संगत प्रतीत नहीं होता। ऐसा कहना भाषाका प्रयोगमात्र है। पहले कोई पापभावको बलात् छोड़ता हो और बादमें पुण्य भावको ग्रहण करता हो ऐसा जिनाममके किसी भी वचनका अभिप्राय नहीं है । समझो, किसीने 'मैं सर्व साधसे विरत है ऐसा भाव किया, केवल वचनात्मक प्रतिमा ही नहीं की, क्योंकि उक्त प्रकारसे पवनात्मक प्रतिज्ञा ( व्यापार ) करनेपर भो भाव भो उक्त प्रतिज्ञा के अनुरूप हो हो जाय ऐसा कोई नियम नहीं है। आगममें व्रतो का लक्षण बतलाते हुए निःशल्यो ब्रती-जो माया, मिथ्यात्व और निदान इन तीनों शल्पोंसे रहित होता है वह प्रती है ( तत्वार्थसूत्र अ०७ सूत्र १८) यह वचन इसी अभिप्रायसे दिया है। अतएव प्रकृतमें यही निर्णय करना चाहिए कि पुण्यरूप परिणाम होनेपर पाप भाव स्त्र टूट जाता है, क्योंकि पुण्यभावका उत्पन्न होना ही पापभावका छूटना है। यह दूसरी बात है कि पुण्यभावके होममें कहीं बाह्य उपदेशादि सामग्री निमित्त होती है और कहीं वह स्वयं अन्तरंगमें व्रतादिके स्वीकाररूप होता है । यद्यपि घवला पु०१ पु० ३६६ का प्रतिज्ञका २ में उद्धरण दिया गया है, परन्तु उसका अभिप्राय हमारे उक्त कथनके अभिप्रायसे भिन्न नहीं है । अन्तरंगमें जो सर्व साबश्व योगसे विरतिरूप परिणाम उत्पन्न होता है उसे ही धी धवलाजी में
में प्रतिज्ञापमें निर्दिष्ट किया गया है। प्रतिज्ञा वाचनिक भी होती हैं और मानसिक भी । कोई वानिक वा मानसिक जैसी भी शुभप्रतिज्ञा कर रहा है उसीके अनुरूप अन्तरंग में परिणामकी प्राप्ति होना यह शुभभाव है जो कहीं पापभावको निवृत्तिरूप होता है और कहीं अन्य प्रकारके शुभभावकी निवृत्तिरूप होता है। हमने अपने प्रथम और द्वितीय उत्तरमें यही अभिप्राय व्यक्त किया था। प्रवचनसार गाथा २०८ और २०६ से भी यही आशय झललता है। अतएव हम पूर्वमें जो कुछ लिल आये है वह सब आगमानुकूल ही लिव आये हैं ऐसा यह समझना चाहिये।
द्वितीय उत्तरम हमने धवला प्रथम भाग और प्रवचनसारके उक्त उल्लेखोंको व्यवहारमयकी प्ररूपणा
८८