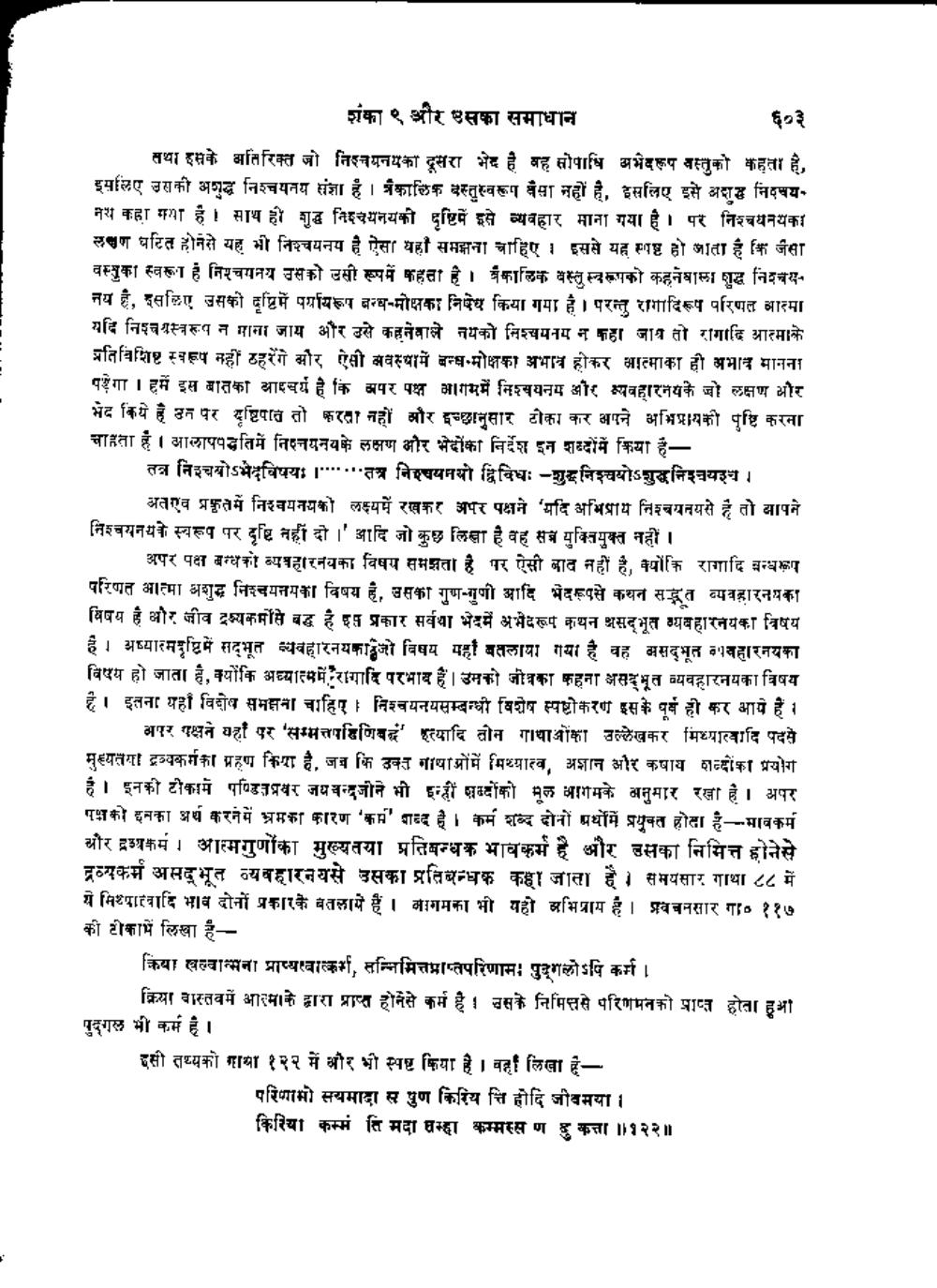________________
शंका ९ और उसका समाधान
६०३ सथा इसके अतिरिक्त जो निश्चयनयका दूसरा भेद है वह सोपाधि अभेदरूप वस्तुको कहता है, इसलिए उस की अशुद्ध निश्चयनय संज्ञा है । कालिक वस्तुस्वरूप पैसा नहीं है, इसलिए इसे अशुस निश्चय नय कहा गया है। साथ ही शुद्ध निश्चयनयको दृष्टि में इसे व्यवहार माना गया है। पर निश्चयनयका
पटित होनसे यह भी निश्चयनय है ऐसा यहाँ समझना चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जैसा वस्तुका स्वरूप है निश्चयनय उसको उसी रूप में कहता है। बकालिक वस्तू स्वरूपको कहनेवाला शुद्ध निश्चय नय है, इसलिए उसको दृष्टि में पर्यायरूप बन्ध-मोक्षका निषेध किया गया है। परन्तु रागादिरूप परिणल आत्मा यदि निश्चयस्त्ररूप न माना जाय और उसे कहनेवाले नयको निश्चयन न कहा जाय तो रागादि आत्माके प्रतिविशिष्ट स्वरूप नहीं ठहरेंगे और ऐसी अवस्था बन्ध-मोक्षका अभाव होकर आत्माका ही अभाव मानना पड़ेगा । हमें इस बातका आश्चर्य है कि अपर पक्ष आगममें निश्चयनय और व्यवहारनयके जो लक्षण और भेद किये है उस पर दृष्टिपात तो करता नहीं और इच्छानुसार टोका कर अपने अभिप्रायकी पुष्टि करना चाहता है । आलापपद्धतिमें निश्नयनयके लक्षण और भेदोंका निर्देश इन शब्दों में किया है
तत्र निश्चयोऽभेदविषयः ।.....'तत्र निश्चयमयो द्विविधः -शुद्ध निश्चयोऽशुद्धनिश्चयश्च ।
अतएव प्रकृतम निश्चयनयको लक्ष्य में रखकर अपर पक्षने 'यदि अभिप्राय निश्चयनयसे है तो आपने निश्चयनयके स्वरूप पर दृष्टि नहीं दो ।' आदि जो कुछ लिखा है वह सब युक्तियुक्त नहीं ।
अपर पक्ष बन्धको व्यवहारनयका विषय समझता है पर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रागादि बन्धका परिणत आत्मा अशुद्ध निश्चयनयका विषय है, उसका गुण-गुणी आदि भेदरूपसे कथन सद्भत व्यवहारनयका विषय है और जीव द्रश्यकर्मोसे बद्ध है इस प्रकार सर्वथा भेदमें अभेदरूप कथन असद्भुत व्यवहारनयका विषय है। अध्यात्मदृष्टि में सद्भूत व्यवहारनयकाहजो विषय पहाँ बतलाया गया है वह असद्भूत आवहारनयका विषय हो जाता है, क्योंकि अच्यात्ममें रागादि परभाव हैं। उनको जोत्रका कहना असद्भुत व्यवहारनयका विषय है। इतना यहाँ विदोष समझना चाहिए। निश्चयनयसम्बन्धी विशेष स्पष्टीकरण इसके पूर्व ही कर आये हैं।
अपर पक्षने यहाँ पर 'सम्मत्तपखिणिवई' इत्यादि तीन गाथाओंका उल्लेखकर मिथ्यात्वादि पदसे मुख्यतया द्रश्वकर्मका ग्रहण किया है, जब कि उक्त गाथाओंमें मिथ्यात्व, अज्ञान और कषाय शब्दों का प्रयोग है। इनकी टोकाम पण्डितप्रवर जयचन्दजीने भी इन्हीं शब्दोंको मूल आगमके अनुमार रखा है। अपर पक्षको इनका अर्थ करने में भ्रमका कारण 'क' शब्द है। कर्म शब्द दोनों प्रोंमें प्रयुक्त होता है--मावकर्म
और द्रश्यकर्म । आत्मगुणोंका मुख्यतया प्रतिबन्धक भावकर्म है और उसका निमित्त होनेसे द्रव्यकर्म असद्भूत व्यवहारन यसे उसका प्रतिबन्धक कहा जाता है। समयसार गाथा ८८ में ये मिथ्यात्वादि भाव दोनों प्रकारके बतलाये हैं। मागमका भी यही अभिप्राय है। प्रवचनसार गा०११७ की टीका लिखा है
किया खल्वान्मना प्राप्यत्वाकर्म, सन्निमित्तप्राप्तपरिणामः पुदगलोऽपि कर्म ।
क्रिया वास्तवमें आत्माके द्वारा प्राप्त होनेसे कर्म है। उसके निमित्तसे परिणमनको प्राप्त होता हुआ पुद्गल भी कम है। इसी तथ्यको गाथा १२२ में और भी स्पष्ट किया है। वह लिखा है
परिणामो सयमादा स पुण किरिय त्ति होदि जीवमया। किरिया कम्मं ति मदा घम्हा कम्मरस ण टु कत्ता ॥१२२॥