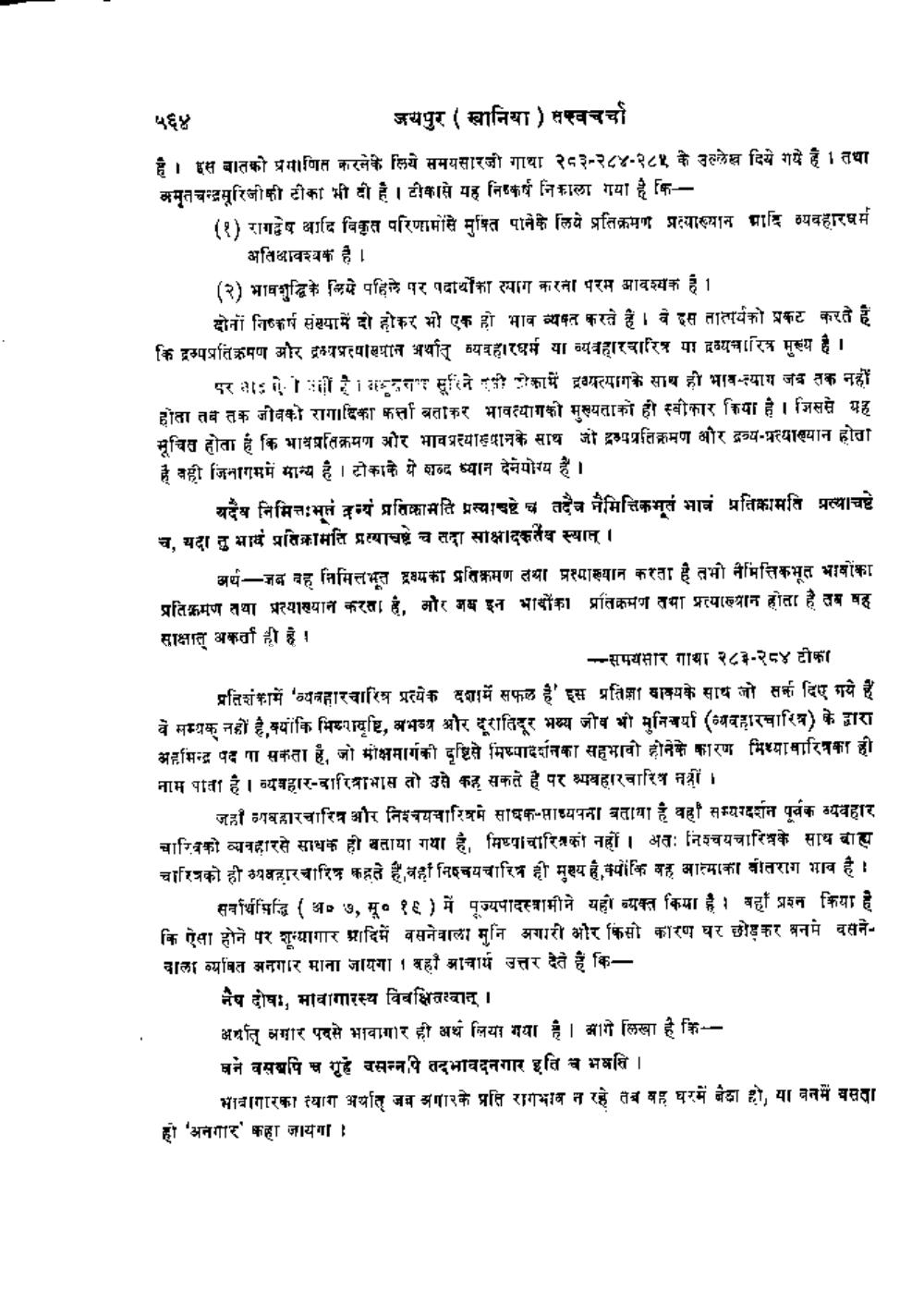________________
५६४
जयपुर ( वानिया) सस्वचर्चा है। इस बातको प्रमाणित करने के लिये समयसारजी गाथा २५३-२८४.२८५ के उल्लेख दिये गये हैं 1 तथा अमृतचन्द्रसुरिजी की टीका भी दी है । टीकासे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि(१) रागद्वेष आदि विकृत परिणामोंसे मुक्ति पाने के लिये प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान मादि व्यवहारधर्म
अतिवावश्यक है। (२) भाषशुद्धि के लिये पहिने पर पदार्थोका त्याग करना परम आवश्यक है 1
दोनों निष्कर्ष संख्यामें दो होकर भी एक हो भाव व्यक्त करते हैं। वे इस तात्पर्यको प्रकट करते हैं कि द्रम्पप्रतिक्रमण और द्रन्धप्रत्यास्पान अर्थात् व्यवहारधर्म या व्यवहारचारित्र या द्रव्यचारित्र मुख्य है।
परीवस्य सरिने पोकामें व्यत्यागके साथ ही भाव-त्याग जब तक नहीं होता तब तक जीवको रागादिका कर्ता बताकर भावत्यागकी मुख्यताको ही स्वीकार किया है। जिससे यह मुचित होता है कि भावप्रतिक्रमण और भावप्रत्याख्यानके साथ जो द्रव्यप्रतिक्रमण और द्रव्य-प्रत्याख्यान होता है वही जिनागममें मान्य है । टोकाके ये शब्द ध्यान देने योग्य है।
यदेव निमित्त भत्तं वन्य प्रतिकामति प्रत्याच च तदैव नैमित्तिकमतं भावं प्रतिकामति प्रत्याचष्टे च, यदा तु भाव प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदा साक्षादकतेव स्याप्त ।
अर्थ-जब वह निमित्तभूत दूधयका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है तभी नैमित्तिकभूत भावोंका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है, और जब इन भादोंका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान होता है तब वह साक्षात् अकर्ता ही है।
-समयसार गाथा २८३-२८४ टीका प्रतिशंकामें 'व्यवहारचारित्र प्रत्येक दशामें सफल है' इस प्रतिमा वाक्यके साथ जो सर्क दिए गये हैं वे सम्यक नहीं है,क्योंकि मियादृष्टि, अभय और दूरातिदूर भव्य जीव भी मुनिचर्या (व्यवहारचारित्र) के द्वारा अहमिन्द्र पद पा सकता है, जो मोक्षमार्गकी दृष्टिसे मिध्यादर्शनका सहभावी होने के कारण मिथ्यावारित्रका ही नाम पाता है। व्यवहार-चारित्राभास तो उसे कह सकते है पर श्यवहारवारिवनी ।
जहाँ व्यवहारचारित्र और निश्चयचारित्रम साधक-प्ताध्यपना बताया है वहाँ सम्यग्दर्शन पूर्वक व्यवहार चारिखको व्यवहारसे साधक ही बताया गया है, मिथ्याचारित्रको नहीं। अतः निश्चय चारित्रके साथ बाह्य चारित्रको ही व्यवहारचारित्र कहते हैं, वहां निश्चयचारित्र ही मुख्य है क्योंकि वह आत्माका वीतराग भाव है।
सर्वार्थपिद्धि ( अ० ७, मू०१६ ) में पूज्यपादस्वामीने यही व्यक्त किया है। वहाँ प्रश्न किया है कि ऐसा होने पर शून्यागार प्रादिमें वसनेवाला मुनि अगारी और किसी कारण घर छोड़कर अनमै बसनेवाला व्यषित अनगार माना जायगा । वही आचार्य उत्तर देते हैं कि
नेप दोषा, मावागारस्य विवक्षितत्वात् । अर्थात् अगार पवसे भावागार ही अर्थ लिया गया है। आगे लिखा है कि-- घने वसमपि च गृह बसन्नपि तदभावदनगार इति च भवति ।
भावागारका त्याग अर्थात जब अगारके प्रति रागभाव न रहे तब वह घरमें बैठा हो, या वनमें बसता हो 'अनगार' कहा जायगा।