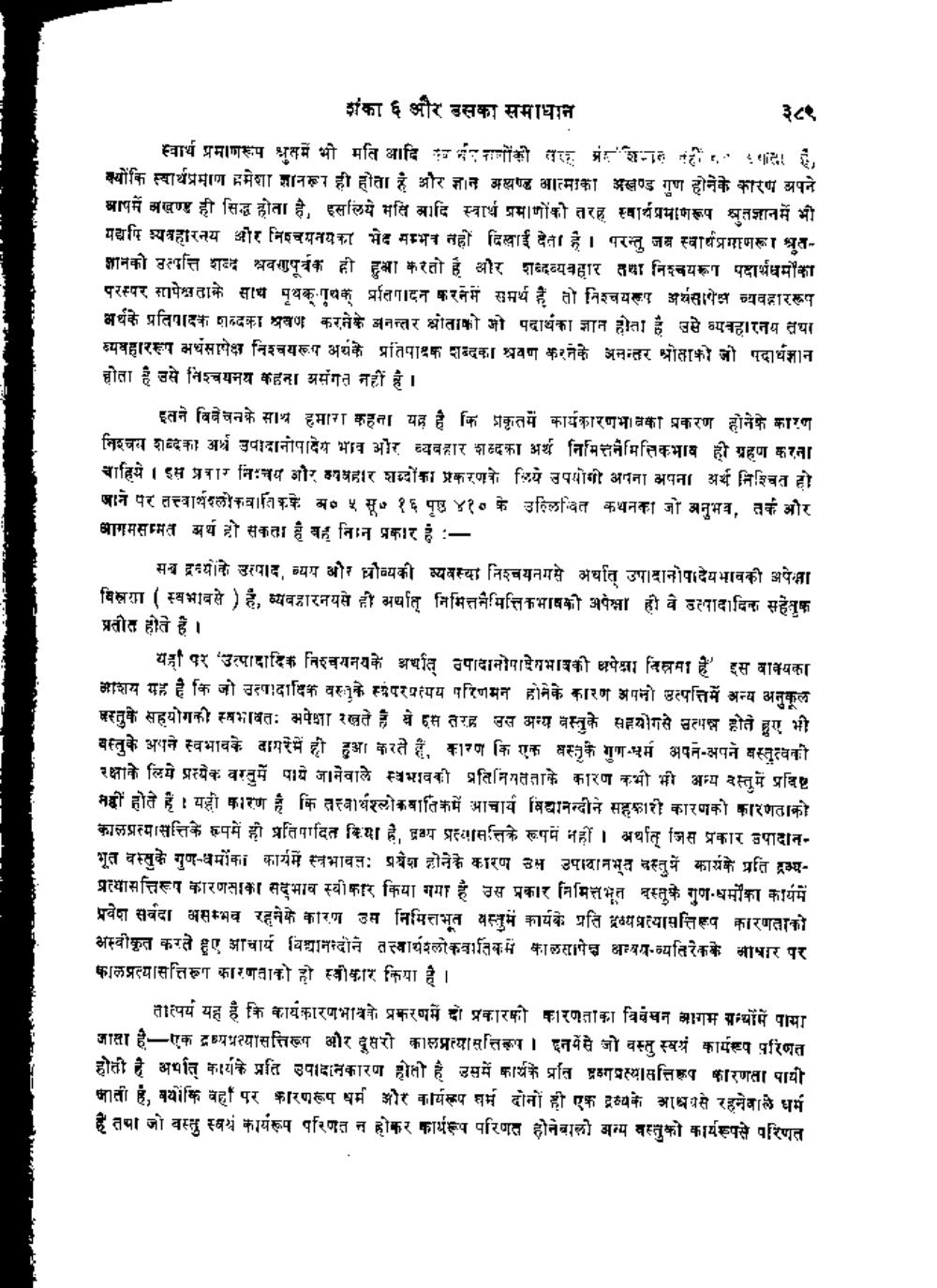________________
का ६ और उसका समाधान स्वार्थ प्रमाणरूप भूत में भी मति आदि नामोंकी वर. अंश-रू नहीं पाता है, क्योंकि स्वार्थप्रमाण हमेशा शानका ही होता है और ज्ञान अध्यण्ड आत्माका अखण्ड गुण होनेके कारण अपने आपमें अखण्ड ही सिद्ध होता है, इसलिये मति आदि स्वार्थ प्रमाणोंकी तरह स्वार्थ प्रमाणरूप श्रुतज्ञान में भी यद्यपि यत्रहारनय और निश्चयनयका भेद सम्भव नहीं दिखाई देता है। परन्तु जब स्वार्थप्रमाणला श्रुतज्ञानको उत्पत्ति शब्द श्रवणुपूर्वक ही हुआ करतो है और शब्दव्यवहार तथा निश्चयका पदार्थधौका परस्पर सापेश्श ताके साथ पृथक् गायक प्रतिपादन करने में समर्थ हैं तो निश्च यरूप अर्थसापेक्ष व्यवहाररूप अर्थ के प्रतिपादक शब्दका श्रवण करने के अनन्तर श्रोताको जो पदार्थका ज्ञान होता है उसे व्यवहारनय तथा व्यवहाररूप अर्थसापेक्ष निश्चयरूप अर्थके प्रतिपादक शब्दका श्रवण करनेके अनन्तर श्रोताको जो पदार्थज्ञान होता है उसे निश्चयमय कहना असंगत नहीं है।
इतने विवेचन के साथ हमारा कहना यह है कि कृतम कार्यकारणभा का प्रकरण होने के कारण निश्चय शब्दका अर्थ उपादानोपादेय भाव और व्यवहार शब्दका अर्थ निमित्तनैमित्तिकभाष ही ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार निःचय और पबहार शब्दोंका प्रकरणके लिये उपयोगी अपना अपना अर्थ निश्चित हो जाने पर तत्त्वार्थरलोकवाति कफे २० ५ सू. १६ पृष्ठ ४१० के उल्लिवित कथनका जो अनुभव, तर्क और आगमसम्मत अर्थ हो सकता है वह निम्न प्रकार है :
सब द्रव्योंके उत्पाद, व्यय और धौव्यकी व्यवस्था निश्चयनय से अर्थात उपादानोपादेयभावको अपेक्षा विसया ( स्वभावसे )है, व्यवहारनयसे ही अर्थात निमित्तनैमित्तिकभाषकी अपेक्षा ही वे उत्पादादिक सहेलक प्रतीत होते हैं।
यहां पर उत्पादादिक विश्वयनयके अर्थात् उपादानोपावभावकी अपेक्षा दिनमा हैं। इस वाक्यका आशय यह है कि जो उत्पादादिक वस्तके स्परप्रत्यय परिणमन होने के कारण अपनो उत्पत्ति में अन्य अनुकूल पस्तुके सहयोगको स्वभावतः अपेक्षा रखते हैं वे इस तरह उस अन्य वस्तुके सहयोगसे उत्पन्न होते हुए भी वस्तुके अपने स्वभावके दायरे में ही हुआ करते हैं, कारण कि एक वस्तके गुण-धर्म अपने-अपने वस्तत्वको रक्षाके लिये प्रत्येक वस्तुमें पाये जानेवाले स्वभावकी प्रतिनियतताके कारण कभी भी अन्य वस्तु में प्रविष्ट महीं होते हैं। यही कारण है कि तत्वार्थश्लोकवातिकमें आचार्य विद्यानन्दीने सहकारी कारणको कारणताको कालप्रत्मासत्तिके रूपमें ही प्रतिपादित किया है, द्रव्य प्रत्यासत्तिके रूपमें नहीं। अर्थात् जिस प्रकार उपादानभूत वस्तुके गुण-धमाका कार्य में स्वभावत: प्रवेश होने के कारण उस उपायानभूत दस्तु में कार्य के प्रति द्रश्यप्रत्यासत्तिरूप कारणसाका सद्भाव स्वीकार किया गया है उस प्रकार निमित्तभूत बस्तुके गुण-धर्मोका कार्यम प्रवेश सर्वदा असम्भव रहने के कारण उस निमित्तभूत वस्तुमै कार्यके प्रति द्रव्य प्रत्यासत्तिहप कारणताको अस्वीकृत करते हुए आचार्य विद्यानन्दीने तत्वार्यश्लोकवातिय में कालसापेन अध्यय-व्यतिरेकके आधार पर कालप्रत्यासत्तिका कारणताको हो स्वीकार किया है।
तात्पर्य यह है कि कार्यकारणभाव प्रकरणमें दो प्रकारको कारणताका विवंचन आगम ग्रन्थों में पाया जाता है-एक द्रध्ययस्यासत्तिरूप और दुसरो कालप्रत्यासत्तिका। इनमें से जो वस्तु स्वयं कार्यरूप परिणत होती है अर्थात कार्य के प्रति उपादानकारण होती है उसमें कार्य प्रति प्रगप्रस्थासतिरूप कारणता पायी जाती है, क्योंकि वहाँ पर कारणरूप धर्म और कार्यरूप धर्म दोनों ही एक द्रव्यके आधसे रहनेवाले धर्म है तथा जो वस्तु स्वयं कार्यरूप परिणत न होकर कार्यरूप परिणत होनेवालो अन्य वस्तुको कार्यरूपसे परिणत