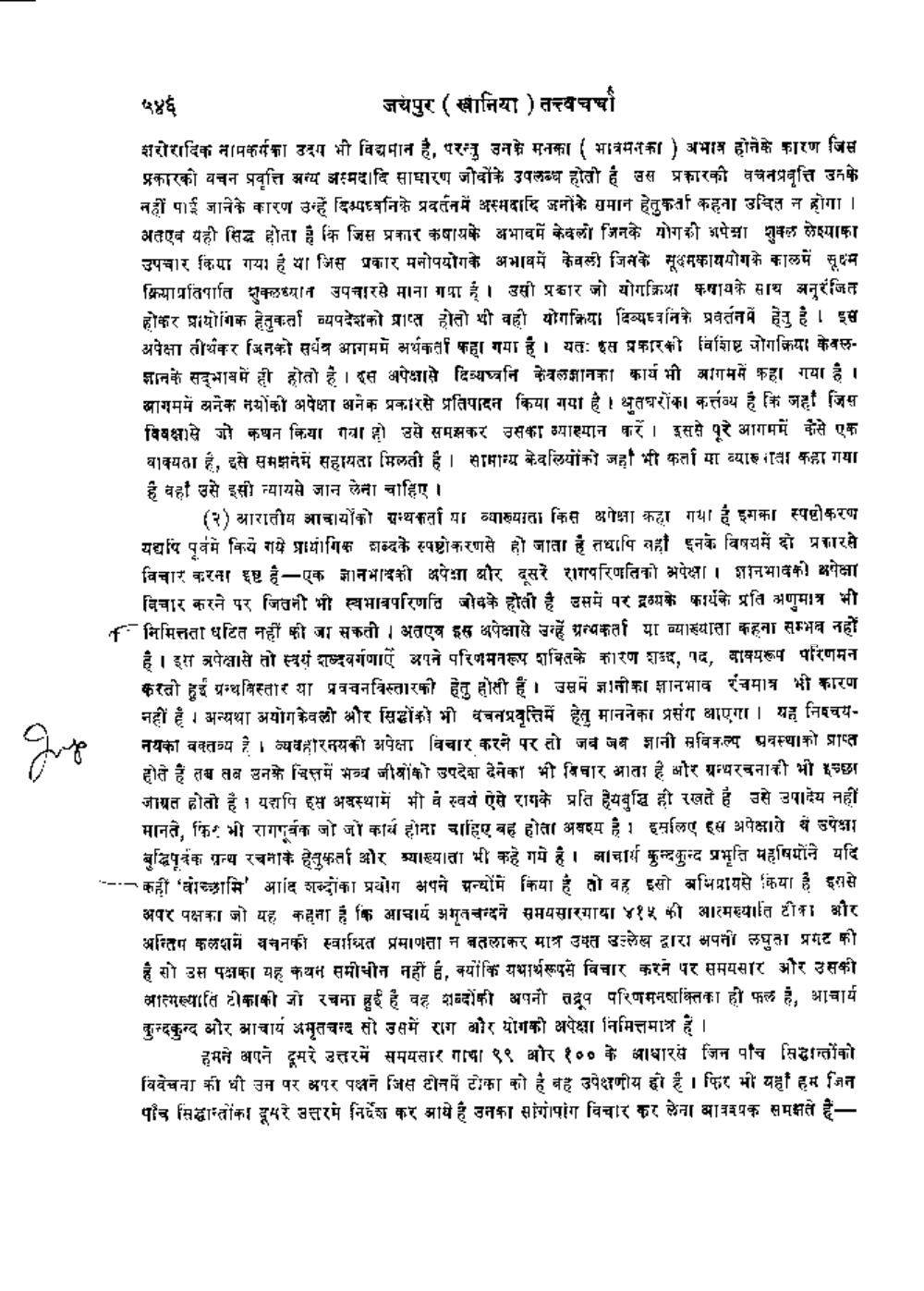________________
जयपुर (खानिया ) तत्त्वचर्चा शरोरादिक नामकर्म का उदय भी विद्यमान है, परन्तु उनके मनका { भावमनका ) अभाव होने के कारण जिस प्रकारको वचन प्रवृत्ति अन्य अस्मदादि साधारण जीवोंके उपलब्ध होती है उस प्रकारको वचनप्रवृत्ति उनके नहीं पाई जाने के कारण उन्हें दिपध्वनिके प्रवर्तन में अस्मदादि जनों के समान हेतुका कहना उचित न होगा । अतएव यही सिद्ध होता है कि जिस प्रकार कषायके अभाव में केवलो जिनके योगकी अपेमा शुक्ल लेश्याका उपचार किया गया है या जिस प्रकार मनोपयोगके अभावमें केवली जिनके सूदमकाययोगके काल में सूक्ष्म क्रियाप्रतिपाति शुक्ल ध्यान उपचारसे माना गया है। उसी प्रकार जो योगक्रिया पायके साथ अनुरंजित होकर प्रायोगिक हेतृकों व्यपदेशको प्राप्त होतो थी वही योगक्रिया दिव्यध्वनिके प्रवर्तन हेतु है। इस अपेक्षा तीर्थकर जिनको सर्वत्र आगमम अर्थका कहा गया है। यतः इस प्रकारको विशिष्ट जोगक्रिया केवलज्ञान के सद्भाव में ही होती है । इस अपेक्षासे दियध्वनि केवलज्ञानका कार्य भी आगममें कहा गया है। आगममें अनेक नयों की अपेक्षा अनेक प्रकारसे प्रतिपादन किया गया है। श्रुतघरोंका कर्तव्य है कि जहां जिस विवक्षासे जो कथन किया गया हो उसे समझकर उसका व्याख्यान करें। इससे पूरे आगममें कैसे एक वाक्यता है, इसे समझने में सहायता मिलती है। सामान्य केवलियोंको जहाँ भी कर्ता या ब्याावा कहा गया है वहाँ उसे इसी न्यायसे जान लेना चाहिए।
(२) आरातीय आचायौंको सन्थकर्ता या व्याख्याता किस अपेक्षा कहा गया है इसका स्पष्टीकरण यद्यपि पूर्वमें किये गये प्रायोगिक छाब्दके स्पष्टीकरणसे हो जाता है तथापि वहाँ इनके विषय में दो प्रकारसे विचार करना इष्ट है-एक ज्ञानभादकी अपेक्षा और दूसरे रागपरिणतिको अपेक्षा । शानभावको अपेक्षा
विचार करने पर जितनी भी स्वभावपरिणति जोदके होती है उसमें पर द्रव्यके कार्यके प्रति अणुमात्र भी f निमित्तता धटित नहीं की जा सकती। अतएव इस अपेक्षासे उन्हें अन्यकर्ता या व्याख्याता कहना सम्भव नहीं
है। इस अपेक्षासे तो स्वयं शब्दवर्गणाएं अपने परिणमनरूप शक्लिके कारण शब्द, पद, वाक्यरूप परिणमन करती हुई ग्रन्थविस्तार या प्रवचन विस्तारको हेतु होती है। उस में ज्ञानी का शानभाव रंचमात्र भी कारण नहीं है । अन्यथा अयोग केवली और सिद्धोंको भी वचनप्रवृत्तिमें हेतु माननेका प्रसंग आएगा । यह निश्चयनयका वक्तव्य है । व्यवहारमयकी अपेक्षा विचार करने पर तो जब जब ज्ञानी सबिकल्प अवस्थाको प्राप्त होते हैं तब तब उनके चिप्समें भव्य जीवों को उपदेश देने का भी विचार आता है और ग्रन्धरचनाकी भी इच्छा जाग्रत होतो है । यद्यपि इस अवस्थामें भी वे स्वयं ऐसे रागके प्रति हेयबुद्धि ही रखते है उसे उपादेय नहीं मानते, फिर भी रागगर्वक जो जो कार्य होना चाहिए बह होता अवश्य है। इसलिए इस अपेक्षारो ये उपेक्षा
मक ग्रन्थ रचनाके हेलका और श्याख्याता भी कहे गये है। प्राचार्य कून्द कन्द प्रति महषिमोंने यदि --'- कहीं 'वाच्छामि' आदि शब्दोंका प्रयोग अपने अन्थों में किया है तो वह इसो अभिप्रायसे किया है इससे
अपर पक्षका जो यह कहना है कि आचार्य अमृतचन्दने समयसारयाया ४१५ की आत्मख्याति टीका और अन्तिम कलशमें बचनकी स्वाचित प्रमाणता म बतलाकर मात्र उक्त उल्लेख द्वारा अपनी लघुता प्रगट की है सो उस पक्षका यह कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि यथार्थ रूपसे विचार करने पर समयसार और उसकी
आत्मख्याति टीकाकी जो रचना हुई है वह शब्दोंकी अपनी तद्रूप परिणमनशक्तिका ही फल है, आचार्य कुन्दकुन्द और आचार्य अमृतचन्द सो उसमें राग और योगको अपेक्षा निमित्तमात्र है।
हमने अपने दूसरे उत्तरमें समयसार गाथा ९९ और १०० के आधारसे जिन पांच सिद्धान्तोंको विवेचना की धी उन पर अपर पक्षने जिस टोन में टोका को है बह उपेक्षणीय हो है । फिर भी यहाँ हम जिन पाँच सिद्धान्तोंका दूसरे उत्तरम निर्देश कर आये हैं उनका सांगोपांग विचार कर लेना बावश्यक समझते हैं