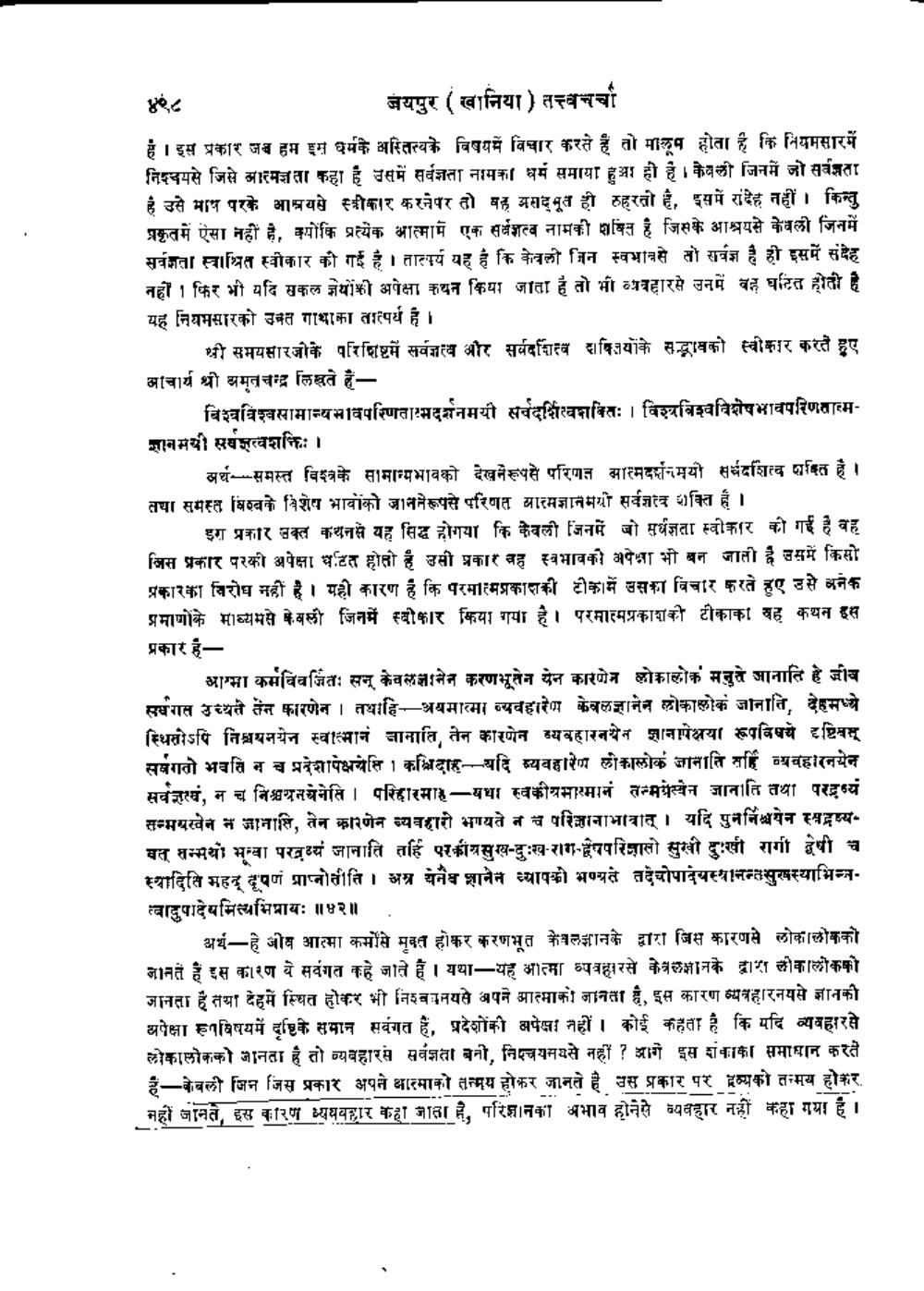________________
૮
जयपुर (खानिया) व चर्चा
है । इस प्रकार जब हम इस धर्म के अस्तित्वके विषय में विचार करते हैं तो मालूम होता है कि नियमसार में faraसे जिसे आत्मज्ञता कहा है उसमें सर्वज्ञता नामका धर्म समाया हुआ ही है। केवली जिनमें जो सर्वज्ञता है उसे मात्र परके आश्रयसे स्वीकार करनेपर तो वह असद्द्भूत ही ठहरती है, इसमें संदेह नहीं । किन्तु प्रकृत में ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक आत्मामें एक सर्वज्ञत्व नामकी शक्ति है जिसके आश्रयसे केवली जिनमें सर्वज्ञता स्वाश्रित स्वीकार की गई है। तात्पर्य यह है कि केवली जिन स्वभाव से तो सर्वज्ञ है ही इसमें संदेह नहीं । फिर भी यदि सकल ज्ञेयोंकी अपेक्षा कथन किया जाता है तो भी व्यवहारसे उनमें वह घटित होती है। यह नियमसारको उक्त गाथाका तात्पर्य है ।
श्री समयसार जोके परिशिष्ट में सर्वज्ञत्य और सर्वदशित्व दाजियोंके सद्भावको स्वीकार करते हुए आचार्य श्री अमृतचन्द्र लिखते हैं
विश्वविश्व सामान्यस विपरिणतारमदर्शनमयी सर्वदर्शिवशक्तिः । विश्वविश्व विशेष भावपरिणतात्मज्ञानमयी सर्वत्वशक्तिः ।
अर्थ- समस्त विश्वके सामान्यभाव को देखने रूपसे परिणत आत्मदर्शनमयो सर्वदशित्व शक्ति है । तथा समस्त विश्व के विशेष भावोंको जाननेरूपसे परिणत बात्मज्ञानमग्री सर्वज्ञत्व शक्ति हुँ ।
इस प्रकार उक्त कथनसे यह सिद्ध होगया कि केवली जिनमें जो सर्वज्ञता स्वीकार को गई है वह जिस प्रकार परकी अपेक्षा घटित होती है उसी प्रकार वह स्वभावको अपेक्षा भी बन जाती है उसमें किसो प्रकारका विरोध नहीं है। यही कारण है कि परमात्मप्रकाशकी टीका में उसका विचार करते हुए उसे अनेक प्रमाणोंके माध्यम से केवली जिनमें स्वीकार किया गया है। परमात्मप्रकाशकी टीकाका यह कथन इस प्रकार है—
आमा कर्मविवर्जितः सन् केवलज्ञानेन करणभूतेन येन कारणेन लोकालोकं मनुते जानाति है जीव सर्वगत उच्यते तेन कारणेन । तथाहि श्रयमात्मा व्यवहारेण केवलज्ञानेन लोकालोकं जानाति, देहमध्ये स्थितोऽपि निश्चयनयेन स्वात्मानं जानाति तेन कारणेन व्यवहारनयेन ज्ञानापेक्षया रूपविषये दृष्टिवस् सर्वगतो भवति न च प्रदेशापेक्षयेति । कचिदाह यदि व्यवहारेण लोकालोकं जानाति सहि व्यवहारनयेन सर्वज्ञत्वं न च निश्रयन येनेति । परिहारमाह-यथा स्वकीयमात्मानं तन्ममेत्येन जानाति तथा परद्रव्यं सम्मयखेन न जानाति, तेन कारणेन व्यवहारो भग्यते न च परिज्ञानाभावात् । यदि पुनर्निश्चयेन स्त्रद्रष्यवत सन्मयो भूत्वा परनुव्यं जानाति तर्हि परकीय सुख-दुःख-राग-द्वेषपरिज्ञालो सुखी दुःखी राग द्वेषी च स्वादिति महद् दूषणं प्राप्नोतीति । अत्र येनैव ज्ञानेन व्यापकी भव्यते तदेयोपादेयस्यानन्तसुखस्याभिन्नत्वादुपादेयमित्यभिप्रायः ॥४२॥
अर्थ- हे जीव आत्मा कर्मोंसे मृक्त होकर करणभूत केवलज्ञानके द्वारा जिस कारण से लोकालोकको जानते हैं इस कारण वे सवंगत कहे जाते हैं । यथा - यह आत्मा व्यवहारसे केवलज्ञानके द्वारा लोकालोकको जानता है तथा देह में स्थित होकर भी निश्चयसे अपने आत्माको जानता है, इस कारण व्यवहारनयसे ज्ञानकी अपेक्षा विषय दृष्टिके समान सर्वगत हैं, प्रदेशोंकी अपेक्षा नहीं। कोई कहता है कि यदि व्यवहार से लोकालोकको जानता है तो व्यवहारस सर्वज्ञता बनी, निश्चयमय से नहीं ? आगे इस शंकाका समाधान करते हैं - केबली जिन जिस प्रकार अपने आत्माको तन्मय होकर जानते है उस प्रकार पर द्रव्यको तन्मय होकर नहीं जानते, इस कारण ध्ययवहार कहा जाता है, परिज्ञानका अभाव होने से व्यवहार नहीं कहा गया है ।