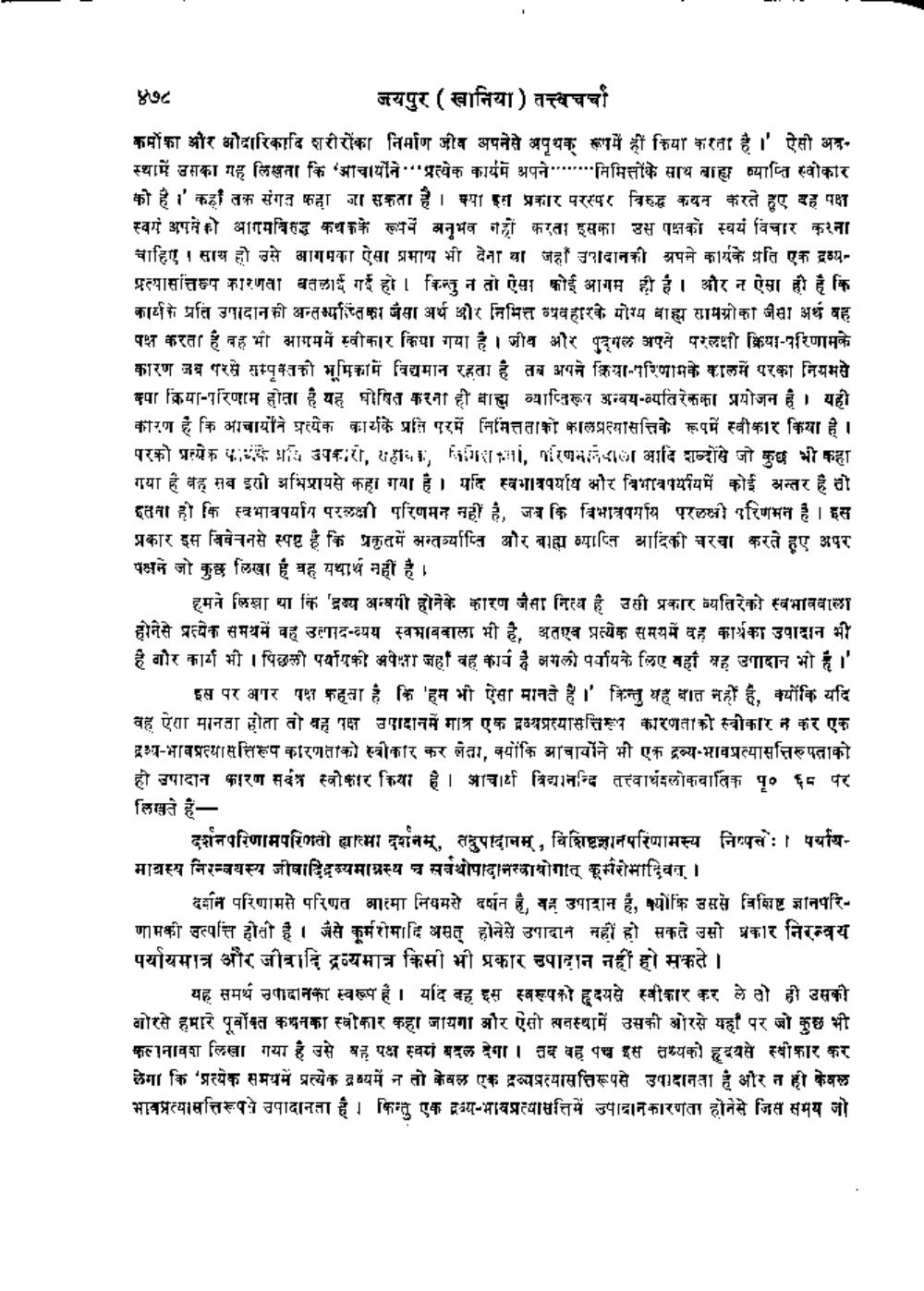________________
૭૮
जयपुर (खानिया) तत्त्वचर्चा
कमोंका और औदारिकादि शरीरोंका निर्माण जीव अपने से अपृथक् रूपमें हीं किया करता है। ऐसी अ स्था में उसका यह लिखना कि 'आचार्योंने प्रत्येक कार्यमे अपने निमित्तों के साथ बाह्य व्याप्ति स्वीकार को है ।' कहाँ तक संगत कहा जा सकता है। क्या इस प्रकार परस्पर विरुद्ध कथन करते हुए वह पक्ष स्वयं अपने को आगमविरुद्ध कथक के रूपमें अनुभव नहीं करता इसका उस पक्ष को स्वयं विचार करना चाहिए। साथ हो उसे आगमका ऐसा प्रभाग भी देना या जहाँ उरादानकी अपने कार्यके प्रति एक द्रव्यप्रत्यासत्तिरूप कारणता बतलाई गई हो। किन्तु न तो ऐसा कोई आगम ही है । और न ऐसा हो है कि कार्य के प्रति उपादान की अन्तप्तिका जैसा अर्थ और निमित्त व्यवहारके योग्य बाह्य सामग्रीका जैसा अर्थ वह पक्ष करता है वह भी आगम में स्वीकार किया गया है। जीव और पुद्गल अपने परलक्षी क्रिया परिणामके कारण जब पर सम्पृक्तको भूमिका में विद्यमान रहता है तब अपने क्रिया परिणाम के कालमें परका नियमसे क्या क्रिया-परिणाम होता है यह घोषित करना ही बाह्य व्याप्तिरूप अन्वयव्यतिरेकका प्रयोजन है । यही कारण है कि आचार्यनेि प्रत्येक कार्यके प्रति परमें निमित्तताको कालप्रत्यासत्तिके रूपमें स्वीकार किया है । परको प्रत्येक उपकारी, सहायक किसिम, रिमाल आदि शब्दोंसे जो कुछ भी कहा गया है वह सब इसी अभिप्रायसे कहा गया है। यदि स्वभात्रपर्याय और विभात्रपर्याय में कोई अन्तर है तो इतना ही कि स्वभाव पर्याय परलक्षी परिणमन नहीं है, जब कि विभात्रपर्याय परलक्षी परिणमन है । इस प्रकार इस विवेचनसे स्पष्ट है कि प्रकृत में अन्तर्व्याप्ति और बाह्य व्याप्ति यादिकी चरचा करते हुए अपर पक्षने जो कुछ लिखा है वह यथार्थ नहीं है ।
हमने लिखा था कि 'द्रव्य अन्वयी होनेके कारण जैसा नित्य है उसी प्रकार व्यतिरेको स्वभाववाला होनेसे प्रत्येक समय में वह उत्पाद व्यय स्वभाववाला भी है, अतएव प्रत्येक समय में वह कार्यका उपादान भी है गौर कार्य भी । पिछली पर्यायको अपेक्षा जहाँ वह कार्य है अगलो पर्यायके लिए वहाँ वह उपादान भी है।'
इस पर अगर पक्ष कहता है कि हम भी ऐसा मानते हैं । किन्तु यह बात नहीं है, क्योंकि यदि वह ऐसा मानता होता तो वह पक्ष उपादानमें मात्र एक द्रव्यप्रत्यासत्तिरूप कारणताको स्वीकार न कर एक द्रश्य भावप्रत्यासत्तिरूप कारणताको स्वीकार कर लेता, क्योंकि आचार्योंने भी एक द्रव्य भावप्रत्यासत्तिरूपताको ही उपादान कारण सर्वत्र स्वीकार किया है। आचार्य विद्यानन्दितत्त्वार्थवलोकवालिक पृ० ६८ पर लिखते हैं
दर्शन परिणामपरिगतो ह्यात्मा दर्शनम्, तदुपादानम्, विशिष्टज्ञान परिणामस्य निष्पतः । पर्यायमात्रस्य निरन्वयस्य जीवादिद्रव्यमानस्य च सर्वथोपादानत्वायोगात् कूरोमादिवत ।
दर्शन परिणाम से परिणत आत्मा नियमसे दर्शन है, यह उपादान है, क्योंकि उससे विशिष्ट ज्ञानपरिणामकी उत्पत्ति होती है । जैसे कूर्ममादि असत् होनेसे उपादान नहीं हो सकते उसी प्रकार निरन्वय पर्यायमात्र और जीवादि द्रव्यमात्र किसी भी प्रकार उपादान नहीं हो सकते ।
यह समर्थ उपादानका स्वरूप हैं । यदि वह इस स्वरूपको हृदयसे स्वीकार कर ले तो ही उसकी ओरसे हमारे पूर्वोक्त कथनका स्वीकार कहा जायगा और ऐसी व्यवस्था में उसकी ओरसे यहाँ पर जो कुछ भी कल्पनावश लिखा गया है उसे वह पक्ष स्वयं बदल देगा । तब वह पच इस तथ्यको हृदयसे स्वीकार कर लेगा कि 'प्रत्येक समय में प्रत्येक द्रव्यमें न तो केवल एक द्रव्यप्रत्यासत्तिरूपसे उपादानता है और न ही केवल भावप्रत्यासत्तिरूप उपादानता है । किन्तु एक द्रव्य भावप्रत्यासत्ति में उपादानकारणता होनेसे जिस समय जो