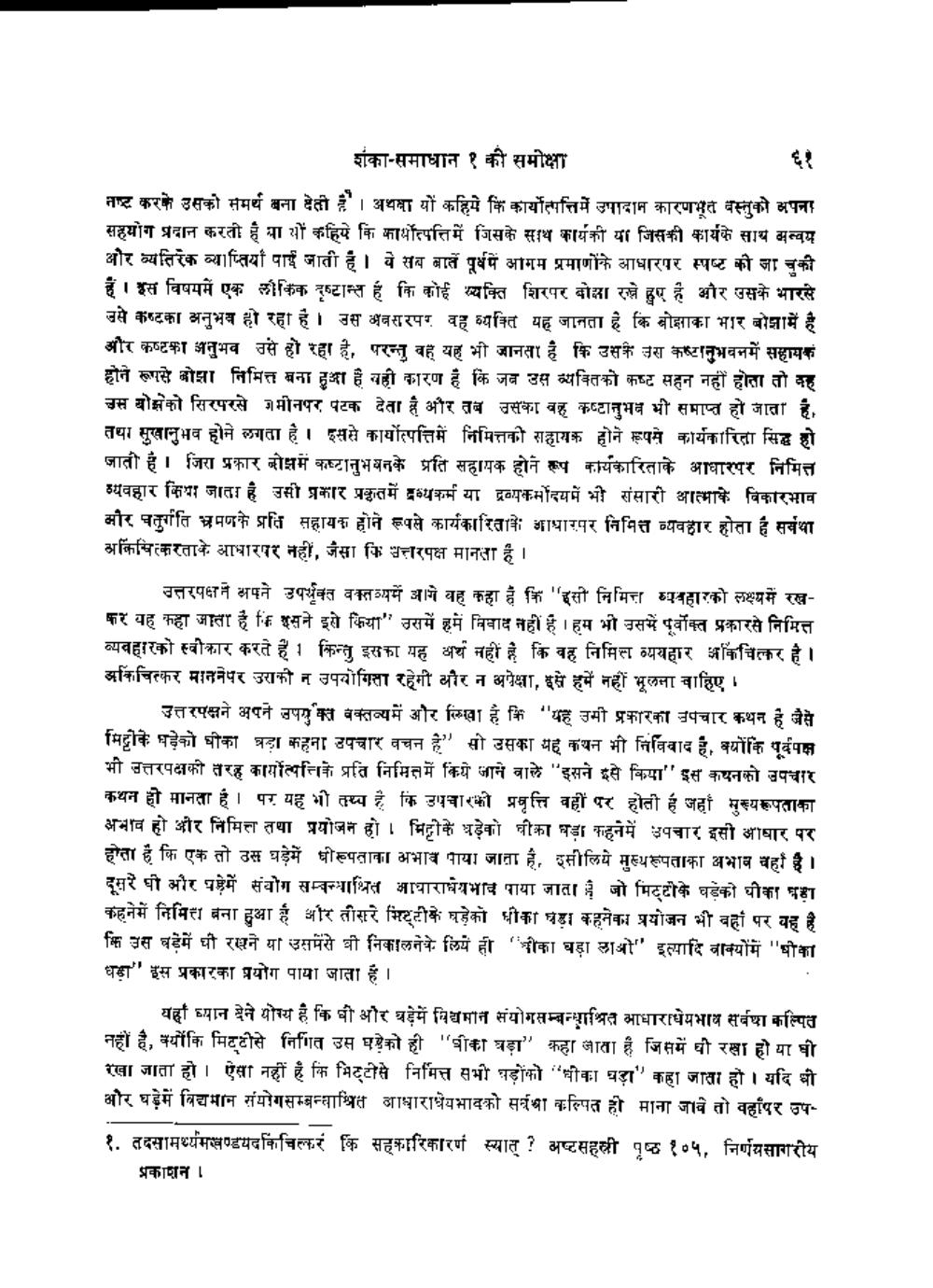________________
शंका-समाधान १ की समीक्षा नष्ट करके उसको समर्थ बना देती है । अथवा यो कहिये कि कार्योत्पत्तिमें उपादाम कारणभूत बस्तुको अपना सहयोग प्रदान करती है या यों कहिये कि कार्योत्पत्तिमें जिसके साथ कार्यकी या जिसकी कार्यके साथ अन्वय
और व्यतिरेक व्याप्तियाँ पाई जाती है। वे सब बातें पूर्व में आमम प्रमाणोंके आधारपर स्पष्ट की जा चुकी हैं। इस विषय में एक लौकिक दष्टान्त है कि कोई व्यक्ति शिरपर बोझा रख्ने हुए है और उसके भारसे
| कष्टका अनुभव हो रहा है। उस अवसरपर वह व्यक्ति यह जानता है कि बोझाका भार बोशामें है और कष्टका अनुभव उसे हो रहा है, परन्तु वह यह भी जानता है कि उसके उस कष्टानुभवनमें सहायक होने रूपसे बोझा निमित्त बना हुआ है वही कारण है कि जब उस व्यक्तिको कष्ट सहन नहीं होता तो वह उस बोझेको सिरपरसे जमीनपर पटक देता है और तब उसका वह कष्टानुभव भी समाप्त हो जाता है, तथा सुखानुभव होने लगता है। इससे कार्योत्पत्तिमें निमित्तकी सहायक होने रूपसे कार्यकारिता सिद्ध हो जाती है। जिरा प्रकार नोझम कष्टानुभवनके प्रति सहायक होने रूप कार्यकारिताके आधारपर निमित्त व्यवहार किया जाता है उसी प्रकार प्रकृतमें द्रव्यकर्म या द्रव्यकर्मोदय में भी संसारी आत्माके विकारभाव और चतुर्गति भ्रमणके प्रति सहायक होने रूपसे कार्यकारिताके आधारपर निमित्त व्यवहार होता है सर्वथा अकिंचित्करताके आधारपर नहीं, जैसा कि उत्तरपक्ष मानता है।
उत्तरपक्षने अपने उपर्युक्त वक्तव्यमें आगे वह कहा है कि "इसी निमित्त व्यवहारको लक्ष्यमें रखकर वह कहा जाता है कि इसने इसे किया" उसमें हमें विवाद नहीं है। हम भी उसमें पूर्वोक्त प्रकारसे निमित्त व्यवहारको स्वीकार करते है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह निमित्त व्यवहार अकिचित्कर है। अकिंचित्कर माननेपर उराकी न उपयोगिता रहेगी और न अपेक्षा, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए।
उत्तरपसने अपने उपर्य क्त वक्तव्य में और लिखा है कि "यह जमी प्रकारका उपचार कथन है जैसे मिट्टीके घड़ेको घीका बड़ा कहना उपचार वचन है" सो उसका यह कयन भी निविवाद है, क्योंकि पूर्वपक्ष भी उत्तरपक्षकी तरह कार्योत्पत्तिके प्रति निमित में किये जाने वाले "इसने इसे किया"इस कपनको उपचार कथन हो मानता है। पर यह भी तथ्य है कि उपचारको प्रवृत्ति वहीं पर होती है जहाँ मुख्यरूपताका अभाव हो और निमित्त तथा प्रयोजन हो । मिट्टोके धड़ेको घीका घड़ा कहनमें उपचार इसी आधार पर होता है कि एक तो उस घड़ेमें धीरूपताका अभाव पाया जाता है, इसीलिये मुख्यरूपताका अभाव वहाँ है। दूसरे घी और पड़े में संयोग सम्बन्धाश्रित आचाराधेयभाव पाया जाता है जो मिट्टीके घड़ेको घीका पहा कहने में निमित्त बना हुआ है और तीसरे मिट्टीके घड़ेको धीका घडा कहनेका प्रयोजन भी वहां पर यह है कि उस बडेमें घी रखने या उसमसे बी निकालनेके लिये ही चीका घड़ा लाओ" इत्यादि वाक्योंमें "धोका धड़ा" इस प्रकारका प्रयोग पाया जाता है।
यहाँ ध्यान देने योग्य है कि घी और बड़ेमें विद्यमान संयोगसम्बन्धश्रित आधाराधेयभाव सर्वथा कल्पित नहीं है, क्योंकि मिट्टीसे निर्मित उस घटेको ही "पीका घड़ा' कहा जाता है जिसमें घी रखा हो या घी रखा जाता हो। ऐसा नहीं है कि मिट्टीसे निमित्त सभी घड़ोंको “घीका घा' कहा जाता हो। यदि धी और घडे में विद्यमान संयोगसम्बन्धाश्रित बाधाराधेयभावको सर्वथा कल्पित ही माना जावे तो वहाँपर उप१. तदसामर्थ्यमखण्डयदकिंचिकर कि सहकारिकारणं स्यात् ? अष्टसहस्री पृष्ठ १०५, निर्णयसागरीय
प्रकाशन ।