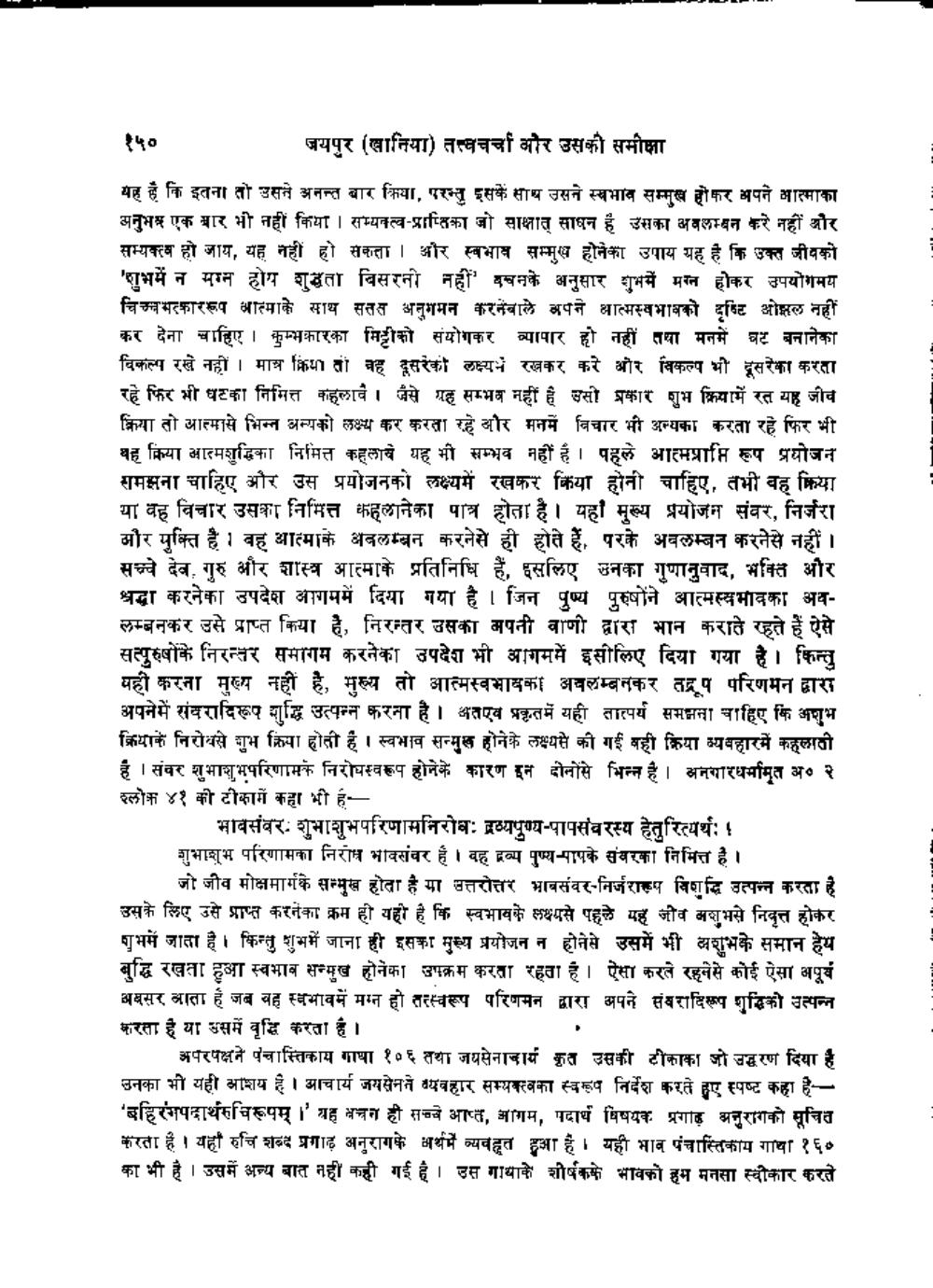________________
१५०
जयपुर (खानिया) तस्वचर्चा और उसकी समीक्षा
यह है कि इतना तो उसने अनन्त बार किया, परन्तु इसके साथ उसने स्वभाव सम्मुख होकर अपने भात्माका अनुभव एक बार भी नहीं किया। सम्यक्त्व-प्राप्तिका जो साक्षात् साधन है उसका अवलम्बन करे नहीं और सम्यक्त्व हो जाय, यह नहीं हो सकता । और स्वभाव सम्मुख होने का उपाय यह है कि उक्त जीवको 'शुभमें न मग्म होय शुद्धता बिसरनी नहीं' वचनके अनुसार शुभमें मग्न होकर उपयोगमय चिकनभत्काररूप आत्माके साथ सत्तस अनुगमन करनेवाले अपने बात्मस्वभावको दृष्टि ओझल नहीं कर देना चाहिए। कुम्भकारका मिट्टीको संयोगकर व्यापार हो नहीं तथा मनमें घट बनानेका विकल्प रखे नहीं । मात्र किया तो वह दूसरेको लक्ष्य रखकर करे और विकल्प भी दूसरेका करता रहे फिर भी घटका निमित्त कहलावै । जैसे यह सम्भव नहीं है उसी प्रकार शुभ क्रिया में रत यष्ठ जीव क्रिया तो आत्मासे भिन्न अन्यको लक्ष्य कर करता रहे और मनमें विचार भी अन्यका करता रहे फिर भी यह क्रिया आत्मशुद्धिका निमित्त कलावे यह भी सम्भव नहीं है। पहले आत्मप्राप्ति रूप प्रयोजन समझना चाहिए और उस प्रयोजनको लक्ष्यमें रखकर किया होनी चाहिए, तभी वह क्रिया या वह विचार उसका निमित्त कहलानेका पात्र होता है। यहाँ मुख्य प्रयोजन संवर, निर्जरा और मुक्ति है । वह आत्माके अवलम्बन करनेसे ही होते हैं, परके अवलम्बन करनेसे नहीं। सच्चे देव, गुरु और शास्त्र आत्माके प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनका गुणानुवाद, भक्ति और श्रद्धा करनेका उपदेश आगममें दिया गया है । जिन पुण्य पुरुषोंने आत्मस्वभावका अवलम्बनकर उसे प्राप्त किया है, निरन्तर उसका अपनी वाणी द्वारा भान कराते रहते हैं ऐसे सत्पुरुषों के निरन्तर समागम करनेका उपदेश भी आगममें इसीलिए दिया गया है। किन्तु यही करना मुख्य नहीं है, मुख्य तो आत्मस्वभावका अवलम्बनकर तद्रूप परिणमन द्वारा अपनेमें संवरादिरूप शुद्धि उत्पन्न करना है। अतएव प्रकृतमें यही तात्पर्य समझना चाहिए कि अशुभ क्रियाक निरोबसे शुभ क्रिया होती है । स्वभाव सन्मुख होनेके लक्ष्यसे की गई वही क्रिया व्यवहारमें कहलाती है । संवर शुभाशुभपरिणाम निरोधस्वरूप होनेके कारण इन दोनोंसे भिन्न है। अनगारधर्मामृत अ० २ श्लोक ४१ की टीकामें कहा भी है
भावसंवरः शुभाशुभपरिणामनिरोवः द्रव्यपुग्य-पापसंवरस्य हेतुरित्यर्थः । शुभाशुभ परिणामका निराध भावसंवर है । वह द्रव्य पुण्य-पापके संवरका निमित्त है।
जो जीव मोक्षमार्गके सन्मुख होता है मा उत्तरोत्तर भावसंवर-निर्जरारूप विशुद्धि उत्पन्न करता है उसके लिए उसे प्राप्त करनेका क्रम ही यही है कि स्वभावके लक्ष्यसे पहले यह जीव अशुभसे निवृत्त होकर शुभमें जाता है। किन्तु शुभमें जाना ही इसका मुख्य प्रयोजन न होनेसे उसमें भी अशुभके समान हेय बुद्धि रखता हुआ स्वभाव सन्मुख होनेका उपक्रम करता रहता है। ऐसा करते रहने से कोई ऐसा अपूर्व अबसर आता है जब वह स्वभावमें मग्न हो तत्स्वरूप परिणमन द्वारा अपने संवरादिरूप शुद्धिको उत्पन्न करता है या उसमें वृद्धि करता है।
अपरपक्षने पंचास्तिकाय गाथा १०६ तथा जयसेनाचार्य कृत उसकी टीकाका जो उद्धरण दिया है उनका भी यही आशय है । आचार्य जयसेनने व्यवहार सम्यक्त्वका स्वरूप निर्देश करते हुए स्पष्ट कहा है'बहिरंगपदार्थरुचिरूपम् ।' यह वचन ही सच्चे आप्त, आगम, पदार्थ घिषयक प्रगाढ़ अनुरागको सूचित करता है । यहाँ रुचि शब्द प्रगाढ़ अनुरागके अर्थमें व्यवहृत हुआ है। यही भाव पंचास्तिकाय गाथा १६० का भी है। उसमें अन्य बात नहीं कही गई है। उस गाथाके शीर्षकके भावको हम मनसा स्वीकार करते