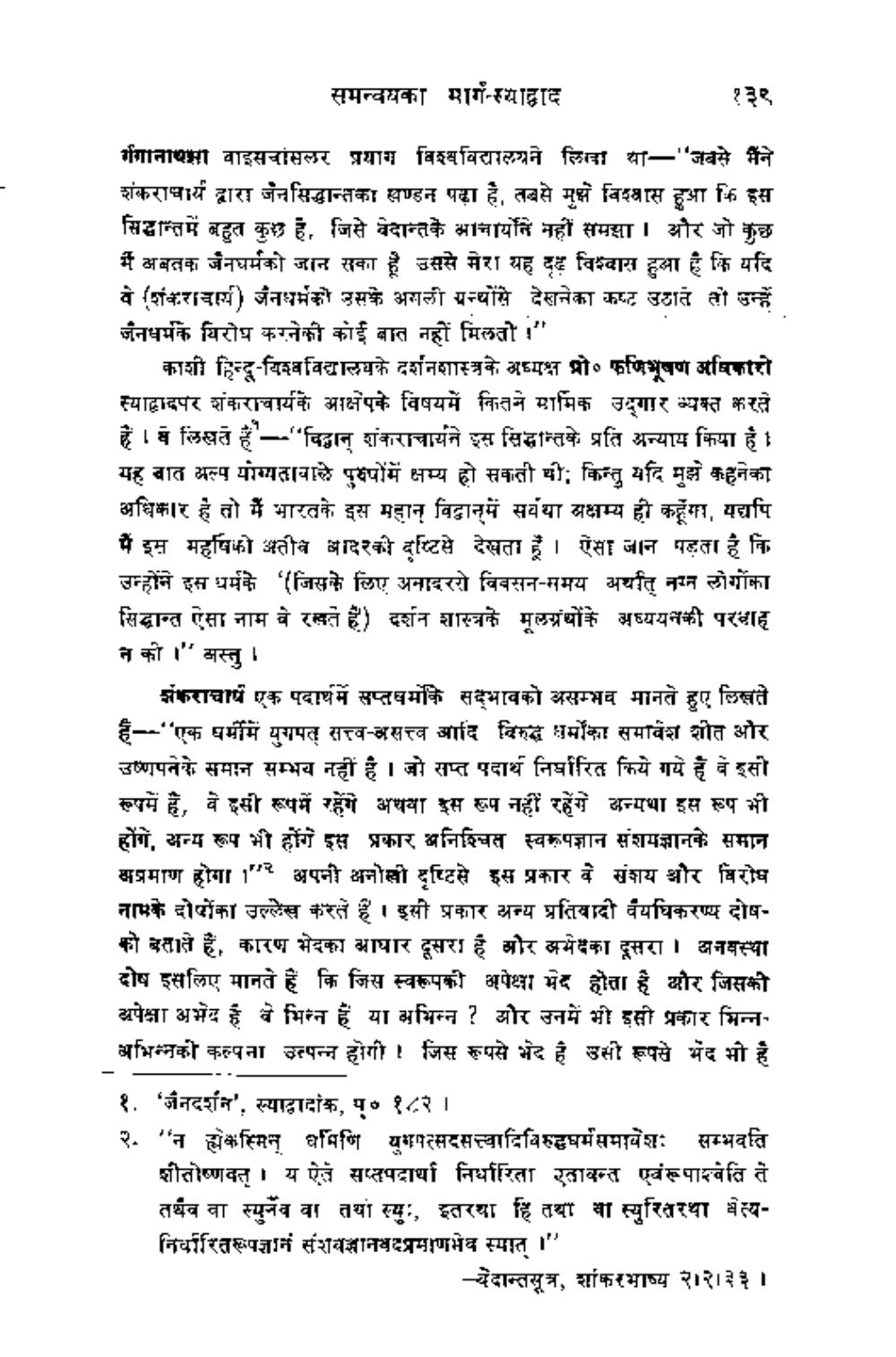________________
समन्वयका मार्ग-स्याद्वाद
१३२
गंगानाथझा वाइसचांसलर प्रयाग विश्वविद्यालय ने लिया था-"जबसे मैंने शंकराचार्य द्वारा जनसिद्धान्तका खण्डन पढ़ा है, तबसे मुझे विश्वास हुआ कि इस सिद्धान्त में बहुत कुछ है, जिसे वेदान्तके भाचार्योने नहीं समझा। और जो कुछ मैं अबतक जैनधर्मको जान सका हूँ उससे मेरा यह दृढ विश्वास हुआ है कि यदि वे शंकराचार्य) जनधर्मको उसके अगली ग्रन्थोंसे देखने का कष्ट उठाते तो उन्हें जनधर्मक विरोध करने की कोई बात नहीं मिलती।" __काशी हिन्दु-विश्वविद्यालयके दर्शनशास्त्रके अध्यक्ष प्रो० फणिभूषण अधिकारी स्याद्वादपर शंकराचार्य के आक्षेपके विषयमें नितिने मार्मिक उद्गार व्यक्त करते हैं । वे लिखते हैं'--"विद्वान् शंकराचार्य ने इस सिद्धान्तके प्रति अन्याय किया है। यह बात अल्प योग्यतावाले पुरूषोंमें क्षम्य हो सकती थी; किन्तु यदि मुझे कहनेका अधिकार है तो मैं भारतके इस महान विद्वान्में सर्वथा अक्षम्य ही कहूँगा, यद्यपि मैं इस महर्षिको अतीव आदरको दष्टिसे देखता हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने इस धर्मके (जिसके लिए अनादररो विवसन-ममय अर्थात् नग्न लोगोंका सिद्धान्त ऐसा नाम वे रखते है) दर्शन शास्त्रके मूलग्रंथों के अध्ययनकी परवाह न को ।” अस्तु ।
शंकराचार्य एक पदार्थ में सप्तषकि सद्भावको असम्भव मानते हुए लिखते है--"एक धम युगपत् सत्त्व-असत्त्व आदि विरुद्ध धर्मोंका समावेश शीत और उष्णपने के समान सम्भव नहीं है । जो सप्त पदार्थ निर्धारित किये गये है वे इसी रूपमें है, वे इसी रूपमें रहेंगे अथवा इस रूप नहीं रहेंगे अन्यथा इस रूप भी होंगे, अन्य रूप भी होंगे इस प्रकार अनिश्चित स्वरूपज्ञान संशयज्ञानके समान मप्रमाण होगा ।"२ अपनी अनोखी दृष्टि से इस प्रकार वे संशय और विरोध नामके दोपोंका उल्लेख करते हैं । इसी प्रकार अन्य प्रतिवादी वैयधिकरण्य दोषको बताते हैं, कारण भेदका आधार दूसरा है और अभेदका दूसरा । अनवस्था दोष इसलिए मानते हैं कि जिस स्वरूपको अपेक्षा भेद होता है और जिसकी अपेक्षा अभेद है वे भिन्न हैं या अभिन्न ? और उनमें भी इसी प्रकार भिन्नअभिन्नकी कल्पना उत्पन्न होगी। जिस रूपसे भेद है उसी रूपसे भेद भी है १. 'जैनदर्शन', स्याहादांक, प. १८२ । २. "न होकस्मिन् मिणि युगपरसदसत्त्वादिविरुद्धधर्मसमावेशः सम्भवति
शीतोष्णवत । य ऐले सप्तपदार्था निर्धारिता रतावन्त एवंरूपाश्चति ते तर्थव वा स्युव वा तथा स्युः, इतरया हि तथा वा स्युरितरथा धेत्यनिर्धारितरूपज्ञानं संशवज्ञानवप्रमाणभेव स्यात् ।"
-येदान्तसूत्र, किरभाष्य २१२।३३ ।