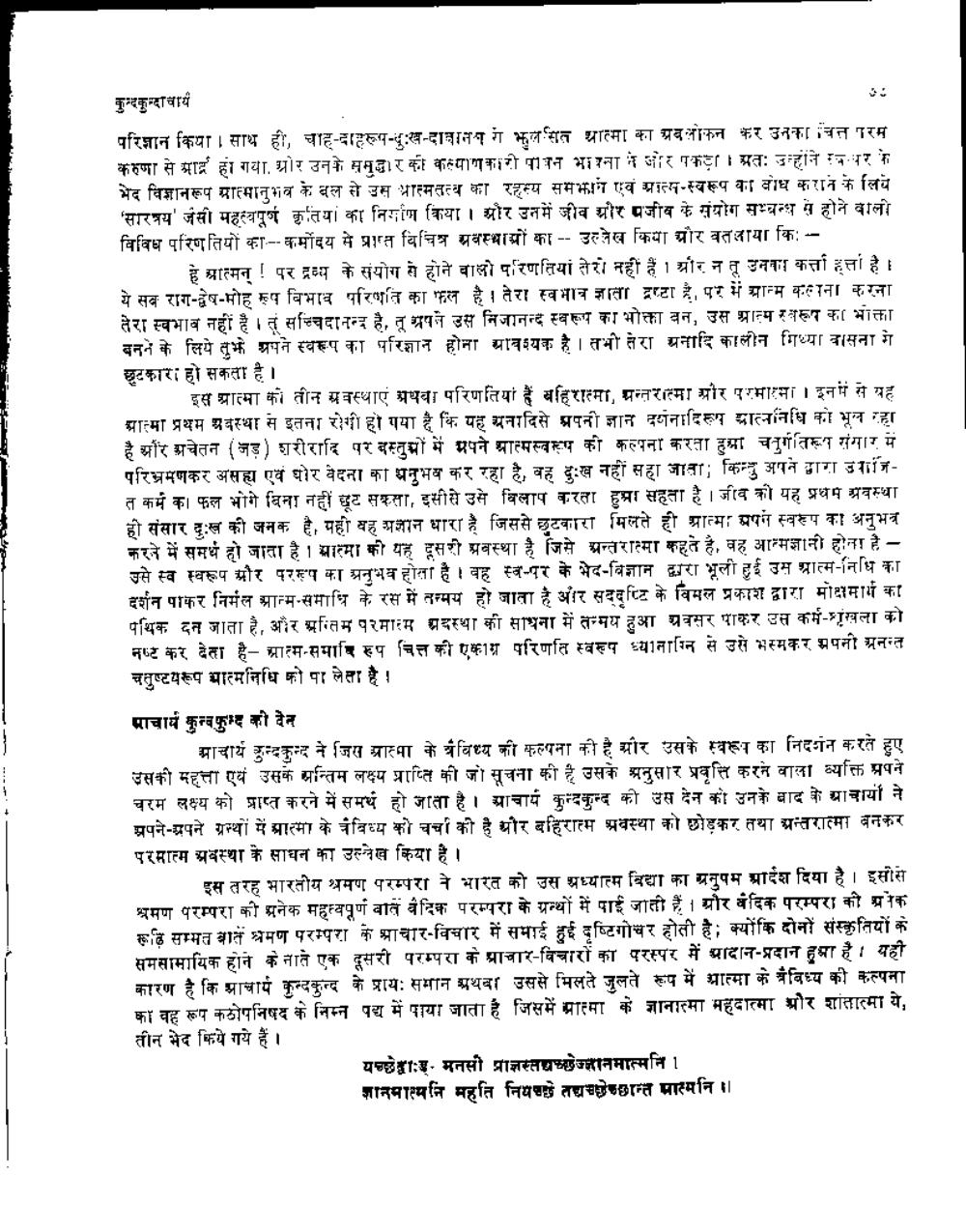________________
कुन्दकुन्दाचार्य
परिज्ञान किया। साथ ही, चाह-वाहरूप दु:ख-दावान से भुलसित श्रात्मा का अवलोकन कर उनका चित्त परम करुणा से माई हां गया. और उनके समुद्धार की कल्याणकारी पात्र भावना ने जोर पकड़ा। अतः उन्होंने स्वबर के भेद विज्ञानरूप ग्रात्मानुभव के बल से उस आत्मतत्व का रहस्य समझाने एवं आत्म-स्वरूप का बोध कराने के लिये 'सार' जैसी महत्वपूर्ण कृतियों का निर्माण किया । और उनमें जीव और बजीब के संयोग सम्बन्ध से होने वाली विविध परिणतियों का कर्मोदय से प्राप्त विचित्र अवस्थामों का उल्लेख किया और बतलाया कि
3
-
हे श्रात्मन् ! पर द्रव्य के संयोग से होने वाली परिणतियां तेरी नहीं हैं और न तू उनका कर्त्ता त्त है। ये सब राग-द्वेष-मोह रूप विभाव परिषति का फल है । तेरा स्वभाव ज्ञाता द्रष्टा है, पर में ग्रान्म कल्पना करना तेरा स्वभाव नहीं है। तूं सच्चिदानन्द है, तू अपने उस निजानन्द स्वरूप का भोक्ता वन, उस श्रात्म स्वरूप का भक्ता बनने के लिये तुझे अपने स्वरूप का परिज्ञान होना मावश्यक है। तभी तेरा अनादि कालीन मिथ्या वासना से छुटकारा हो सकता है ।
इस श्रात्मा को तीन यवस्थाएं अथवा परिणतियां हैं बहिरात्मा अन्तरात्मा और परमात्मा । इनमें से यह आत्मा प्रथम अवस्था से इतना रोगी हो गया है कि यह अनादिसे अपनी ज्ञान वर्णनादिरूप यानिधि को भूल रहा है और अचेतन (जड़) शरीरादि पर वस्तुनों में अपने श्रात्मस्वरूप की कल्पना करता हुआ चतुर्गतिरूप संसार में परिभ्रमणकर असह्य एवं घोर वेदना का अनुभव कर रहा है, वह दुःख नहीं सहा जाता; किन्तु अपने द्वारा नाजि त कर्म का फल भोगे बिना नहीं छूट सकता, इसीसे उसे विलाप करता हुआ सहता है। जीव की यह प्रथम अवस्था ही संसार दुःख की जनक है, यही वह अज्ञान धारा है जिससे छुटकारा मिलते ही श्रात्मा अपने स्वरूप का अनुभव करने में समर्थ हो जाता है । म्रात्मा की यह दूसरी अवस्था है जिसे अन्तरात्मा कहते है, वह आत्मज्ञानी होता हैउसे स्व स्वरूप और पररूप का अनुभव होता है। वह स्वपर के भेद - विज्ञान द्वारा भूली हुई उस श्रात्म-निधि का दर्शन पाकर निर्मल आत्म-समाधि के रस में तन्मय हो जाता है और सद्दृष्टि के विमल प्रकाश द्वारा मोक्षमार्ग का पथिक दन जाता है, और अतिम परमात्म अवस्था की साधना में तन्मय हुआ अवसर पाकर उस कर्म-श्रृंखला को नष्ट कर देता है- ग्रात्म-समाधि रूप चित्त की एकाग्र परिणति स्वरूप ध्याताग्नि से उसे भस्मकर अपनी अनन्त चतुष्टयरूप भ्रात्मनिधि को पा लेता है ।
-
प्राचार्य कुम्कुभ्द की देन
आचार्य कुन्दकुन्द ने जिस ग्रात्मा के वैविध्य की कल्पना की है और उसके स्वरूप का निदर्शन करते हुए उसकी महत्ता एवं उसके अन्तिम लक्ष्य प्राप्ति की जो सूचना की है उसके अनुसार प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। आचार्य कुन्दकुन्द की उस देन को उनके बाद के आचार्य ने अपने-अपने ग्रन्थों में आत्मा के चैविध्य को चर्चा की है और बहिरात्म अवस्था को छोड़कर तथा अन्तरात्मा बनकर परमात्म अवस्था के साधन का उल्लेख किया है।
यच्छेवाङ मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञानमात्मनि । ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेतचछेच्छान्त मात्मनि ॥
इस तरह भारतीय श्रमण परम्परा ने भारत को उस अध्यात्म विद्या का ग्रनुपम आदेश दिया है। इसीस श्रमण परम्परा की अनेक महत्वपूर्ण बातें वैदिक परम्परा के ग्रन्थों में पाई जाती हैं। और वैदिक परम्परा की अनेक रूढ़ि सम्मत बातें श्रमण परम्परा के आचार-विचार में समाई हुई दृष्टिगोचर होती है; क्योंकि दोनों संस्कृतियों के समसामायिक होने के नाते एक दूसरी परम्परा के श्राचार-विचारों का परस्पर में आदान-प्रदान हुआ है। यही कारण है कि श्राचार्य कुन्दकुन्द के प्रायः समान अथवा उससे मिलते जुलते रूप में आत्मा के वैविध्य की कल्पना का वह रूप कठोपनिषद के निम्न पद्य में पाया जाता है जिसमें ग्रात्मा के ज्ञानात्मा महदात्मा और शांतात्मा ये, तीन भेद किये गये हैं ।