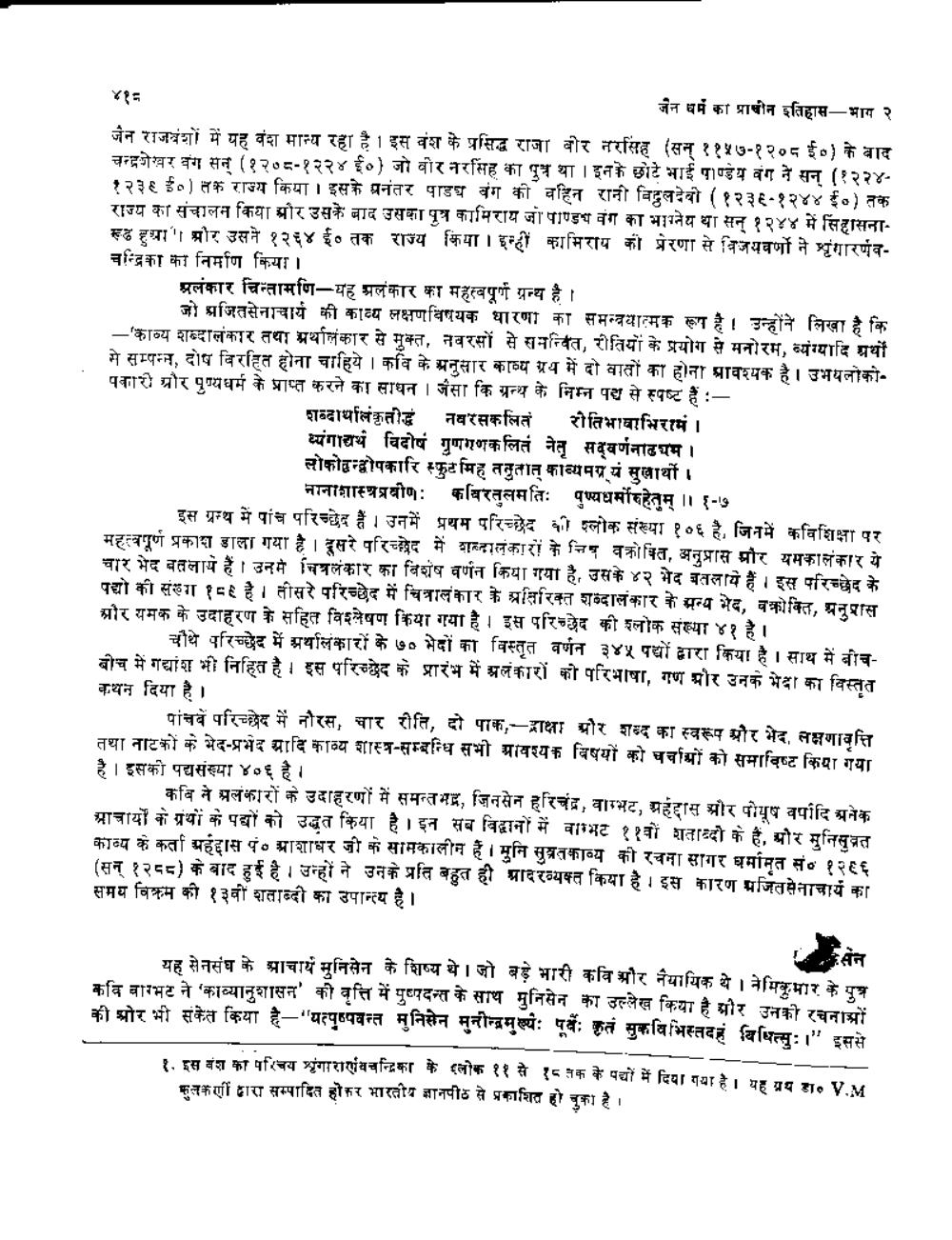________________
जैन धर्म का प्राचीन इतिहास भाग २
जैन राजवंशों में यह वंश मान्य रहा है। इस वंश के प्रसिद्ध राजा वीर नरसिंह (सन् १९५७-१२०८ ई.) के बाद चन्द्रशेखर वंग सन (१२०८-१२२४ ई०) जो वीर नरसिंह का पुत्र था । इनके छोटे भाई पाण्डेय वंग ने सन् (१२२४१२३६ ई0) तक राज्य किया। इसके प्रनंतर पाडय बंग की वहिन रानी बिगुलदेवी (१२३६.१२४४ ई.) तक राज्य का संचालन किया और उसके बाद उसका पुत्र कामिराय जो पाण्डव वंग का भाग्नेय था सन् १२४४ में सिंहासनारूढ ह्या । और उसने १२६४ ई. तक राज्य किया। इन्हीं कामिराय की प्रेरणा से विजयवों ने श्रृंगारर्णवचन्द्रिका का निर्माण किया।
अलंकार चिन्तामणि-यह अलंकार का महत्वपूर्ण ग्रन्थ है।
जो प्रजितसेनाचार्य की काव्य लक्षणविषयक धारणा का समन्वयात्मक रूप है। उन्होंने लिखा है कि -'काव्य शब्दालंकार तथा प्रर्थालंकार से मुक्त, नवरसों से समन्वित, रीतियों के प्रयोग से मनोरम, व्यंग्यादि प्रथों मे सम्पन्न, दोष विरहित होना चाहिये । कवि के अनुसार काव्य पथ में दो वातों का होना प्रावश्यक है। उभयलोकोपवारी प्रौर पुण्यधर्म के प्राप्त करने का साधन । जैसा कि ग्रन्थ के निम्न पत्र से स्पष्ट हैं :
शब्दार्थालंकृतीद्ध नवरसकलित रीतिभावाभिरामं । व्यंगारार्थ विदोष गुणगणक लित नेतृ सवर्णनाढयम । लोकोद्वन्द्वोपकारि स्फुट मिह तनुतात् काव्यमग्र यं सुखार्थो ।
नानाशास्त्रप्रवीण: कविरतुलमतिः पुण्यधर्मोकहेतुम् ।। ५-७ इस ग्रन्थ में पांच परिच्छेद हैं। उनमें प्रथम परिच्छेद की श्लोक संख्या १०६ है, जिनमें कविशिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। दूसरे परिच्छेद में बाब्दालंकारों के निष वक्रोक्ति, अनुप्रास मोर यमकालंकार ये चार भेद बतलाये हैं। उनमे चित्रलंकार का विशेष वर्णन किया गया है, उसके ४२ भेद बतलाये हैं । इस परिच्छेद के पद्यो की संख्या १८९ है। तीसरे परिच्छेद में चित्रालंकार के अतिरिक्त शब्दालंकार के अन्य भेद, वक्रोक्ति, अनुप्रास और यमक के उदाहरण के सहित विश्लेषण किया गया है। इस परिच्छेद की श्लोक संख्या ४१ है।
चौथे परिच्छेद में अलकारों के ७०भेदों का विस्तृत वर्णन ३४५ पद्यों द्वारा किया है। साथ में बीचबीच में गद्यांश भी निहित है। इस परिच्छेद के प्रारंभ में अलंकारों को परिभाषा, गण और उनके भेदा का विस्तत कथन दिया है।
पनि परिच्छेद में नौरस, चार रीति, दो पाक, द्राक्षा और शब्द का स्वरूप और भेद, लक्षगावृत्ति नया नाटकों के भेद-प्रभेद मादि काव्य शास्त्र-सम्बन्धि सभी प्रावश्यक विषयों को चर्चायों को समाविष्ट किया गया है। इसकी पद्यसंख्या ४०६ है।
कवि ने अलंकारों के उदाहरणों में समन्तभद्र, जिनसेन हरिचंद्र, वाग्भट, अहहास और पोयष वाटि अनेक प्राचार्यों के ग्रंथों के पद्यों को उद्धत किया है। इन सब विद्वानों में वाग्भट ११वौं शताब्दी के है और मनिसवत काव्य के कर्ता प्रहास पं० पाशाधर जी के सामकालीन हैं । मुनि सुव्रतकाव्य की रचना सागर धर्मामत सं० १२६६ (सन १२८८) के बाद हई है। उन्हों ने उनके प्रति बहुत ही प्रादरव्यक्त किया है। इस कारण प्रजितनाचा का समय विक्रम की १३वीं शताब्दी का उपान्त्य है।
यह सेनसंघ के प्राचार्य मुनिसेन के शिष्य थे। जो बड़े भारी कवि और नैयायिक थे। नेमिकमारपत्र कवि वाग्भट ने 'काव्यानुशासन' की वृत्ति में पुष्पदन्त के साथ मुनिसेन का उल्लेख किया है और उनको पता की ओर भी संकेत किया है-"यत्पुष्पवन्त मुनिसेन मुनीन्द्रमुख्यः पूर्वः कृतं सुकविभिस्तदहं विधिसः। इससे
इस वंश का परिचय श्रृंगारावचन्द्रिका के लोक ११ से १८तक के पद्यों में दिया गया है। यह प्रथाvv कुलकणी द्वारा सम्पादित हो कर भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो चुका है।