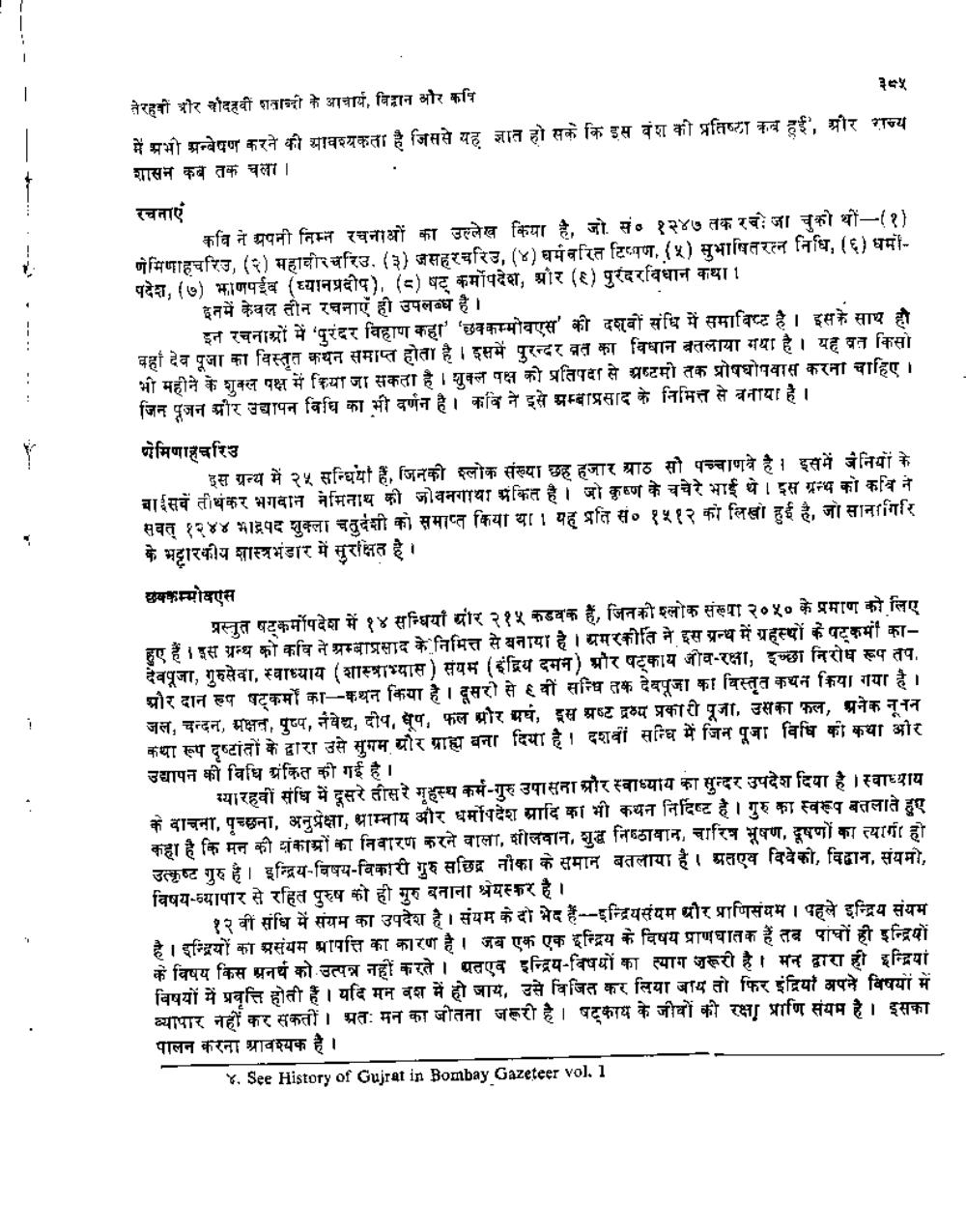________________
तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी के आचार्य, विद्वान और कवि में अभी अन्वेषण करने की मावश्यकता है जिससे यह ज्ञात हो सके कि इस वंश की प्रतिष्ठा कब हुई, और राज्य शासन कब तक चला। रचनाएं
कवि ने अपनी निम्न रचनाओं का उल्लेख किया है, जो. सं. १२४७ तक रवी जा चुकी थीं-(१) मिणाहचरिउ, (२) महावीर चरिउ. (३) जसहरचरिउ, (४) धर्मवरित टिप्पण, (५) सुभाषितरत्न निधि, (६) धर्मोंपदेश, (७) भाणपईव (ध्यानप्रदीप), (८) षट् कर्मोपदेश, और (३) पुरंदरविधान कथा ।
इनमें केवल तीन रचनाएं ही उपलब्ध है।
इन रचनाओं में प्रदर विहाण कहा' 'छक्कम्मोवएस' की दशबों संधि में समाविष्ट है। इसके साथ ही वहाँ देव पूजा का विस्तृत कथन समाप्त होता है। इसमें पुरन्दर व्रत का विधान बतलाया गया है। यह व्रत किसो भी महीने के शुक्ल पक्ष में किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष को प्रतिपदा से अष्टमी तक प्रोषधोपवास करना चाहिए। जिन पूजन और उद्यापन विधि का भी वर्णन है। कवि ने इसे अम्बाप्रसाद के निमित्त से बनाया है।
गेमिणाहचरिउ
इस ग्रन्य में २५ सन्धियाँ हैं, जिनकी श्लोक संख्या छह हजार पाठ सौ पच्चाणवे है। इसमें जैनियों के बाईसवें तीथंकर भगवान नेमिनाथ की जोवनगाथा अंकित है। जो कृष्ण के चचेरे भाई थे। इस ग्रन्थ को कवि ने सवत् १२४४ भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी को समाप्त किया था। यह प्रति सं० १५१२ को लिखी हुई है, जो सानागिरि के भट्टारकीय शास्त्रभंडार में सुरक्षित है।
छक्कम्मोवएस
प्रस्तुत षटकर्मोपदेश में १४ सन्धियाँ और २१५ कडवक हैं, जिनकी श्लोक संख्या २०५० के प्रमाण को लिए हुए हैं । इस ग्रन्ध को कवि ने अम्बाप्रसाद के निमित्त से बनाया है। अमरकीर्ति ने इस ग्रन्थ में ग्रहस्थों के पटकमी कादेवपूजा, गुरुसेवा, स्वाध्याय (शास्त्राभ्यास) संयम (इंद्रिय दमन) और षट्काय जीव-रक्षा, इच्छा निरोध रूप तप. और दान रूप षट्कर्मों का-कथन किया है । दूसरी सेवी सन्धि तक देवपूजा का विस्तृत कथन किया गया है। जल, चन्दन, मक्षन, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और सघं, इस प्रष्ट द्रव्य प्रकारी पूजा, उसका फल, अनेक ननन कथा रूप दृष्टांतों के द्वारा उसे सुगम यौर ग्राह्य बना दिया है। दशवों सन्धि में जिन पूजा विधि को कथा और उद्यापन की विधि अंकित की गई है।
ग्यारहवीं संधि में दूसरे तीसरे गृहस्थ कर्म-गुरु उपासना और स्वाध्याय का सुन्दर उपदेश दिया है । स्वाध्याय के वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, पाम्नाय और धर्मोपदेश आदि का भी कथन निर्दिष्ट है । गुरु का स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि मन की शंकानों का निवारण करने वाला, शीलवान, शुद्ध निष्ठावान, चारित्र भूषण, दूषणों का त्यागी हो उत्कृष्ट गुरु है। इन्द्रिय-विषय-विकारी गुरु सछिद्र नौका के समान बतलाया है। प्रतएव विवेको, विद्वान, संयमो, विषय-व्यापार से रहित पुरुष को ही गुरु बनाना श्रेयस्कर है।
१२वीं संधि में संयम का उपदेश है। संयम के दो भेद हैं.--इन्द्रियसंयम और प्राणिसंयम । पहले इन्द्रिय संयम है। इन्द्रियों का असंयम प्रापत्ति का कारण है। जब एक एक इन्द्रिय के विषय प्राणघातक हैं तब पांघों ही इन्द्रियों के विषय किस अनर्थ को उत्पन्न नहीं करते। अतएव इन्द्रिय-विषयों का त्याग ज़रूरी है। मन द्वारा ही इन्द्रियां विषयों में प्रवृत्ति होती हैं। यदि मन वश में हो जाय, उसे विजित कर लिया जाय तो फिर इंद्रियां अपने विषयों में व्यापार नहीं कर सकतीं। प्रतः मन का जीतना जरूरी है। षट्काय के जीवों की रक्षा प्राणि संयम है। इसका पालन करना आवश्यक है।
४. See History of Gujrat in Bombay Gazeteer vol.1