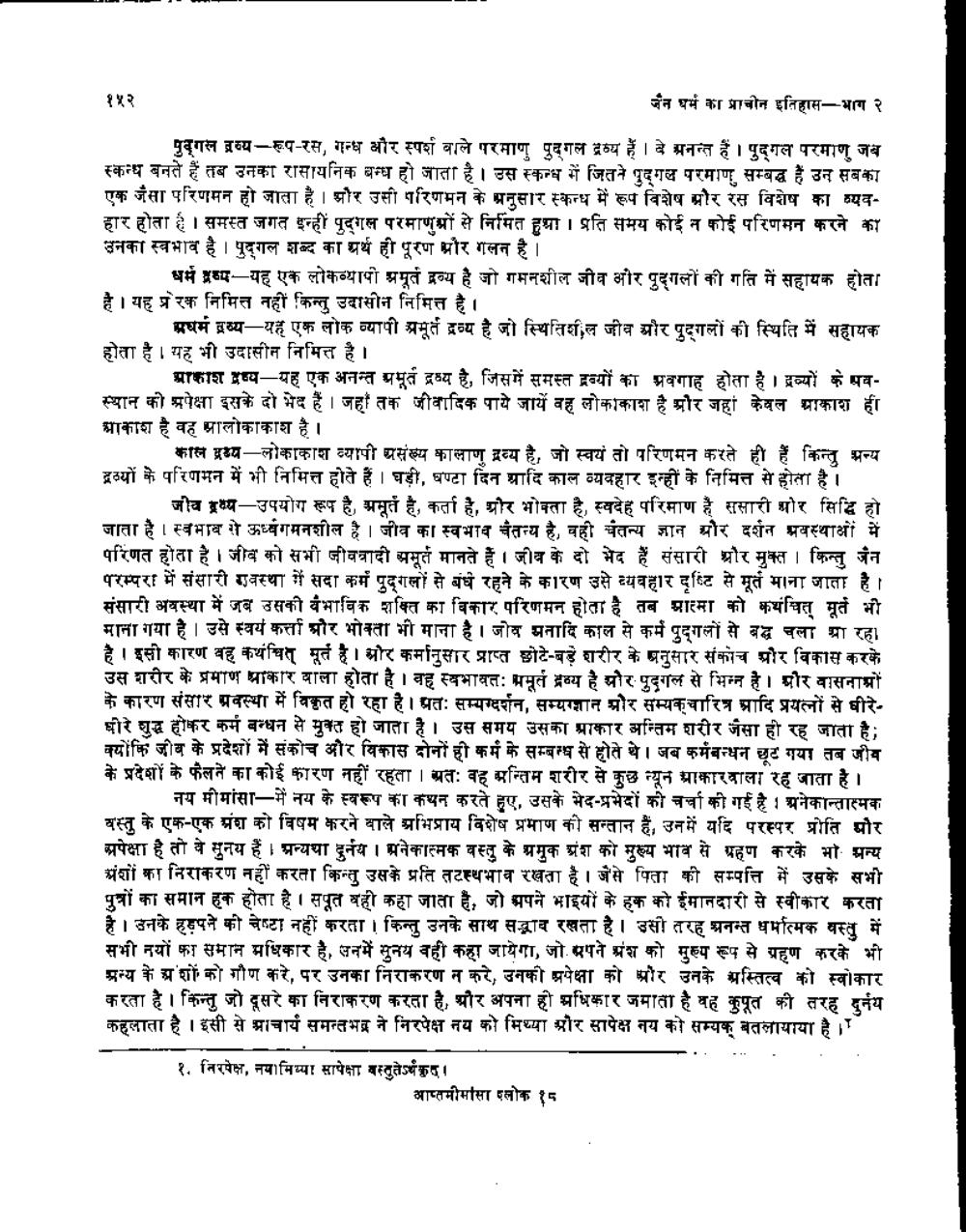________________
१५२
जैन धर्म का प्राचीन इतिहास-भाग २
चहा
पुद्गल तव्य-रूप-रस, गन्ध और स्पर्श बाले परमाणु पूगल द्रव्य हैं । वे अनन्त हैं। पुद्गल परमाणु जब स्कन्ध बनते हैं तब उनका रासायनिक बन्ध हो जाता है। उस स्कन्ध में जितने पुद्गल परमाणु सम्बद्ध हैं उन सबका एक जैसा परिणमन हो जाता है। और उसी परिणमन के अनुसार स्कन्ध में रूप विशेष प्रौर रस विशेष का व्यवहार होता है । समस्त जगत इन्हीं पुद्गल परमाणुनों से निर्मित हुना। प्रति समय कोई न कोई परिणमन करने का उनका स्वभाव है । पुद्गल' शब्द का अर्थ ही पूरण और गलन है।
धर्मव्य-यह एक लोकव्यापी प्रमुर्त द्रव्य है जो गमनशील जीव और पुद्गलों की गति में सहायक होता है। यह प्रेरक निमित्त नहीं किन्तु उदासीन निमित्त है।
अधर्म द्रव्य-यह एक लोक व्यापी अमूर्त द्रव्य है जो स्थितिशील जीव और पुद्गलों की स्थिति में सहायक होता है । यह भी उदासीन निमित्त है।
प्राकाश द्रव्य-यह एक अनन्त अमूर्त द्रव्य है, जिसमें समस्त द्रव्यों का प्रवगाह होता है । द्रव्यों के प्रवस्थान को अपेक्षा इसके दो भेद हैं । जहाँ तक जीवादिक पाये जायें वह लोकाकाश है और जहां केवल प्राकाश ही आकाश है वह पालोकाकाश है।
___ काल द्रव्य–लोकाकाश व्यापी असंख्य कालाणु द्रव्य है, जो स्वयं तो परिणमन करते ही हैं किन्तु अन्य द्रव्यों के परिणमन में भी निमित्त होते हैं । घड़ी, घण्टा दिन प्रादि काल व्यवहार इन्हीं के निमित्त से होता है।
जीव द्रव्य-उपयोग रूप है, अमूर्त है, कर्ता है, और भोक्ता है, स्वदेह परिमाण है ससारी और सिद्धि हो जाता है । स्वभाव से ऊध्वंगमनशील है। जीव का स्वभाव चैतन्य है, वही चंतन्य ज्ञान और दर्शन अवस्थाओं में परिणत होता है। जीव को सभी जीववादी अमूर्त मानते हैं । जीव के दो भेद हैं संसारी और मुक्त । किन्तु जैन परम्परा में संसारी अवस्था में सदा कर्म पुद्गलों से बंधे रहने के कारण उसे व्यबहार दृष्टि से मूर्त माना जाता है। संसारी अवस्था में जब उसकी वैभाविक शक्ति का विकार परिणमन होता है तब प्रात्मा को कथंचित् मूर्त भी माना गया है। उसे स्वयं कर्ता और भोक्ता भी माना है। जोय अनादि काल से कम पुद्गलों से बद्ध चला पा रहा है । इसी कारण वह कथंचित् मूर्त है। और कर्मानुसार प्राप्त छोटे-बड़े शरीर के अनुसार संकोच और विकास करके उस शरीर के प्रमाण प्राकार वाला होता है। वह स्वभावत: प्रमूर्त द्रव्य है और पूदगल से भिन्न है। और वासनामों के कारण संसार अवस्था में विकृत हो रहा है। प्रतः सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र प्रादि प्रयत्नों से धीरेघीरे शुद्ध होकर कर्म बन्धन से मुक्त हो जाता है। उस समय उसका प्राकार अन्तिम शरीर जैसा ही रह जाता है; क्योंकि जीव के प्रदेशों में संकोच और विकास दोनों ही कर्म के सम्बन्ध से होते थे। जब कर्मबन्धन छूट गया तब जीव के प्रदेशों के फैलने का कोई कारण नहीं रहता । अत: वह मन्तिम शरीर से कुछ न्यून प्राकारवाला रह जाता है।
नय मीमांसा-में नय के स्वरूप का कथन करते हुए, उसके भेद-प्रभेदों की चर्चा की गई है। अनेकान्तात्मक वस्तु के एक-एक अंश को विषम करने वाले अभिप्राय विशेष प्रमाण को सन्तान हैं, उनमें यदि परस्पर प्रोति पौर अपेक्षा है तो वे सुनय हैं । अन्यथा दुर्नय । अनेकात्मक वस्तु के अमुक अंश को मुख्य भाव से ग्रहण करके भो अन्य अंशों का निराकरण नहीं करता किन्तु उसके प्रति तटस्थभाव रखता है। जैसे पिता की सम्पत्ति में उसके सभी पुत्रों का समान हक होता है । सपूत वही कहा जाता है, जो अपने भाइयों के हक को ईमानदारी से स्वीकार करता है। उनके हड़पने की चेष्टा नहीं करता। किन्तु उनके साथ सद्भाव रखता है। उसी तरह अनन्त धर्मात्मक वस्तु में सभी नयों का समान मधिकार है, उनमें सुनय वही कहा जायेगा, जो अपने अंश को मुख्य रूप से ग्रहण करके भी अन्य के अशों को गौण करे, पर उनका निराकरण न करे, उनकी अपेक्षा को और उनके अस्तित्व को स्वीकार करता है। किन्तु जो दूसरे का निराकरण करता है, और अपना ही अधिकार जमाता है वह कुपूत की तरह दुर्नय कहलाता है । इसी से प्राचार्य समन्तभद्र ने निरपेक्ष नय को मिथ्या और सापेक्ष नय को सम्यक बतलायाया है।
१. निरपेक्ष, नयामिम्या सापेक्षा वस्तुतेऽर्थकृत ।
आप्तमीमांसा श्लोक १८