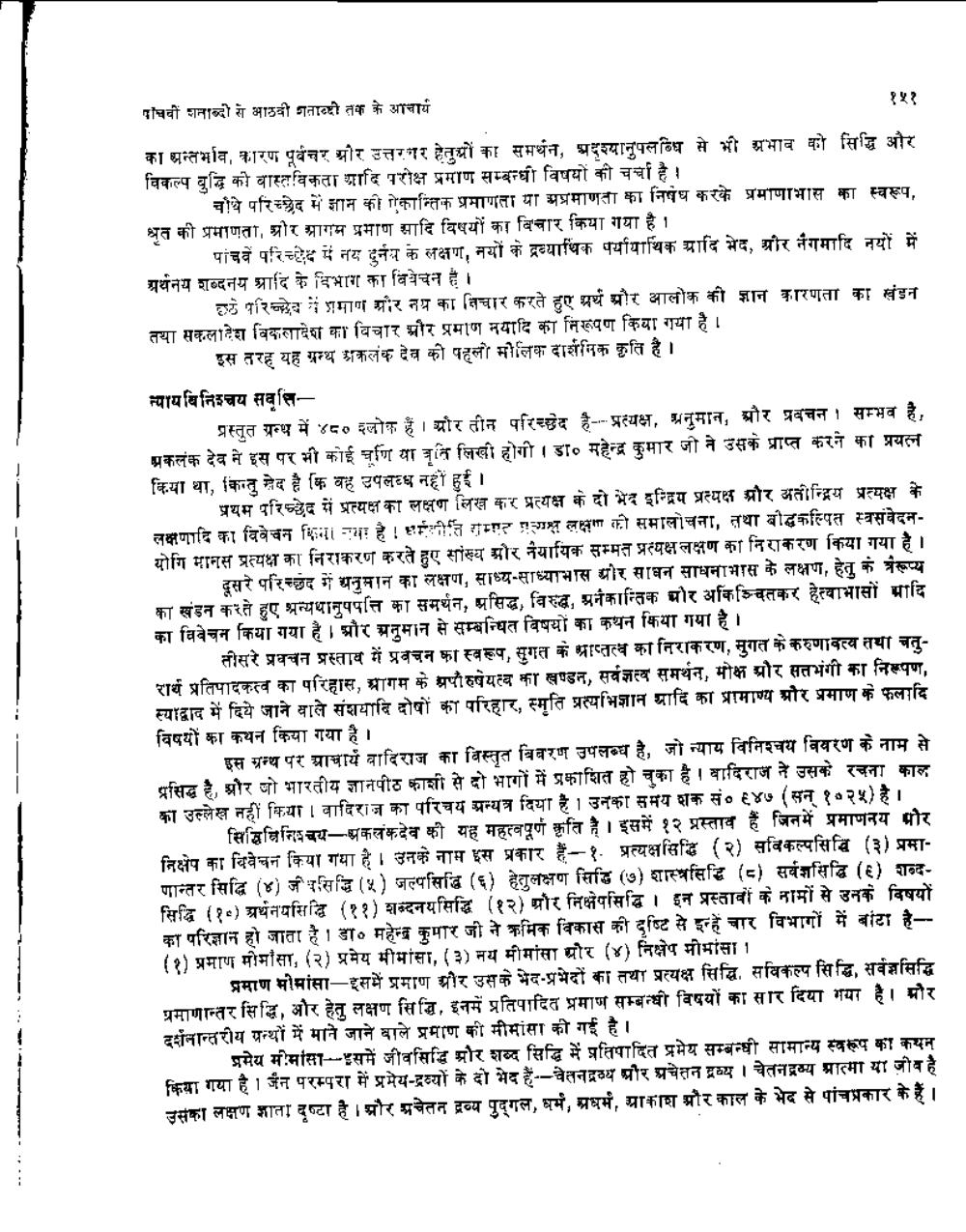________________
पांचवीं शताब्दी से आठवी शताब्दी तक के आचार्य
का अन्तर्भाव, कारण पूर्वचर और उत्तरगर हेतूमों का समर्थन, प्रदश्यानुपलब्धि से भी प्रभाव को सिद्धि और विकल्प बुद्धि को बास्तविकता यादि परोक्ष प्रमाण सम्बन्धी विषयों की चर्चा है।
चौथे परिच्छेद में ज्ञान की कान्तिक प्रमाणता या अप्रमाणता का निषेध करके प्रमाणाभास का स्वरूप, श्रुत की प्रमाणता, और आगम प्रमाण आदि विषयों का विचार किया गया है।
पांचवें परिच्छेद में नय दुर्नब के लक्षण, नयों के द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक आदि भेद, और नैगमादि नयों में अर्थनय शब्दनय आदि के विभाग का विवेचन है।
ठे परिच्छेव में प्रमाण पोर नय का विचार करते हए अर्थ और आलोक की ज्ञान कारणता का खंडन तथा सकलादेश विकलादेश का विचार और प्रमाण नयादि का निरूपण किया गया है ।
इस तरह यह ग्रन्थ अकलंक देव की पहली मौलिक दार्शनिक कृति है।
न्याय विनिश्चय सवृत्ति
प्रस्तुत ग्रन्थ में ४८० श्लोक हैं । और तीन परिच्छेद है--प्रत्यक्ष, अनुमान, और प्रवचन । सम्भव है, प्रकलंक देव मे इस पर भी कोई चणि या ति लिखी होगी । डा. महेन्द्र कुमार जी ने उसके प्राप्त करने का प्रयत्न किया था, किन्तु खेद है कि वह उपलब्ध नहीं हुई।
प्रथम परिच्छेद में प्रत्यक्ष का लक्षण लिख कर प्रत्यक्ष के दो भेद इन्द्रिय प्रत्यक्ष और अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष के लक्षणादि का विवेचन किया गया है ! धर्मशीति गमाटायच लक्षा को समालोचना, तथा बौद्धकल्पित स्वसंवेदनयोगि मानस प्रत्यक्ष का निराकरण करते हुए सांस्य और नैयायिक सम्मत प्रत्यक्ष लक्षण का निराकरण किया गया है।
दूसरे परिच्छेद में अनुमान का लक्षण, साध्य-साध्याभास और साधन साधनाभास के लक्षण, हेतु के रूप्य का खंडन करते हुए अन्यथानुपपत्ति का समर्थन, प्रसिद्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक पौर अकिश्चितकर हेत्वाभासों मादि का विवेचन किया गया है। और अनुमान से सम्बन्धित विषयों का कथन किया गया है।
तीसरे प्रवचन प्रस्ताव में प्रवचन का स्वरूप, सुगत के प्राप्तत्व का निराकरण, सुगत के करुणावत्य तथा चतुरार्थ प्रतिपादकत्व का परिहास, पागम के अपौरुषेयत्व का खण्डन, सर्वज्ञत्व समर्थन, मोक्ष और सत्तभंगी का निरूपण, स्याद्वाद में दिये जाने वाले संशयादि दोषों का परिहार, स्मृति प्रत्यभिज्ञान यादि का प्रामाण्य और प्रमाण के फलादि विषयों का कथन किया गया है।
___ इस ग्रन्थ पर प्राचार्य वादिराज का विस्तृत विवरण उपलब्ध है, जो न्याय विनिश्चय विवरण के नाम से प्रसिद्ध है, और जो भारतीय ज्ञानपीठ काशी से दो भागों में प्रकाशित हो चुका है । वादिराज ने उसके रचना काल का उल्लेख नहीं किया । वादिराज का परिचय अन्यत्र दिया है। उनका समय शक सं०६४७ (सन् १०२५) है।
सिसिमिनियचय-अकलंकदेव की यह महत्वपूर्ण कृति है। इसमें १२ प्रस्ताव हैं जिनमें प्रमाणनय और निक्षेप का विवेचन किया गया है। उनके नाम इस प्रकार हैं-१. प्रत्यक्षसिद्धि (२) सविकल्प सिद्धि (३) प्रमाणान्तर सिद्धि (४) जयसिद्धि (५) जल्पसिद्धि (६) हेतुलक्षण सिद्धि (७) शास्त्रसिद्धि (८) सर्वशसिद्धि (6) शब्दसिद्धि (१०) अर्थनयसिद्धि (११) शन्दनयसिद्धि (१२) और निक्षेपसिद्धि । इन प्रस्तावों के नामों से उनके विषयों का परिज्ञान हो जाता है । डा. महेन्द्र कुमार जी ने क्रमिक विकास की दृष्टि से इन्हें चार विभागों में बांटा है(१) प्रमाण मीमांसा, (२) प्रमेय मीमांसा, (३) नय मीमांसा और (४) निक्षेप मीमांसा।
प्रमाण मीमांसा-इसमें प्रमाण और उसके भेद-प्रभेदों का तथा प्रत्यक्ष सिद्धि, सविकल्प सिद्धि, सर्वसिद्धि प्रमाणान्तर सिद्धि, और हेतु लक्षण सिद्धि, इनमें प्रतिपादित प्रमाण सम्बन्धी विषयों का सार दिया गया है। और दर्शनान्तरीय ग्रन्थों में माने जाने वाले प्रमाण की मीमांसा की गई है।
प्रमेय मीमांसा-इसमें जीवसिद्धि और शब्द सिद्धि में प्रतिपादित प्रमेय सम्बन्धी सामान्य स्वरूप का कथन किया गया है। जैन परम्परा में प्रमेय-द्रव्यों के दो भेद हैं--चेतनद्रव्य और अचेतन द्रव्य । चेतनद्रव्य प्रात्मा या जीव है उसका लक्षण ज्ञाता दृष्टा है। और अचेतन द्रव्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल के भेद से पांचप्रकार के हैं।