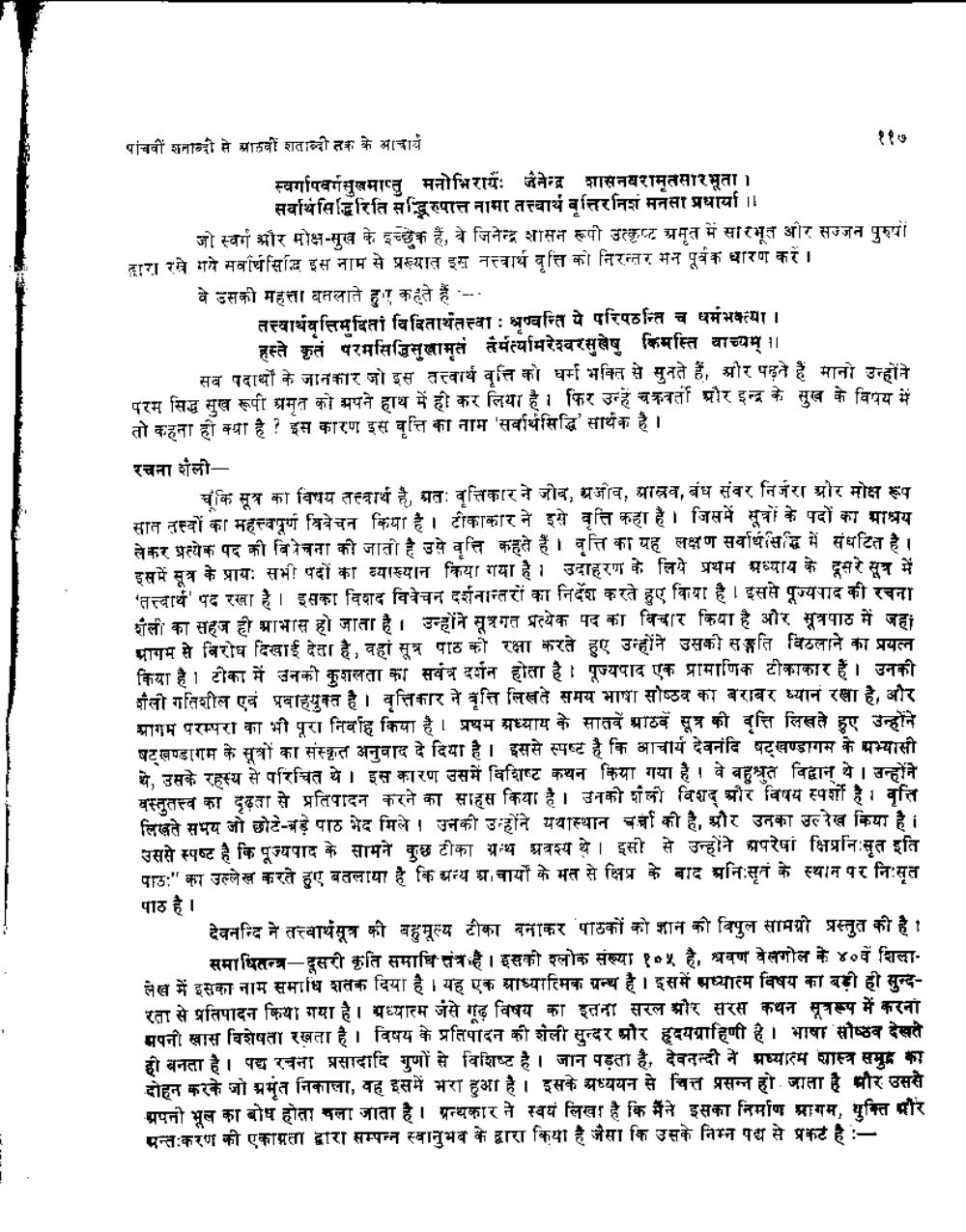________________
पांचवीं शनाब्दी से आठवीं शताब्दी तक के आचार्य
स्वर्गापवर्गसुखमाप्त मनोभिरायः जैनेन्द्र शासनवरामृतसारभूता।
सर्वार्थसिद्धिरिति सद्धिरुपात्त नामा तत्त्वार्थ वृत्तिरनिशं मनसा प्रधार्या ।। जो स्वर्ग और मोक्ष-सुख के इच्छेक हैं, वे जिनेन्द्र शासन रूपो उत्कृष्ट अमृत में सारभूत और सज्जन पुरुषों द्वारा रखे गये मार्थ सिद्धि इस नाम से प्रख्यात इस नत्त्वार्थ वृत्ति को निरन्तर मन पूर्वक धारण करें। वे उसकी महत्ता बतलाते हुए कहते हैं --..
तत्त्वार्थवत्तिमदितां विरितार्थतत्त्वा: अण्वन्ति ये परिपठन्ति च धर्मभक्त्या ।
हस्ते कृतं परमसिजिसुखामृतं तैर्मामरेश्वरसुखेषु किमस्ति वाच्यम् ।। सब पदार्थों के जानकार जो इस तत्त्वार्थ वृत्ति को धर्म भक्ति से सुनते हैं, और पढ़ते हैं मानो उन्होंने परम सिद्ध सुख रूपी प्रमत को अपने हाथ में ही कर लिया है। फिर उन्हें चक्रवर्ती और इन्द्र के सुख के विषय में तो कहना ही क्या है? इस कारण इस वृत्ति का नाम 'सर्वार्थसिद्धि' सार्थक है। रचना शैली
कि सूत्र का विषय तस्वार्थ है, अतः वृत्तिकार ने जीव, अजीव, पालव, बंध संवर निर्जरा और मोक्ष रूप सात तस्वों का महत्त्वपूर्ण विवेचन किया है। टीकाकार ने इसे वृत्ति कहा है। जिसमें सूत्रों के पदों का पाश्रय लेकर प्रत्येक पद की विवेचना की जाती है उसे वृत्ति कहते हैं। वृत्ति का यह लक्षण सर्वार्थसिद्धि में संघटित है। इसमें सूत्र के प्रायः सभी पदों का व्याख्यान किया गया है। उदाहरण के लिये प्रथम अध्याय के दूसरे सूत्र में 'तत्त्वार्थ' पद रखा है। इसका विवाद विवेचन दर्शनान्तरों का निर्देश करते हुए दिया है । इससे पूज्यपाद की रचना शैली का सहज ही प्राभास हो जाता है। उन्होंने सूत्रगत प्रत्येक पद का विचार किया है और सूत्रपाठ में जहां मागम से विरोध दिखाई देता है, वहां सूत्र पाठ की रक्षा करते हुए उन्होंने उसकी सङ्गति विठलाने का प्रयत्न किया है। टीका में उनकी कुशलता का सर्वत्र दर्शन होता है। पूज्यपाद एक प्रामाणिक टीकाकार हैं। उनकी शैली गतिशील एवं प्रवाहयुक्त है। वृत्तिकार ने वृत्ति लिखते समय भाषा सौष्ठव का बराबर ध्यान रखा है, और मागम परम्परा का भी पूरा निर्वाह किया है। प्रथम अध्याय के सातवें पाठवें सूत्र की वृत्ति लिखते हुए उन्होंने षट खण्डागम के सूत्रों का संस्कृत अनुवाद दे दिया है। इससे स्पष्ट है कि आचार्य देवनंदि षट्खण्डागम के अभ्यासी थे, उसके रहस्य से परिचित थे। इस कारण उसमें विशिष्ट कथन किया गया है। वे बहश्रत विद्वान थे। उन्होंने वस्तूतत्त्व का दृढ़ता से प्रतिपादन करने का साहस किया है। उनकी शैली विशद् और विषय स्पर्शो है। वत्ति लिखते समय जो छोटे-बड़े पाठ भेद मिले। उनकी उन्होंने यथास्थान चर्चा की है, और उनका उल्लेख किया है। उससे स्पष्ट है कि पूज्यपाद के सामने कुछ टीका ग्रन्थ अवश्य थे। इसी से उन्होंने अपरेषां क्षिनिःसूत इति पाउ:" का उल्लेख करते हुए बतलाया है कि अन्य प्राचार्यों के मत से क्षिप्र के बाद अनिःसतं के स्थान पर निःसत पाठ है।
देवनन्दि ने तत्त्वार्थसूत्र की बहुमूल्य टीका बनाकर पाठकों को ज्ञान की विपुल सामग्री प्रस्तुत की है।
समाधितन्त्र-दुसरी कृति समाधि तंत्र है। इसकी श्लोक संख्या १०५ है, श्रवण वेलगोल के ४०वें शिलालेख में इसका नाम समाधि शतक दिया है। यह एक प्राध्यात्मिक ग्रन्थ है। इसमें मध्यात्म विषय का बड़ी ही सुन्दरता से प्रतिपादन किया गया है। अध्यात्म से गढ़ विषय का इतना सरल और सरस कथन सूत्ररूप में करना मपनी खास विशेषता रखता है। विषय के प्रतिपादन की शैली सुन्दर और हृदयग्राहिणी है। भाषा सौष्ठव देखते ही बनता है। पद्य रचना प्रसादादि गुणों से विशिष्ट है। जान पड़ता है, देवनन्दी ने अध्यात्म शास्त्र समुद्र का दोहन करके जो अमृत निकाला, वह इसमें भरा हुआ है। इसके अध्ययन से चित्त प्रसन्न हो जाता है और उससे अपनी भूल का बोध होता चला जाता है। ग्रन्थकार ने स्वयं लिखा है कि मैंने इसका निर्माण प्रागम, युक्ति और पन्तःकरण की एकाग्रता द्वारा सम्पन्न स्वानुभव के द्वारा किया है जैसा कि उसके निम्न पद्य से प्रकट है: