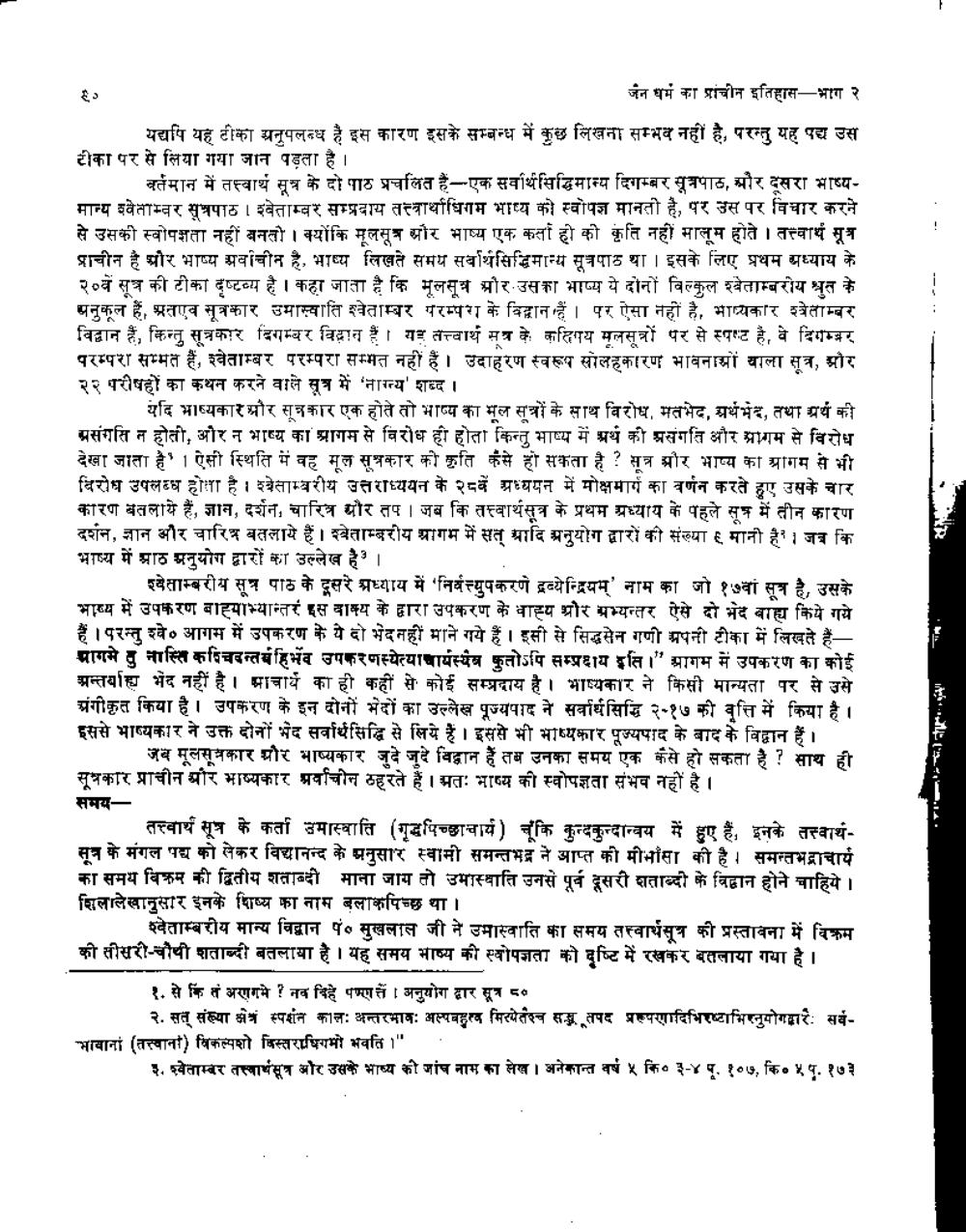________________
जन धर्म का प्राचीन इतिहास-भाग २
यद्यपि यह टीका अनुपलब्ध है इस कारण इसके सम्बन्ध में कुछ लिखना सम्भव नहीं है, परन्तु यह पद्य उस टीका पर से लिया गया जान पड़ता है।
वर्तमान में तत्त्वार्थ सूत्र के दो पाठ प्रचलित हैं-एक सर्वार्थसिद्धिमान्य दिगम्बर सुत्रपाठ, और दसरा भाष्यमान्य श्वेताम्बर सुत्रपाठ । श्वेताम्बर सम्प्रदाय तत्त्वार्थाधिगम भाष्य को स्वोपज्ञ मानती है, पर उस पर विचार करने से उसकी स्वोपज्ञता नहीं बनती। क्योंकि मूलसूत्र और भाष्य एक कर्ता ही को कृति नहीं मालूम होते । तत्त्वार्थ सूत्र प्राचीन है और भाष्य अर्वाचीन है, भाध्य लिखते समय सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठ था । इसके लिए प्रथम अध्याय के २०वें सूत्र की टीका दृष्टव्य है । कहा जाता है कि मूलसूत्र और उसका भाष्य ये दोनों विल्कुल श्वेताम्बरीय श्रुत के अनुकूल हैं, अतएव सूत्रकार उमास्वाति श्वेताम्बर परम्परा के विद्वान हैं। पर ऐसा नहीं है, भाष्यकार श्वेताम्बर विद्वान हैं, किन्तु सूत्रकार दिगम्बर विद्वान हैं। यह तत्त्वार्थ सूत्र के कतिपय मूलसूत्रों पर से स्पष्ट है, वे दिगम्बर परम्परा सम्मत हैं, श्वेताम्बर परम्परा सम्मत नहीं हैं। उदाहरण स्वरूप सोलहकारण भावनाओं याला सूत्र, और २२ परीषहों का कथन करने वाले सुत्र में 'नान्य' शब्द ।।
यदि भाष्यकार और सूत्रकार एक होते तो भाष्य का मल सत्रों के साथ विरोध, मतभेद, अर्थभेद, तथा अर्थ की प्रसंगति न होती, और न भाष्य का प्रागम से विरोध ही होता किन्तु भाष्य में अर्थ की प्रसंगति और प्रागम से विरोध देखा जाता है। 1 ऐसी स्थिति में वह मूल सूत्रकार को कृति कैसे हो सकता है ? सूत्र और भाष्य का अागम से भी बिरोध उपलब्ध होता है। श्वेताम्बरीय उत्तराध्ययन के २८३ अध्ययन में मोक्षमार्ग का वर्णन करते हुए उसके चार कारण बतलाये हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप । जब कि तत्त्वार्थसूत्र के प्रथम अध्याय के पहले सूत्र में तीन कारण दर्शन, ज्ञान और चारित्र बतलाये हैं। श्वेताम्बरीय प्रागम में सत् प्रादि अनुयोग द्वारों की संख्या ६ मानी है। जब कि भाष्य में पाठ अनुयोग द्वारों का उल्लेख है।
श्वेताम्बरीय सूत्र पाठ के दूसरे अध्याय में 'निर्वत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्' नाम का जो १७वां सूत्र है, उसके भाष्य में उपकरण बाह्याभ्यान्तर इस वाक्य के द्वारा उपकरण के वाह्य और अभ्यन्तर ऐसे दो भेद बाह्य किये गये हैं। परन्तु श्वे० आगम में उपकरण के ये दो भेदनहीं माने गये हैं। इसी से सिद्धसेन गणी अपनी टीका में लिखते हैंमागमे तु नास्ति कविचवन्त हि व उपकरणस्येत्याचार्यस्यैव कुतोऽपि सम्प्रदाय इति।" पागम में उपकरण का कोई अन्तर्वाह्य भेद नहीं है। प्राचार्य का ही कहीं से कोई सम्प्रदाय है। भाष्यकार ने किसी मान्यता पर से उसे अंगीकृत किया है। उपकरण के इन दोनों भेदों का उल्लेख पूज्यपाद ने सर्वार्थसिद्धि २-१७की वृत्ति में किया है। इससे भाष्यकार ने उक्त दोनों भेद सर्वार्थसिद्धि से लिये हैं। इससे भी भाष्यकार पूज्यपाद के बाद के विद्वान हैं।
जब मूलसूत्रकार और भाष्यकार जुदे जुदे विद्वान हैं तब उनका समय एक कैसे हो सकता है ? साथ ही सूत्रकार प्राचीन और भाष्यकार अर्वाचीन ठहरते हैं । अतः भाष्य की स्वोपज्ञता संभव नहीं है। समय
तत्त्वार्थ सूत्र के कर्ता उमास्वाति (गृपिच्छाचार्य) चूंकि कुन्दकुन्दान्वय में हुए हैं, इनके तस्वार्थसूत्र के मंगल पद्य को लेकर विद्यानन्द के अनुसार स्वामी समन्तभद्र ने आप्त की मीमांसा की है। समन्तभद्राचार्य का समय विक्रम की द्वितीय शताब्दी माना जाय तो उभास्वाति उनसे पूर्व दूसरी शताब्दी के विद्वान होने चाहिये। शिलालेखानुसार इनके शिष्य का नाम बलाकपिच्छ था।
श्वेताम्बरीय मान्य विद्वान पं० सुखलाल जी ने उमास्वाति का समय तस्वार्थसत्र की प्रस्तावना में विक्रम की तीसरी-चौथी शताब्दी बतलाया है। यह समय भाष्य की स्वोपज्ञता को दृष्टि में रखकर बतलाया गया है।
१.से कि त अरणगमे ? नव बिहे पण तें । अनुयोग द्वार सूत्र ८०
२. सत् संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालः अन्तरभाकः अल्पबहत्व मिरपेतेश्च समतपद प्ररूपणादिभिरष्टाभिरनुयोगद्वारः सर्वभावाना (तरवाना) विकल्पशो विस्तराषियमो भवति ।" .
३. श्वेताम्बर तत्त्वार्थसूत्र और उसके भाष्य की जांच नाम का लेख । अनेकान्त वर्ष ५ कि० ३-४ पू. १०७, कि.५५. १७३