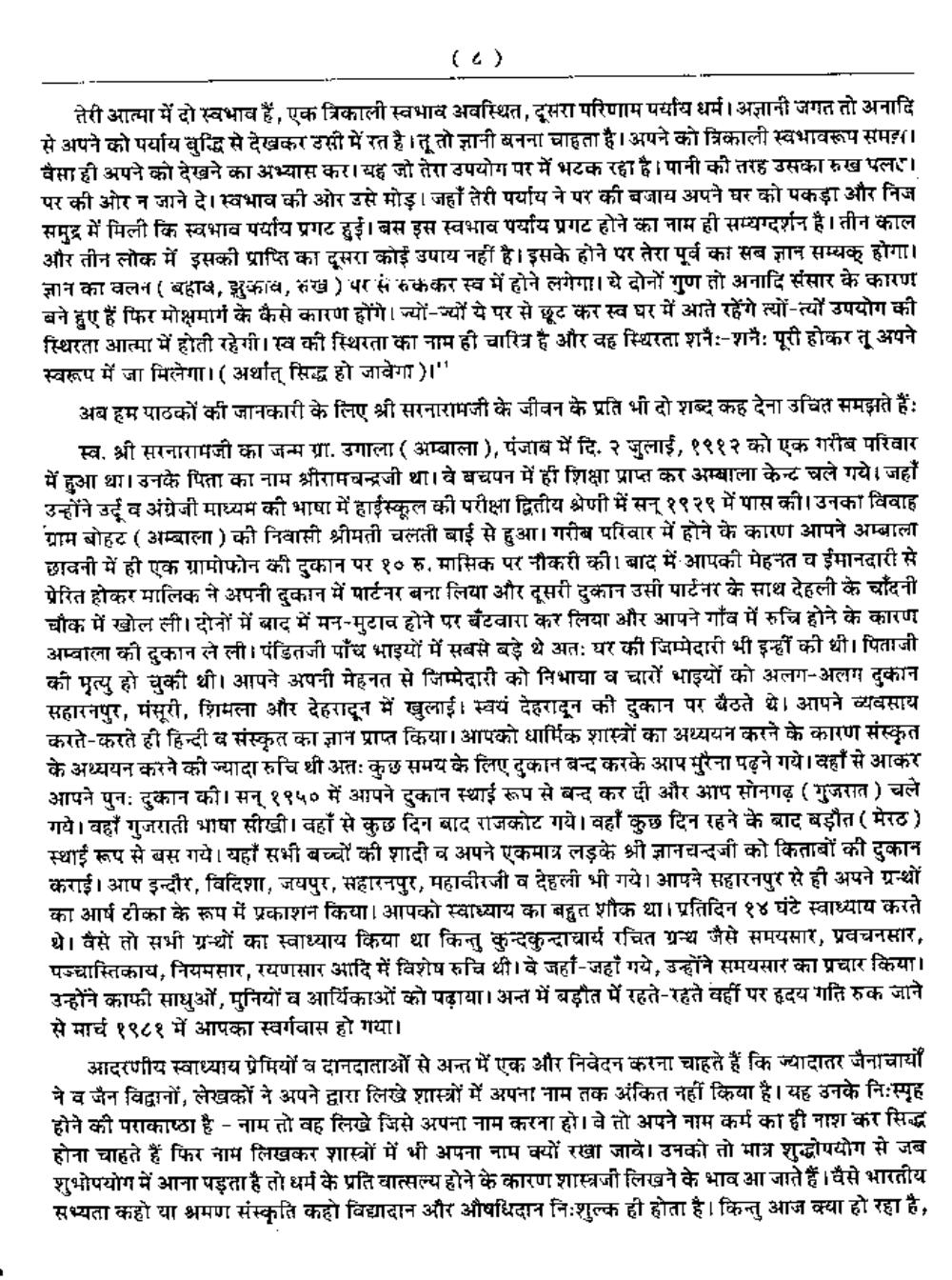________________
तेरी आत्मा में दो स्वभाव हैं, एक त्रिकाली स्वभाव अवस्थित, दूसरा परिणाम पर्याय धर्म। अज्ञानी जगत तो अनादि से अपने को पर्याय बुद्धि से देखकर उसी में रत है। तू तो ज्ञानी बनना चाहता है। अपने को त्रिकाली स्वभावरूप समड़ा। वैसा ही अपने को देखने का अभ्यास कर। यह जो तेरा उपयोग पर में भटक रहा है। पानी की तरह उसका रुख पलाए। पर की ओर न जाने दे। स्वभाव की ओर उसे मोड़। जहाँ तेरी पर्याय ने पर की बजाय अपने घर को पकड़ा और निज समुद्र में मिली कि स्वभाव पर्याय प्रगट हुई। बस इस स्वभाव पर्याय प्रगट होने का नाम ही सम्यग्दर्शन है। तीन काल
और तीन लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसके होने पर तेरा पूर्व का सब ज्ञान सम्यक् होगा। ज्ञान का वलन ( बहाव, झुकाव, रुख) पर रुककर स्व में होने लगेगा। ये दोनों गुण तो अनादि संसार के कारण बने हुए हैं फिर मोक्षमार्ग के कैसे कारण होंगे। ज्यों-ज्यों ये पर से छूट कर स्व घर में आते रहेंगे त्यों-त्यों उपयोग की स्थिरता आत्मा में होती रहेगी। स्व की स्थिरता का नाम ही चारित्र है और वह स्थिरता शनैः-शनैः पूरी होकर तू अपने स्वरूप में जा मिलेगा। ( अर्थात् सिद्ध हो जावेगा)।"
अब हम याठकों की जानकारी के लिए श्री सरनारामजी के जीवन के प्रति भी दो शब्द कह देना उचित समझते हैं:
स्व. श्री सरनारामजी का जन्म ग्रा. उगाला ( अम्बाला), पंजाब में दि. २ जुलाई, १९१२ को एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीरामचन्द्रजी था। वे बचपन में ही शिक्षा प्राप्त कर अम्बाला केन्ट चले गये। जहाँ उन्होंने उर्दू व अंग्रेजी माध्यम की भाषा में हाईस्कूल की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में सन् १९२९ में पास की। उनका विवाह ग्राम बोहट ( अम्बाला) की निवासी श्रीमती चलती बाई से हुआ। गरीब परिवार में होने के कारण आपने अम्बाला छावनी में ही एक ग्रामोफोन की दुकान पर १० रू. मासिक पर नौकरी की। बाद में आपकी मेहनत व ईमानदारी से प्रेरित होकर मालिक ने अपनी दुकान में पार्टनर बना लिया और दूसरी दुकान उसी पार्टनर के साथ देहली के चाँदनी चौक में खोल ली। दोनों में बाद में मन-मुटाव होने पर बँटवारा कर लिया और आपने गाँव में रुचि होने के कारण अम्बाला की दुकान ले ली। पंडितजी पाँच भाइयों में सबसे बड़े थे अत: घर की जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी। पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। आपने अपनी मेहनत से जिम्मेदारी को निभाया व चारों भाइयों व सहारनपुर, मंसूरी, शिमला और देहरादून में खुलाई। स्वयं देहरादून की दुकान पर बैठते थे। आपने व्यवसाय करते-करते ही हिन्दी व संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। आपको धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करने के कारण संस्कृत के अध्ययन करने की ज्यादा रुचि थी अतः कुछ समय के लिए दुकान बन्द करके आप मुरैना पढ़ने गये। वहाँ से आकर आपने पुन: दुकान की। सन् १९५० में आपने दुकान स्थाई रूप से बन्द कर दी और आप सोनगढ़ (गुजरात) चले गये। वहाँ गुजराती भाषा सीखी। वहाँ से कुछ दिन बाद राजकोट गये। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद बड़ौत ( मेरठ)
से बस गये। यहाँ सभी बच्चों की शादी व अपने एकमात्र लड़के श्री ज्ञानचन्दजी को किताबों की दुकान कराई। आप इन्दौर, विदिशा, जयपुर, सहारनपुर, महावीरजी व देहली भी गये। आपने सहारनपुर से ही अपने ग्रन्थों का आर्ष टीका के रूप प्रकाशन किया। आपको स्वाध्याय का बहुत शौक था। प्रतिदिन १४ घंटे स्वाध्याय करते थे। वैसे तो सभी ग्रन्थों का स्वाध्याय किया था किन्तु कुन्दकुन्दाचार्य रचित ग्रन्थ जैसे समयसार, प्रवचनसार, पञ्चास्तिकाय, नियमसार, रयणसार आदि में विशेष रुचि थी। वे जहाँ-जहाँ गये, उन्होंने समयसार का प्रचार किया। उन्होंने काफी साधुओं, मनियों व आर्यिकाओं को पढाया। अन्त में बडौत में रहते-रहते वहीं पर हदय गति रुक जाने से मार्च १९८१ में आपका स्वर्गवास हो गया।
आदरणीय स्वाध्याय प्रेमियों व दानदाताओं से अन्त में एक और निवेदन करना चाहते हैं कि ज्यादातर जैनाचार्यों ने व जैन विद्वानों, लेखकों ने अपने द्वारा लिखे शास्त्रों में अपना नाम तक अंकित नहीं किया है। यह उनके नि:स्पृह होने की पराकाष्ठा है - नाम तो वह लिखे जिसे अपना नाम करना हो। वे तो अपने नाम कर्म का ही नाश कर सिद्ध होना चाहते हैं फिर नाम लिखकर शास्त्रों में भी अपना नाम क्यों रखा जावे। उनको तो मात्र शुद्धोपयोग से जब शुभोपयोग में आना पड़ता है तो धर्म के प्रति वात्सल्य होने के कारण शास्त्रजी लिखने के भाव आ जाते हैं। वैसे भारतीय सभ्यता कहो या श्रमण संस्कृति कहो विद्यादान और औषधिदान निःशुल्क ही होता है। किन्तु आज क्या हो रहा है,