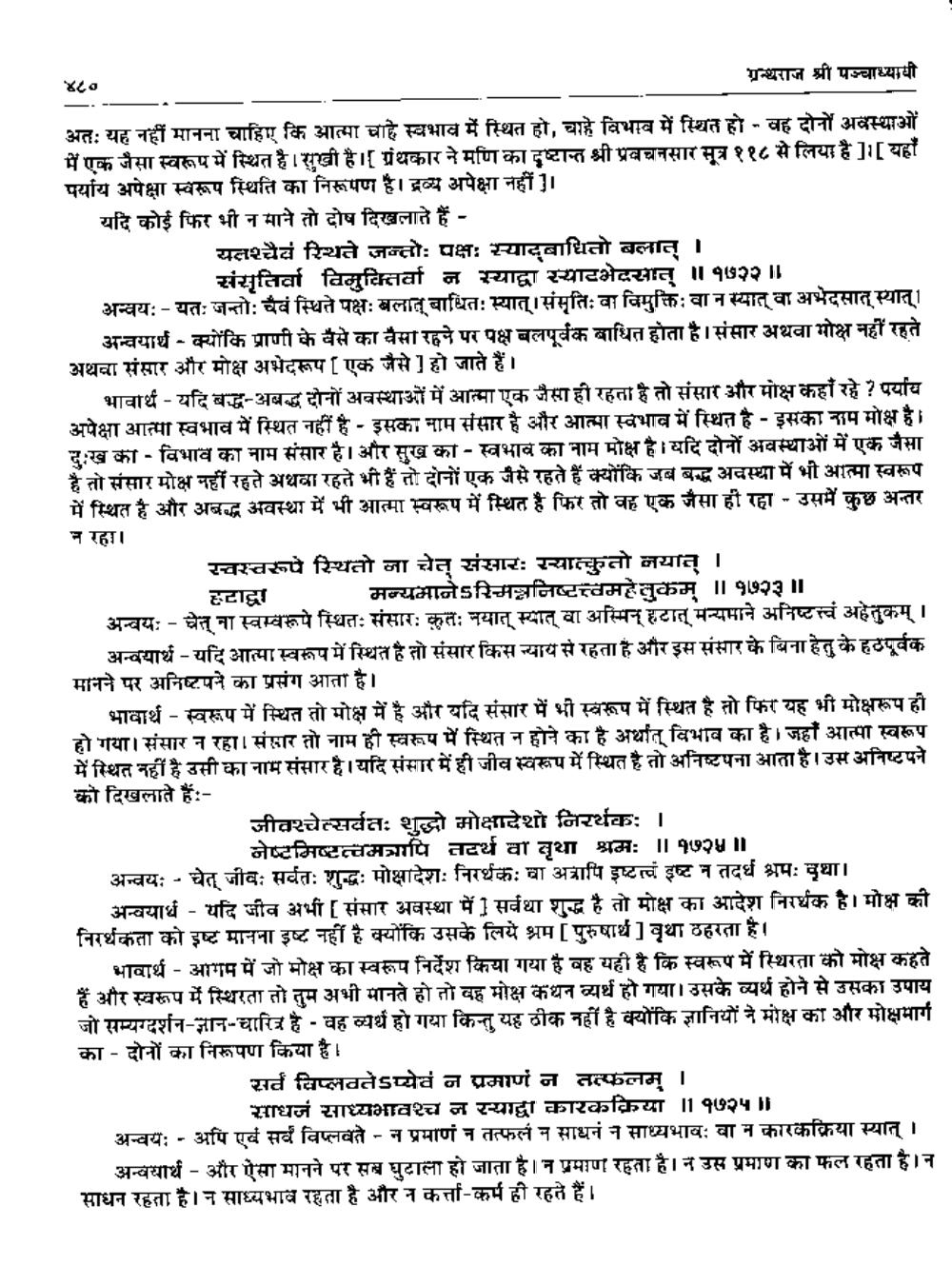________________
४८०
ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी
अतः यह नहीं मानना चाहिए कि आत्मा चाहे स्वभाव में स्थित हो, चाहे विभाव में स्थित हो - वह दोनों अवस्थाओं में एक जैसा स्वरूप में स्थित है। सुखी है।[ग्रंथकार ने मणिका दृष्टान्त श्री प्रवचनसार सूत्र ११८ से लिया है ][यहाँ पर्याय अपेक्षा स्वरूप स्थिति का निरूपण है। द्रव्य अपेक्षा नहीं। यदि कोई फिर भी न माने तो दोष दिखलाते हैं
यतश्चैवं स्थिते जन्तोः पक्षः स्याद्बाधितो बलात् ।
संसतिर्वा विमुक्तिर्वा न स्याद्वा स्याटभेदसात् ॥ १७२२॥ अन्वय: - यतः जन्तो: चैवं स्थिते पक्षः बलात् बाधित: स्यात्।संसृतिः वा विमुक्तिः वा न स्यात् वा अभेदसात् स्यात्।
अन्वयार्थ - क्योंकि प्राणी के वैसे का वैसा रहने पर पक्ष बलपूर्वक बाधित होता है। संसार अथवा मोक्ष नहीं रहते अथवा संसार और मोक्ष अभेदरूप[एक जैसे हो जाते हैं। __ भावार्थ - यदि बद्ध-अबद्ध दोनों अवस्थाओं में आत्मा एक जैसा ही रहता है तो संसार और मोक्ष कहाँ रहे ? पर्याय अपेक्षा आत्मा स्वभाव में स्थित नहीं है - इसका नाम संसार है और आत्मा स्वभाव में स्थित है - इसका नाम मोक्ष है। दुःखका-विभाव का नाम संसार है। और सुख का- स्वभाव का नाम मोक्ष है। यदि दोनों अवस्थाओं में एक जैसा है तो संसार मोक्ष नहीं रहते अथवा रहते भी हैं तो दोनों एक जैसे रहते हैं क्योंकि जब बद्ध अवस्था में भी आत्मा स्वरूप में स्थित है और अबद्ध अवस्था में भी आत्मा स्वरूप में स्थित है फिर तो वह एक जैसा ही रहा - उसमें कुछ अन्तर न रहा।
स्वस्वरूपे स्थितो ना चेत् संसार: स्यात्कुतो नयात् । हटाद्वा
मन्यमानेऽस्मिन्ननिष्टत्त्वमहे। कम् ॥ १७२३॥ अन्वयः - चेत् ना स्वम्वरूपे स्थितः संसार: कुतः नयात् स्यात् वा अस्मिन् हटात् मन्यमाने अनिष्टत्त्वं अहेतुकम् ।
अन्वयार्थ - यदि आत्मा स्वरूप में स्थित है तो संसार किस न्याय से रहता है और इस संसार के बिना हेतु के हठपूर्वक मानने पर अनिष्टपने का प्रसंग आता है। ___ भावार्थ - स्वरूप में स्थित तो मोक्ष में है और यदि संसार में भी स्वरूप में स्थित है तो फिर यह भी मोक्षरूप ही हो गया। संसार न रहा। संहार तो नाम ही स्वरूप में स्थित न होने का है अर्थात विभाव का है। जहाँ आत्मा स्वरूप में स्थित नहीं है उसी का नाम संसार है। यदि संसार में ही जीव स्वरूप में स्थित है तो अनिष्टपना आता है। उस अनिष्टपने को दिखलाते हैं:
जीतश्चेत्सर्वतः शुद्धो मोक्षादेशो निरर्थकः ।
नेष्टमिष्टत्वमत्रापि तदर्थ वा वृथा श्रमः || १७२५॥ अन्वयः - चेत् जीवः सर्वत: शुद्धः मोक्षादेशः निरर्थकः चा अत्रापि इष्टत्वं इष्ट न तदर्थ श्रमः वृथा।
अन्वयार्थ - यदि जीव अभी [ संसार अवस्था में] सर्वथा शुद्ध है तो मोक्ष का आदेश निरर्थक है। मोक्ष की निरर्थकता को इष्ट मानना इष्ट नहीं है क्योंकि उसके लिये श्रम [ पुरुषार्थ ] वृथा ठहरता है।
भावार्थ - आगम में जो मोक्ष का स्वरूप निर्देश किया गया है वह यही है कि स्वरूप में स्थिरता को मोक्ष कहते हैं और स्वरूप में स्थिरता तो तुम अभी मानते हो तो वह मोक्ष कथन व्यर्थ हो गया। उसके व्यर्थ होने से उसका उपाय जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र है - वह व्यर्थ हो गया किन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि ज्ञानियों ने मोक्ष का और मोक्षमार्ग का-दोनों का निरूपण किया है।
सर्वं विप्लवतेऽप्येवं न प्रमाणं न तत्फलम् ।
साधजं साध्यभावश्च न रयाद्वा कारकक्रिया ॥ १७२५।। अन्वयः - अपि एवं सर्व विप्लवते - न प्रमाणं न तत्फलं न साधनं न साध्यभावः वा न कारकक्रिया स्यात् ।
अन्वयार्थ - और ऐसा मानने पर सब घुटाला हो जाता है। न प्रमाण रहता है। न उस प्रमाण का फल रहता है।न साधन रहता है। न साध्यभाव रहता है और न कर्ता-कर्म ही रहते हैं।