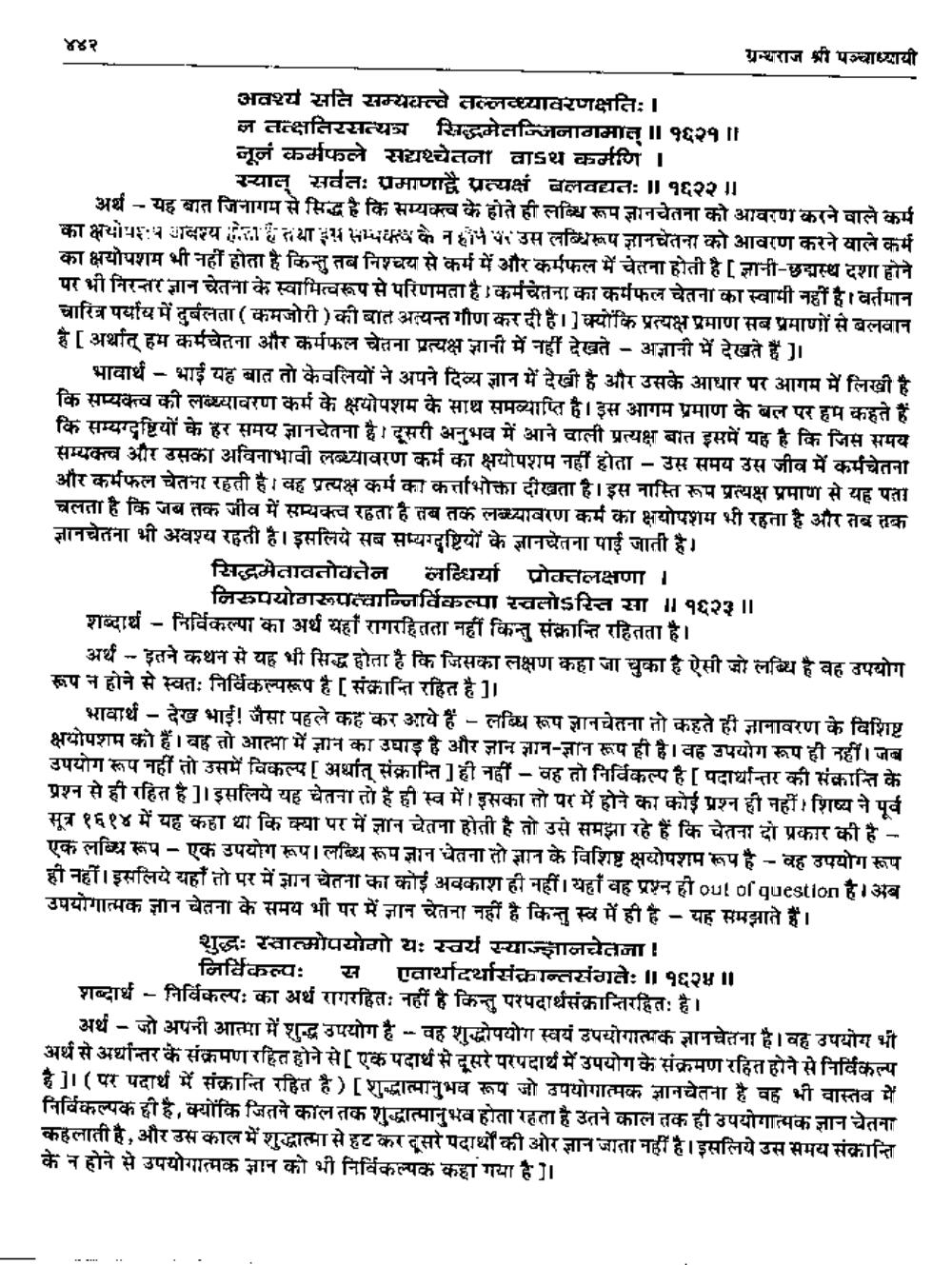________________
ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी
अवश्य सति सम्यक्त्वे तल्लव्ध्यावरणक्षतिः। ज तक्षतिरसत्यत्र सिद्भमेतजिनागमात् ।। १६२१॥ नूनं कर्मफले सद्यश्चेतना वाsथ कर्मणि ।
स्यात् सर्वतः प्रमाणाद्वै प्रत्यक्षं बलवद्यतः ॥ १६२२॥ अर्थ- यह बात जिनागम से सिद्ध है कि सम्यक्त्व के होते ही लब्धि रूप ज्ञानचेतना को आवरण करने वाले कर्म का क्षयोपश्य अवश्य होता है तथा इस सम्यक्षकेनहोने पर उस लब्धिरूप ज्ञानचेतना को आवरण करने वाले कर्म का क्षयोपशम भी नहीं होता है किन्तु तब निश्चय से कर्म में और कर्मफल में चेतना होती है [ज्ञानी-छद्मस्थ दशा होने पर भी निरन्तर ज्ञान चेतना के स्वामित्वरूप से परिणमता है। कर्मचेतना का कर्मफल चेतना का स्वामी नहीं है। वर्तमान चारित्र पर्याय में दुर्बलता (कमजोरी)की बात अत्यन्त गीण कर दी है। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण सब प्रमाणों से बलवान है [अर्थात् हम कर्मचेतना और कर्मफल चेतना प्रत्यक्ष ज्ञानी में नहीं देखते - अज्ञानी में देखते हैं । __ भावार्थ - भाई यह बात तो केवलियों ने अपने दिव्य ज्ञान में देखी है और उसके आधार पर आगम में लिखी है कि सम्यक्त्व की लब्ध्यावरण कर्म के क्षयोपशम के साथ समव्याप्ति है। इस आगम प्रमाण के बल पर हम कहते हैं कि सम्यग्दृष्टियों के हर समय ज्ञानचेतना है। दूसरी अनुभव में आने वाली प्रत्यक्ष बात इसमें यह है कि जिस समय सम्यक्व और उसका अविनाभावी लब्ध्यावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं होता - उस समय उस जीव में कर्मचेतना और कर्मफल चेतना रहती है। वह प्रत्यक्ष कर्म का कर्ताभोक्ता दीखता है। इस नास्ति रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से यह पता चलता है कि जब तक जीव में सम्यक्त्व रहता है तब तक लब्ध्यावरण कर्म का क्षयोपशम भी रहता है और तब तक ज्ञानचेतना भी अवश्य रहती है। इसलिये सब सम्यग्दृष्टियों के ज्ञानचेतना पाई जाती है।
सिद्धमेताततोवतेन लब्धिर्या प्रोक्त्तलक्षणा ।
निरुपयोगरूपत्वान्जिर्विकल्पा रचलोऽरित सा ॥ १९२३॥ शब्दार्थ - निर्विकल्पा का अर्थ यहाँ रागरहितता नहीं किन्तु संक्रान्ति रहितता है।
अर्थ - इतने कथन से यह भी सिद्ध होता है कि जिसका लक्षण कहा जा चुका है ऐसी जो लब्धि है वह उपयोग रूप न होने से स्वतः निर्विकल्परूप है [ संक्रान्ति रहित है ]|
भावार्थ-देख भाई! जैसा पहले कह कर आये हैं - लब्धि रूप ज्ञानचेतना तो कहते ही ज्ञानावरण के विशिष्ट क्षयोपशम को हैं। बह तो आत्मा में ज्ञान का उघाड़ है और ज्ञान ज्ञान-ज्ञान रूप ही है। वह उपयोग रूप ही नहीं। जब उपयोग रूप नहीं तो उसमें विकल्प [ अर्थात् संक्रान्ति] ही नहीं- वह तो निर्विकल्प है [ पदार्थान्तर की संक्रान्ति के प्रश्न से ही रहित है ]। इसलिये यह चेतना तो है ही स्व में। इसका तो पर में होने का कोई प्रश्न ही नहीं। शिष्य ने पूर्व सूत्र १६१४ में यह कहा था कि क्या पर में ज्ञान चेतना होती है तो उसे समझा रहे हैं कि चेतना दो प्रकार की है - एक लब्धि रूप - एक उपयोग रूप। लब्धि रूप ज्ञान चेतना तो ज्ञान के विशिष्ट क्षयोपशम रूप है - वह उपयोग रूप ही नहीं। इसलिये यहाँ तोपर में ज्ञानचेतना का कोई अवकाश ही नहीं। यहाँ वह प्रश्न ही out of question है। अब उपयोगात्मक ज्ञान चेतना के समय भी पर में ज्ञान चेतना नहीं है किन्तु स्व में ही है - यह समझाते हैं।
शुद्धः स्वात्मोपयोगो यः स्वयं स्याज्ज्ञानचेतना!
निर्विकल्पः स एवार्थादर्थासंक्रान्तसंगतेः॥ १६२४॥ शब्दार्थ - निर्विकल्पः का अर्थ रागरहितः नहीं है किन्तु परपदार्थसंक्रान्तिरहित: है।
अर्थ - जो अपनी आत्मा में शुद्ध उपयोग है -- वह शुद्धोपयोग स्वयं उपयोगात्मक ज्ञानचेतना है। वह उपयोग भी अर्थ से अर्थान्तर के संक्रमणरहित होने से [ एक पदार्थ से दूसरे परपदार्थ में उपयोग के संक्रमण रहित होने से निर्विकल्प है।( पर पदार्थ में संक्रान्ति रहित है)[शद्धात्मानभव रूप जो उपयोगात्मक ज्ञानचेतना है वह भी वास्तव में निर्विकल्पक ही है, क्योंकि जितने काल तक शुद्धात्मानुभव होता रहता है उतने काल तक ही उपयोगात्मक ज्ञानचेतना कहलाती है, और उस काल में शुद्धात्मा से हट कर दूसरे पदार्थों की ओर ज्ञान जाता नहीं है। इसलिये उस समय संक्रान्ति के न होने से उपयोगात्मक ज्ञान को भी निर्विकल्पक कहा गया है।